स्टोरीटेल पर ‘वैशाली की नगरवधू’ सुनने में वक्त लगा। यूँ तो इसका वाचन समय ही लगभग 27 घंटे हैं, लेकिन अन्यथा भी यह उपन्यास कई पात्रों, स्थानों, पटाक्षेपों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों से गुजरता है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले अधिकांश मेरी उम्र के व्यक्ति यह पुस्तक पढ़ चुके होते हैं। जैसे माइकल मधुसूदन दत्त की ‘मेघनाध वध’ को हर बंगाली इसलिए पढ़ लेते हैं कि उनकी भाषा बेहतर हो जाएगी, उसी तरह का एक व्यायाम यह पुस्तक भी है। यह मैंने स्कूल के दिनों में पढ़ी थी, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे शब्दकोश में कम से कम दो-ढाई सौ शब्द तो जुड़ ही गए। मैं यह नहीं कहना चाह रहा कि यह पुस्तक हिंदी में नहीं है, लेकिन बोल-चाल की आधुनिक हिंदी से भिन्न है। एक इतिहास कथा की जो भाषा अपेक्षित है, वैसी ही है।
एक और निजी कारण शायद यह भी रहा हो कि इसमें जिस क्षेत्र और परिवेश का वर्णन है, वह कभी मेरे पूर्वजों का भी रहा होगा। आज जो मुज़फ़्फ़रपुर या हाजीपुर की दुर्गंधित गलियाँ हैं, वह कभी वैभवशाली रही होंगी। मिट्टी के नीचे एक संपन्न नगर दबा होगा। एक व्यवस्थित नगर जिसकी व्यवस्था के गुण भले नहीं बचे, अवगुण समीचीन हैं।
कथावाचक त्रिलोक ने इसे पूरे इत्मीनान से पढ़ा है। एक-एक वाक्य को भाव से नत्थी कर। यह सहज नहीं रहा होगा, क्योंकि जब शब्द ही तत्सम हैं, तो उसका अर्थ लगाते हुए पढ़ना कितना कठिन होगा। मुझे कथावाचक की उम्र नहीं पता, मगर जो भी रही हो, ऐसी भाषा पिछली दो-तीन सदियों में तो नहीं ही बोली गयी। न सिर्फ़ बल्कि स्थान, पात्र, संदर्भ सभी प्राचीन हैं। यह एक बड़े फलक की कथा है, जिसमें वज्जि महाजनपद को पुनर्जीवित किया गया। इसमें बिहार की वर्तमान भाषा और बोलियाँ नदारद हैं।
जैसा कथा के शीर्षक से स्पष्ट है, यह ‘वैशाली की नगरवधू’ यानी अम्बपाली (आम्रपाली) की कथा है। उस समय यह प्रथा थी कि नगर की सबसे सुंदर युवती किसी एक पुरुष से विवाह न कर, संपूर्ण नगर की वधू होती। इस प्रथा की आज के संदर्भ में स्वाभाविक आलोचना तो हो सकती है, लेकिन आम्बपाली के जीवन से कई उन्मुक्त स्वर भी उभरते है। आम्बपाली नगरवधू होकर अपनी शर्तों पर नगरवधू बनती है। वे शर्तें क्या हैं, इसके लिए तो कहानी सुननी होंगी। लेकिन, आम्बपाली सहज प्राप्य गणिका रूप में भी नहीं है, न ही एक समर्पित पत्नी रूप में। आम्बपाली के लिए प्रयुक्त संबोधन भी ‘देवी’ यानी पूज्य है।
कथा ऐतिहासिक रूप से बहुत ही संवेदनशील समय की है, जब धर्म और वर्ण-भेद पर प्रश्न उठने शुरू हो गए थे। बुद्ध और महावीर का उदय हुआ था। तथागत (बुद्ध) द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन को यूँ प्रस्तुत किया गया है, जैसे वह हमारे सामने घट रहा हो। ब्राह्मणवाद पर विमर्श कथा में कुछ यूँ पिरोया गया है, कि वह सीधे मुखर रूप से आक्रमण न होकर, हमें आत्म-चिंतन के लिए प्रेरित करती है। इस तरह यह एक प्राच्यवादी (ओरियेंटलिस्ट) गद्य होकर भी प्रगतिवादी गद्य है।
अगर किसी को भारत के प्राचीन इतिहास में रुचि हो, तो यह एक पथ-प्रदर्शक है। वज्जि गणतंत्र (वैशाली) अगर कथा का केंद्र है, तो विदेह, कौसाम्बी, गांधार आदि भी कथा में यूँ आते हैं, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा कर रहे हों। आज के संदर्भ में कहें तो पूरे उत्तर भारत होते हुए अफ़ग़ानिस्तान तक। यह सोचना ही रोमांच से भर देता है कि संस्कृति का विस्तार आज से कहीं विस्तृत था।
एक रूपक के रूप में भी आम्बपाली को देखा जा सकता है, जिसकी कामना के लिए मगध के सम्राट बिम्बिसार वैशाली पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। इससे राज्यों के मध्य संबंध उभर कर आते हैं। व्यापारिक और ऐच्छिक संबंधों में द्वंद्व दिखता है, जो किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है, जिसे ‘डिप्लोमेसी’ के रूप में परिभाषित किया जाता है।
वहीं, कथा में एक सहिष्णु समाज दर्शाया गया है, जिसमें परस्पर विरोधी या असम्मत पंथ भी साथ रहते हैं। बौद्ध और जैन पंथों के साथ असहमति के बावजूद उनका सह-अस्तित्व है। आज भले ही अक्सर बौद्ध को भिन्न धर्म मान लिया गया है, किंतु कभी वह एक ही धर्म की शाखा थी। वह अपने-आप में स्वतंत्र होकर भी एक ही चेतना की पौध थी। न सिर्फ़ समाज, बल्कि राज्य द्वारा भी इन पंथों को पर्याप्त संरक्षण था। यह हमें सोचने को मजबूर करता है कि आखिर किन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म के अनुयायी लुप्त होते चले गए, और भारत से बाहर ही प्रमुखता से बच गए।
समाज में न सिर्फ़ वर्ण-भेद, बल्कि सामंतवाद के रूप भी इस कथा में दर्शाया गया है। सामंत और कृषक में एक आर्थिक फाँक है, और इसी तरह श्रोत्रिय ब्राह्मण और शूद्रों में भी बड़ी फाँक है। यह वर्ण-व्यवस्था की जड़ों को दिखाती है, कि वह कितनी सदियों से चली आ रही है। उसका स्वरूप समानतावाद की ओर बढ़ने के बजाय रूढ़ कैसे होता गया? ऐसे प्रश्न सुनते हुए मन को झकझोरते भी हैं।
हालाँकि इस किताब को एक इतिहास मान लेना भी भूल होगी। इसमें तीन चौथाई से अधिक हिस्सा लेखक की कल्पना है। कुछ अंश तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से सीधे नकारे भी जा सकते हैं। वहाँ फंतासी का प्रयोग है, जो अक्सर ऐतिहासिक कथाओं में स्वत: आ जाता है। उसकी अपनी काव्यात्मक उपलब्धि भी मानी जा सकती है, लेकिन अगर यथार्थवादी कथा होती तो उसे एक तर्कशील व्यक्ति को सुनने में शायद कुछ अधिक पसंद आता। अगर पात्र वास्तविक हैं, तो कथा में फंतासी को अधिक से अधिक जादुई यथार्थवाद कह कर तार्किक बताया जा सकता है।
इसके बावजूद अगर मानक साहित्य या विश्व-स्तर के साहित्य के रूप में चर्चा होगी, तो ‘वैशाली की नगरवधू’ को जगह दी ही जाएगी। यह उन किताबों में है, जिसके लिए कहा जा सकता है कि जीवन में इसे न सुना, तो जीवन निरर्थक है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। यह भाषा, शिल्प, कल्पना, विषयवस्तु, हर तरह से एक परिश्रम से लिखी किताब है। इसलिए इसे परिश्रम कर सुन भी लेना चाहिए।
स्टोरीटेल पर इसी कड़ी में लेखक की दो अन्य पुस्तकें ‘वयं रक्षाम:’ और ‘सोमनाथ’ भी सुनी जानी चाहिए। यह तीनों एक चक्र पूरा करते हैं।


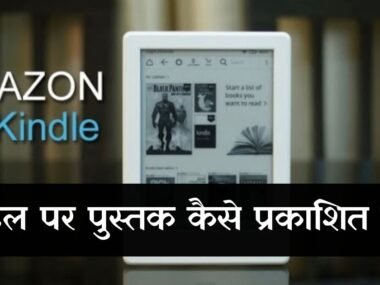
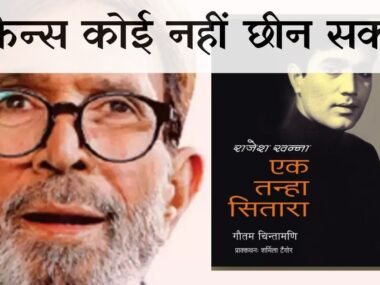
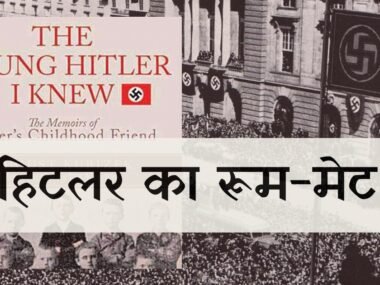
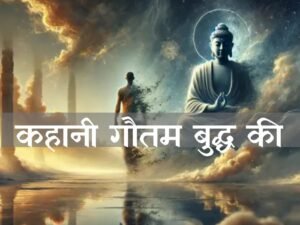
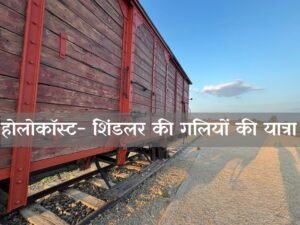
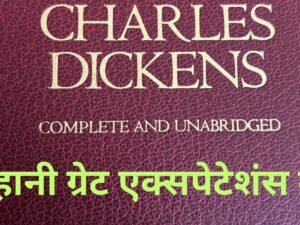
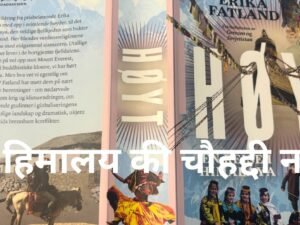
1 comment
Manniya Pravin Kumar Jha ji , maine apki LTTE par likhi kuch lekhon ko facebook par padha halanki sirf 2 ya 3 episodes hi mujhe mile . Mai ye kehna chahunga ki aapne LTTE ke ghatnakram ko vastav me bahut ki kareene se saja kar aur kahani ke roop me prastut kiya hai jo vastav me bahut hi jatil aur sarahniy karya hai.
Mere vichar se “Vaishali ki Nagarvadhu” ko bhi shashtri ji ne purane ghatnakramo ko ek sutra me piro kar us samay ke samajik praidrishya ko kahani ka akaar de kar logo ke saamne prastut kiya hai. Maine aisa kahi bhi nahi paya ki shahshtri ji ne usse ek itihaas ke roop me prastut ya mahimamandit kiya ho . Somnath ki kahani bhi yahi darsaati hai.
Dhanyawaad