1
मैं वियना के यूरोपीय रेडियोलॉजी सम्मेलन में शरीक होने आया था। एक पूरा दिन दिमाग के धीरे-धीरे कमजोर होने पर था, जिसमें पिछले दशकों में डाक्टरों की रुचि बढ़ी है। आज से दो दशक पहले जब मैं अमरीका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में अलझाइमर नामक बीमारी के शोध से जुड़ा था, तो यह ख़ास रुचिकर नहीं लगी। बल्कि मैंने शोध बीच में ही त्याग दिया, और डाक्टरी के पारंपरिक प्रैक्टिस की ओर लौट गया। रुचिकर का अर्थ यहाँ धन, यश आदि से भी है जो मेडिकल रिसर्च में कम होता है।
लेकिन, दिमाग का शोध मानव-जाति का सबसे उलझा हुआ शोध भी है। आखिर होमो सैपिएंस नामक प्रजाति के पास सभी जीवों से अधिक क्या है? दिमाग ही तो है। मानव विकास में भी जो अंग सबसे अधिक विकसित हुआ, वह मस्तिष्क ही है। आने वाले समय में यह और भी विकसित होगा। अगर किसी से उसके बाह्य अंग एक-एक कर छीन लिए जाएँ, तो भी दिमाग के चलते रहने तक उसका जीवन है। दिमाग शिथिल पड़ गया जिसे ‘ब्रेन डेड’ भी कहते हैं, तो वह जीकर भी क्या जीएगा?
भारतीयों को संभवतः स्मरण हो जब अरुणा शानबाग नामक एक नर्स यौन-हिंसा के पश्चात 41 वर्ष तक मूक, दृष्टिहीन और प्रतिक्रिया-हीन अवस्था में रही। सर्वोच्च न्यायालय तक अपील की गयी कि उन्हें ‘यूथैनेसिया’ यानी गरिमापूर्ण चिकित्सकीय मृत्यु दे दी जाए, मगर न्यायालय तैयार नहीं हुई। हालाँकि उनकी मृत्यु के बाद भविष्य में ‘पैसिव यूथैनेसिया’ (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की इजाज़त देने को मंजूरी मिली।
दरअसल, एक लंबे समय तक दिमाग को शरीर का एक अंग-मात्र ही माना जाता रहा। मानसिक रोगों का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट दवाओं या ऑपरेशन से करते थे। जिनका दिमाग चिकित्सकीय जाँचों के हिसाब से ठीक होता था, उनको रोगी नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसे ‘हिस्टिरिया’ कहा जाता, जिसका मूल है हिस्टेरो यानी- बच्चादानी। प्राचीन काल में महिलाएँ शिकायत करती कि उनका बच्चादानी कहीं गुम हो गया है। इसे महिलाओं की ख़ामख़ा बहानेबाज़ी माना जाता, और इस रोग को निरर्थक।
बीसवीं सदी तक जब महिलाएँ पीठ दर्द, पेट दर्द या कोई भी शिकायत करती, तो डाक्टर इसे ‘हिस्टिरिया’ कहते। इसकी वजह थी कि महिलाओं की शारीरिक जाँच में कोई कमी नहीं मिलती। इसलिए यह बहानेबाज़ी या ख़ामख़ा की नौटंकी के सिवा और क्या हो सकता था? पुरुषों में ऐसी शिकायत कम देखी जाती, तो यह तर्क और पुख़्ता हो जाता कि महिलाएँ खुद यह स्वांग रचती है। सिर्फ़ कुछ तवज्जो पाने के लिए।
लेकिन, क्या यही सच था? अगर नहीं, तो सच का उजागर कब और किसने किया?
2
मैं वियना के ऑस्ट्रिया सेंटर से निकल कर टहलते हुए डैन्यूब नदी के किनारे गए। फिर लगा कि यह नदी पार कर लेता हूँ। रेलवे पुल के साथ चल रही पद-मार्ग पर मैं चलने लगा। नदी पार कर सीधा चलता गया तो एक नहर मिली। वह भी पार कर गया। वहाँ एक भारतीय रेस्तराँ दिखा, जो एक केरल के व्यक्ति चला रहे थे। उनसे पूछा कि आस-पास कुछ देखने की जगह है। उन्होंने पूरी सूची बतानी शुरू कर दी- कला संग्रहालय, पैलेस, फव्वारे, गिरजाघर…
मैंने कहा कि यह सब तो मुझे किसी भी यात्रा वेबसाइट पर दिख जाएँगे। सिग्मंड फ्रॉय्ड का नाम सुना है आपने?
उन्होंने कहा- हाँ! उनका घर तो यही पास में ही है।
दरअसल मैंने तो गंतव्य पहले ही तय कर लिया था, सिर्फ़ जानना चाह रहा था कि एक रेस्तराँ चलाने वाला भारतीय इस नाम से परिचित हैं या नहीं। हालाँकि भारतीयों के सामान्य ज्ञान को कम नहीं आँकना चाहिए। जनाब पूरे अप-टू-डेट थे। जब मैंने कहा कि मैं बिहार से हूँ, उन्होंने तपाक से कहा- नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है न? वियना में बैठे-बैठे हर बसंत बदलते गठबंधन की ताज़ा जानकारी रखना साधारण बात नहीं।
वहाँ से जब सिग्मंड फ्रॉय्ड की गलियों में जाने लगा, तो नीचे फुटपाथ पर सुनहरी पट्टियाँ नज़र आयी। मैं इन पट्टियों से परिचित था, क्योंकि रोम में भी दिखी थी। ये इस बात की पहचान है कि यह इलाक़ा कभी यहूदी बस्ती रहा था। अब यहूदी नहीं बचे, उनकी ये स्मारिकाएँ ही बची है। उस पर दर्ज़ था कि यहाँ अमुक यहूदी रहते थे, और अमुक ईसवी में उनको नाज़ी उठा कर ले गए और मार दिए गए। कुछ स्थानों पर तो पट्टियों के बजाय पंक्तिबद्ध नाम ही उकेर दिए गए थे। उस गली में मरने वाले ही इतने थे कि कितनी पट्टियाँ लगाते?
उन यहूदियों की लाशों के ऊपर चलते हुए आखिर सिग्मंड फ्रॉय्ड का घर भी आ ही गया। उस घर की तो पूरी दीवाल ही नामों से भरी थी!
पूछने पर पता लगा कि जब सिग्मंड फ्रॉय्ड नाज़ियों के डर से सपरिवार भाग गए, तो उनके इसी घर में मुहल्ले के यहूदियों के बंद कर दिया गया। बाद में उन्हें ले जाकर गोली मार दी गयी, या गैस चैम्बर आदि में डाल दिया गया।
क्या यह भी एक तरह का मानसिक रोग था? अन्यथा एक मनुष्य का दिमाग भला सैकड़ों मनुष्यों की बलि चढ़ाने की क्यों सोचेगा? उन पट्टियों और दीवारों पर बूढ़ों, बच्चों, औरतों और तमाम निर्दोष लोगों के नाम थे। अब उन घरों के मालिक बदल चुके थे, जहाँ कभी वे रहते थे। जहाँ कभी डॉ. सिग्मंड फ्रॉय्ड अपना क्लिनिक चलाते थे।
3
अंदर प्रवेश करते ही एक सीढ़ी दिखी, जिससे पहले तल पर जाना था। पहली मंजिल पर दोनों तरफ़ दो दरवाजे थे। जैसा आज-कल के अपार्टमेंट में होता है, ये दो फ्लैट थे। दोनों दरवाज़ों पर एक ही नाम था- Prof. Dr. Freud
इतना डाक्टरी अनुभव से स्पष्ट था कि एक फ्लैट में उनका आवास होगा, और दूसरे फ्लैट में क्लिनिक। ये दोनों फ्लैट अंदर से जुड़े हुए भी होंगे। डाक्टरों का घर और क्लिनिक जितना पास हो, उतनी ही मरीजों को सहूलियत होती थी। ज़रूरत पड़ने पर रात को ढाई बजे भी दरवाज़ा खटखटा दिया, तो अपने आला और अन्य यंत्रों के साथ डाक्टर मिल जाएँगे।
वहाँ उनके एक मित्र का अनुभव अंकित था, ‘मैंने हमेशा यही पाया कि घंटी चाहे किसी दरवाजे की बजाओ, खुलता हमेशा दूसरा दरवाजा’
यूँ तो यह वाक्य मज़ाकिया लगता है, मगर इसी वाक्य में सिग्मंड फ्रॉय्ड का रहस्य छुपा है। दिमाग के दो दरवाज़ों का- चेतन (कॉन्शस) और अवचेतन (सब्कॉन्शस)!
बहरहाल, मैं पहले उनके आवास का मुआयना करने गया। दरवाज़ा खुलते ही उनका ड्राइंग रूम दिखा, जो बाहर एक बरामदे की ओर खुलता था। वहाँ एक ठूँठ शाहबलूत का पेड़ तब भी था, अब भी एक है। मैंने लगभग दरवाज़े से ही यह कयास लगा लिया कि वहाँ जाकर अक्सर फ्रॉय्ड महोदय तंबाकू के कश लेते होंगे। यह बात बरामदे पर लिखे विवरण से पक्का भी हो गया।
ड्राइंग रूम में उनका शतरंज और ताश रखा था, जो वह अक्सर अकेले ही बैठ कर खेला करते। वहीं उनकी लिखी पुस्तक ‘टोटम ऐंड टैबू’ का पहला दुर्लभ संस्करण भी रखा था। उनके द्वारा जमा किए गए मिस्र, रोम और अन्य स्थानों के जंतर-मंतर भी रखे थे। इसे देख कर यह शंका हो सकती है कि यह किसी औघर या तांत्रिक का घर है। लेकिन, औघर, तांत्रिक या कुलदेवताओं का मनोविज्ञान क्या है?
फ्रॉय्ड ने धर्म के विषय में सीधे-सीधे न लिख कर कबीलों के विश्वासों और देवताओं पर लिखा। उन्होंने यह कहा कि मनुष्य जिस तरह अपने माता-पिता से जुड़ा होता है, उसी तरह एक कबीला भी अपना एक माता और पिता तय करता है। यह उन्हें सुरक्षा भी देता है, जीजीविषा भी, और एक यौन-बंधन भी। ये ऐसी छवियाँ हैं, जिनके प्रति किसी तरह की यौन-भावना नहीं उत्पन्न हो सकती, जो अन्यथा एक मानवीय गुण है।
फ्रॉय्ड ने तो यहाँ तक कहा कि एक बच्चा पैदाइशी यौनाकर्षण के साथ आता है। एक पुत्र अपनी माँ से और एक पुत्री अपने पिता से आकर्षित हो सकती है, और इस आकर्षण में वह प्रतिद्वंद्वी निर्माण भी कर लेती है। पुत्र अपनी माँ से स्नेह में पिता को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगता है, और यही स्थिति पुत्री की अपने माँ के साथ हो सकती है। इसे उन्होंने ‘ईडीपस कॉम्प्लेक्स’ (Oedipus complex) कहा।
बाल्य मन से किशोरावस्था में प्रवेश के साथ इस तरह के कॉम्प्लेक्स घट जाते हैं, लेकिन यह उसकी मानसिकता पर प्रभाव डाल सकती है। लिंग-बोध बाल्यकाल से ही हो जाता है, और इस कारण यौन-हिंसा या यौन-शोषण भी उसके बोध का हिस्सा है। अगर बोध न होता, तो इसका दूरगामी मानसिक प्रभाव कैसे होता? सिर्फ़ यह उसके अवचेतन में कहीं दब जाता है।
सवाल ये है कि उस अवचेतन तक पहुँचा कैसे जाए? दूसरों की छोड़िए, क्या खुद के अवचेतन में हम कभी प्रवेश करते हैं? इसका उत्तर अगले कमरे में मिलता है।
4
यह सिग्मंड फ्रॉय्ड का बेडरूम है। यहाँ सोते हुए फ्रॉय्ड ने सपने देखे। जैसे हम सभी देखते हैं। अच्छे, बुरे, डरावने। लेकिन, इन सपनों को हम नींद खुलते ही भूल जाते हैं। अगर कुछ देर याद भी रहते हैं, तो चेतन मन उसे भुलाने का प्रयास करता है। यह जुमला तो सब ने सुना होगा- ‘सपने कभी सच नहीं होते’
फ्रॉय्ड ने अपने ही सपनों का विश्लेषण शुरू किया। तकरीबन ढाई सौ सपनों का संग्रह तैयार किया, और उसके निष्कर्ष निकाले कि इनका अर्थ क्या हो सकता है।
कमरे में ही फ्रॉय्ड की पुस्तक ‘इंटरप्रटेशन ऑफ़ ड्रीम’ का पहला संस्करण रखा था। इसे अपने जीवन काल में ही फ्रॉय्ड ने तीस बार संशोधित किया, जिसमें अपने और अपने मरीजों या दोस्तों के सपने जोड़े।
मैं यहाँ फ्रॉय्ड के वे स्वप्न रख रहा हूँ, जो उस कमरे में अंकित थे। पहला स्वप्न है कि सिगमंड फ्रॉय्ड अपने उसी मकान की खिड़की से अधनंगी अवस्था में कूद रहे हैं। दूसरा स्वप्न है कि कोई जहाजी युद्ध चल रहा है, जहाँ एक-एक कर उनके जहाज हार रहे हैं, मगर एक छोटा सा जहाज बच कर निकल रहा है।
दूसरे स्वप्न का उन्होंने यह विश्लेषण किया कि अमरीका और स्पेन के मध्य युद्ध में वह अपने कुछ परिजनों को लेकर चिंतित थे। तभी यह स्वप्न आया।
पहला स्वप्न क्या यह इशारा कर सकता है कि नाज़ियों के आने के बाद उन्हें खुद यह घर छोड़ कर भागना पड़ेगा? संभावना कम है क्योंकि इस पुस्तक के पहले संस्करण (1899) तक नाज़ी कहीं विश्व-पटल पर थे ही नहीं। लेकिन, ऐसी शंकाएँ तो उपजती ही रहती है।
इस कमरे से निकल कर फ्रॉय्ड का बाथरूम आता है। उस ज़माने में यूरोप के रसूखदार लोग भी बाल्टी-मग लेकर नीचे बैठ कर ही नहाते थे। हालाँकि आखिरी दिनों में एक बाथ-टब उन्होंने लगवा लिया था, जो अब वहाँ मौजूद नहीं था। कई चीज़ें फ्रॉय्ड खुद उखाड़ कर अपने साथ लंदन ले गए, और कई नाज़ियों ने तोड़ दी।
अब मैंने उस आवास से उनके क्लिनिक की ओर प्रवेश किया, जो एक गलियारे के माध्यम से जुड़ा था। वहीं दुनिया का वह इलाज शुरू हुआ, जो पहले बहुत कम देखा-सुना गया था- मानसिक विश्लेषण (साइकोअनालिसिस)!
5
क्लिनिक तो खैर एक जैसे ही होते हैं। बाहर एक प्रतीक्षा-कक्ष, अंदर एक कमरा जहाँ मरीजों की जाँच होती है, एक सुई आदि देने का कमरा और कभी-कभार एक डाक्टर का निजी केबिन।
प्रतीक्षा-कक्ष में एक ठीक-ठाक सोफ़ा लगा था, जो लंदन से उनकी बेटी एन्ना फ्रॉय्ड ने सत्तर के दशक में वापस भिजवाया। जब फ्रॉय्ड के इस घर को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की क़वायद शुरू हुई, तो उनकी चीजें यहाँ मंगवाई गयी। सोफ़े के पीछे फ्रॉय्ड की तमाम डिग्रियाँ लगी थी। वियना विश्वविद्यालय से डाक्टरी और न्यूरोलॉजी की डिग्री। पेरिस से साइकोलॉजी में फेलोशिप। लंदन से दो डिग्रियाँ। यह भी मैंने जाना कि वह पूरी तरह व्यवसायिक व्यक्ति थे, जो अमूमन बिना फ़ीस मरीज नहीं देखते। आज भी यही आलम है कि गरीब मानसिक रोग के लिए किसी मनोविश्लेषक के पास अक्सर नहीं जाते। उस समय तो सवाल ही नहीं था।
अंदर जो डॉक्टर का हॉल था, वह आज तो सामान्य है, मगर बीसवीं सदी के हिसाब से अनूठा लगता है। एक आराम-बिस्तर था, जिस पर मरीज लेटे-लेटे अपनी गाथा कहते। स्वयं फ्रॉय्ड उसके साथ लगे कमरे में कुर्सी लगा कर बैठते, और दरवाज़ा खुला रखते। वह चाहते थे कि मरीज अपनी कहानी बिना किसी दबाव के, खुल कर कह दे। यह कुर्सी पर बैठ कर या चेतन अवस्था में कठिन था, इसलिए आराम से लेट कर हल्की नींद में जाते हुए कहे।
इस प्रक्रिया को उन्होंने ‘फ्री असोसिएशन’ कहा। इसके लिए उन्होंने पहले सम्मोहन के असफल प्रयास किए, फिर माथे पर उंगलियों से दबा कर अवचेतन में ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मरीज को निष्क्रिय रह कर खुले दिमाग से बात कहने कहा। जैसे कोई ईसाई व्यक्ति गिरजाघर के पादरी के सामने चीजें कंफेश करता है, कुछ इसी तरह मनोविश्लेषक के समक्ष अपना पूरा चिट्ठा खोल दे।
अपने बचपन के बुरे अनुभव, किसी भी तरह का यौन-अनुभव, कोई ग्लानि, कोई दुष्कर्म जो अवचेतन में कैद होकर रह गया हो, सब बाहर कर दे। इसे उन्होंने ‘कैथार्सिस’ कहा। इसने मनोरोग की धारा ही बदल दी। जिसे लोग ‘हिस्टिरीया’ या नौटंकी कह कर ख़ारिज कर रहे थे, उसकी वजह दरअसल वर्षों पुराना कोई बुरा यौन-अनुभव था।
स्वयं फ्रॉय्ड को यह उस दिन समझ आया जब उनके पास एक एन्ना नामक मरीज आयी, जिसका कमर से नीचे का शरीर लकवा की तरह निष्क्रिय हो रहा था। डाक्टरों को कोई कारण नहीं मिल रहा था, और दरअसल कोई भौतिक कारण था भी नहीं। ऐसे मरीजों को बिजली या पानी के झटके दिए जाते थे, मगर यह भी काम नहीं आए। आखिर फ्रॉय्ड ने अपने प्रोफेसर बोयर को कहा कि वह उन्हें मरीज के अवचेतन में जाने की आज्ञा दें। आखिर कई सेशन में उन्हें एन्ना ने अपने बचपन के बुरे अनुभव बताए, और इस कैथार्सिस के बाद वह धीरे-धीरे ठीक हो गयी। वह बात जो उसे इतने दिनों से किसी सर्पदंश की तरह डस रही थी, वह बाहर आ गयी।
6
आज जब मनोरोग पर चर्चाएँ शुरू हुई है, तो कम से कम यूरोप में एक-एक घंटे के सेशन हो रहे हैं। कम उम्र से ही लोग मनोविश्लेषक से जुड़ रहे हैं। लेकिन, उन दिनों एक-डेढ़ घंटे के एक सेशन करना डॉ. सिग्मंड फ्रॉय्ड ने ही शुरू किया। मैं जिस घर में खड़ा था, उसकी दीवारों के अंदर ही मनोविश्लेषण की पैदाइश हुई।
घर से कुछ दूर ही उसी गली में पहले मनोविश्लेषकों की एक टीम बैठने लगी, जो सोसाइटी आज तक कायम है। कार्ल युंग (Carl Jung) जैसे मनोविश्लेषक उससे जुड़े और उन्होंने फ्रॉय्ड के कई विश्लेषणों को ख़ारिज भी किया। लेकिन, इस विषय ने अपनी जड़े स्थापित कर ली। दिमाग सिर्फ़ एक अंग नहीं रह गया, बल्कि मनुष्य के अनुभवों की एक ऐसी कोडेड तिजोरी बन गयी जिसकी चाभी उसे खुद नहीं मिल रही। वह जब तक खुल कर बाहर नहीं आती, वह अजीबोग़रीब रूप में दिखती रहेगी। कभी एक अबूझ बीमारी, कभी स्मृति-दोष, कभी व्यक्तित्व में विच्छेद, कभी हिंसात्मक, कभी खुद में बंद रहने की प्रवृत्ति, जिसे नाम मिलेगा- पागलपन।
मेरे सामने फ्रॉय्ड के कुछ कोरे काग़ज़ और उनका कलम पड़ा था। उनके विषय में वर्णित है कि ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब उन्होंने कलम को हाथ नहीं लगाया हो। वह चिट्ठियाँ लिखते। अपने दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन ज्वाइग इत्यादि को। उनका मानना था कि कई बार हम आमने-सामने बतिया कर खुल नहीं पाते, मगर चिट्ठी में खुल जाते हैं। नाज़ियों द्वारा तमाम किताबें और चिट्ठियाँ नष्ट करने के बाद भी फ्रॉय्ड की बीस हज़ार से अधिक चिट्ठियाँ संकलित हैं, और आइंस्टाइन से हुए संवाद तो मेरे समक्ष ही मौजूद हैं।
आइंस्टाइन उनसे पूछते हैं, ‘क्या आपके इस मनोविज्ञान से दुनिया में युद्ध रोके जा सकते हैं?’
फ्रॉय्ड उत्तर देते हैं, ‘मनुष्य में यह प्रवृत्ति तो पैदाइशी ही है, लेकिन सांस्कृतिक विकास से इसे कुछ कम अवश्य किया जा सकता है’
एक चिट्ठी में भारत का भी ज़िक्र है, जब रोम्या रोलाँ उन्हें भारतीय संस्कृति में नियमित चिंतन के महत्व को बताते हैं। हालाँकि वहाँ फ्रॉय्ड का जवाब कुछ अलग ही दिशा में है।
फ्रॉय्ड कहते हैं, ‘चिंतन या सोचना प्रगतिशील लगता है। किंतु मैंने पाया है कि बहुत अधिक चिंतन भी हमें पीछे ही ले जाती है’
वहाँ से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि फ्रॉय्ड की एक जीवनी लेता जाऊँ। जो पहली किताब दिखी, उसके पहले अध्याय में ही लिखा था कि जब ऑर्नाल्ड ज्वाइग (जर्मनी) ने उनकी जीवनी लिखने का मन बनाया, फ्रॉय्ड ने कहा,
‘जीवनियाँ झूठ, फरेब और ख़ामख़ा महिमा-मंडन से भरी होती है। मेरी झूठी जीवनी कोई पढ़े, यह मैं नहीं चाहता। और मेरी सच्ची जीवनी कोई पढ़ ले, यह तो मैं क़तई नहीं चाहूँगा’
जीवनी तो नहीं खरीदी। नेटफ्लिक्स पर एक ‘फ्रॉय्ड’ (Freud) नामक एक मसालेदार सीरीज़ ज़रूर देखी, जो घोषित रूप से ही गल्प है।
Author Praveen Jha narrates his travel to the house of neurologist and a pioneer psychoanalyst Sigmund Freud
इस घर का ऑफिसियल विडियो देखने के लिए क्लिक करें
हिटलर के वियना प्रवास पर पढ़ने के लिए क्लिक करें
तस्वीरें








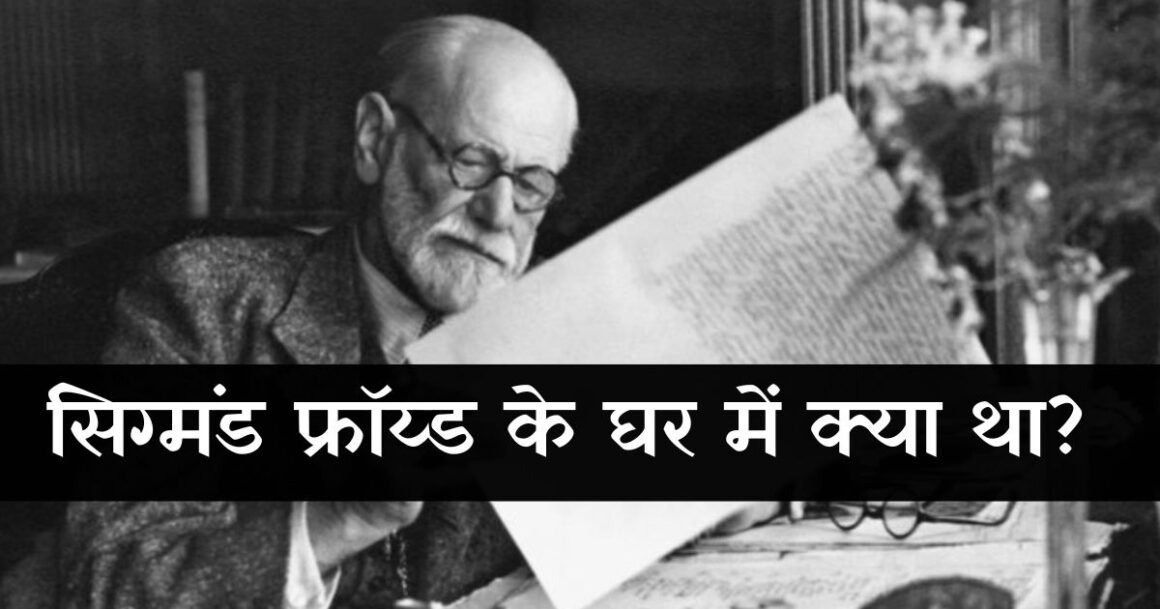
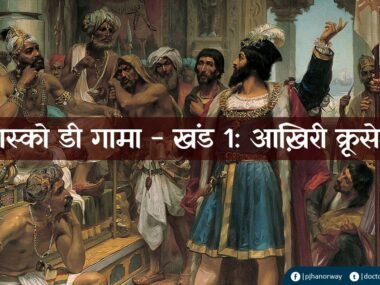
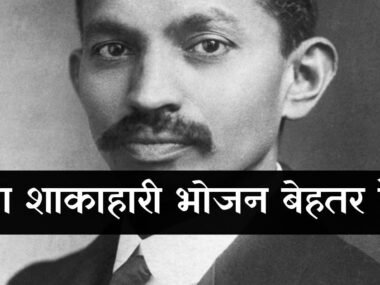
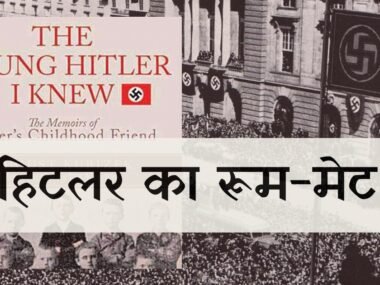
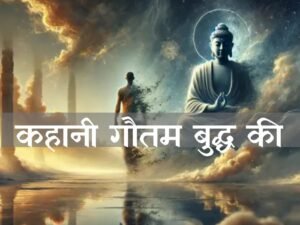
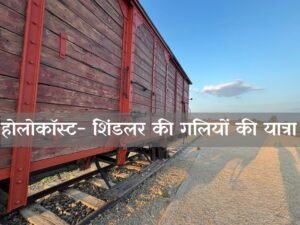
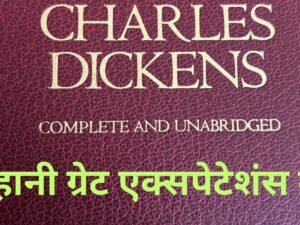
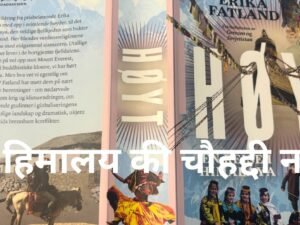
7 comments
दिलचस्प आख्यान। मारे गए यहूदियों के लिखे नामों के बारे में पहली बार जाना।
कुछ रिलेटेड चित्र भी साथ में चिपका देते तो जिज्ञासाओं की पूर्ति भी होती।
धन्यवाद। अब तस्वीरें भी लगा दी हैं
स्वागत. सरल भाषा में अच्छी, उपयोगी जानकारी
कई नई बाते पता लगी, धन्यवाद ।
आपने इतनी रोचक ढ़ंग से जानकारी दी है कि एक ही बार में पुरा पढ़ गया।
बहुत रोचक, पढ़ते हुए कल्पना में अलग ही अनुभूति, फ्रायड के घर में…