1
कोरोना काल में मैं एक शृंखला नियमित देख रहा था, जिसमें कुछ विद्यार्थी जाने-माने इतिहासकारों से संवाद कर रहे थे। उसमें एक संवाद में रोमिला थापर विद्यार्थी को एक होमवर्क सुझाव देती हैं– जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध में चंद्रगुप्त का पलड़ा भारी हुआ, वैवाहिक संधि हुई। उन संबंधों में कैसे आपसी संवाद रहे, क्या विस्तार रहा? यह डेढ़ घंटे के साक्षात्कार में बमुश्किल तीन मिनट का हिस्सा था, जिस पर न जाने किसी ने कार्य शुरू भी किया या नहीं।
हाल ही में आयी पुस्तक ‘अभ्युत्थानम्’ के आवरण से अनुमान लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित उपन्यास है तो यथाशीघ्र गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर लिया।
ऐतिहासिक उपन्यास में हमें कई नए पात्र, मंच, संवाद, घटनाक्रम गढ़ने होते हैं। भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, और व्यवहार को सदियों पीछे ले जाकर आज के पाठकों को संप्रेषित करना पड़ता है। लोग आचार्य चतुरसेन से नरेंद्र कोहली तक के उदाहरण रख सकते हैं, मगर किसी ऐसे लेखक के लिए जिसका यह पहला उपन्यास हो, यह भगीरथ कार्य है।
इस उपन्यास के मोटे तौर पर पाँच खंड कहे जा सकते हैं। पहला खंड व्यभिचारी नंद के मगध नरेश धनानंद बनने की कथा है। दूसरा खंड चणक पुत्र विष्णुगुप्त के तक्षशिला पहुँच कर चाणक्य बनने की। तीसरी कड़ी में चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की खोज और अलेक्षंद्र (अलेक्ज़ेंडर) का आक्रमण है। चौथे खंड में यवनों (यूनानियों) के विरुद्ध अलग-अलग राज्यों का राष्ट्रीयकरण/एकीकरण है। पाँचवे खंड में मगध की राजधानी पाटलीपुत्र से घनानंद को सत्ताच्युत करना है। इन पाँचों खंडों को लगभग चार सौ पृष्ठों में वर्णित किया गया है।
कोई कह सकता है कि यह सब तो हम चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे टीवी धारावाहिकों में देख चुके हैं, चाणक्य नीति हर गली-नुक्कड़ की दुकानों में पॉकेट बुक्स की शक्ल में बिक रही है, उपन्यास में क्या ख़ास होगा।
पहली चीज कि अगर आप इस उपन्यास को पढ़ते हुए एक छोटी डायरी में नए शब्द नोट करते जाएँ, तो लगभग तीन सौ शब्द जमा हो जाएँगे। हर तरह के रत्नों, युद्ध-शैलियों, गुप्तचरी, रति-क्रिया, भवनों की संरचना से जुड़े शब्द उनकी व्याख्या सहित हैं। शराब के पेग से लेकर अंतर्देशीय वीसा-पासपोर्ट तक के लिए शब्द वर्णित हैं!
दूसरी चीज कि चाणक्य नीति बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज़ में रखी गयी है। यानी कथा में जब वह सिचुएशन वाकई आ जाती है तो क्या करना चाहिए। मुझे तो सबसे रोचक लगा जब चाणक्य का तक्षशीला विश्वविद्यालय में पैनल इंटरव्यू होता है, और वह हर प्रश्न का दमदार जवाब देते हैं।
उपन्यास का स्वर बहुधा घोर राष्ट्रवादी है। इस ग्लोबल दुनिया में विदेशियों के प्रति अति-घृणा ख़ास पचती नहीं। उस समय भी संबंध इतने बुरे शायद न रहे हों। एक तरफ़ अलेक्ज़ेंडर और यवनों को भारतीय राक्षसों (?) से भी बदतर कहना, वहीं चंद्रगुप्त का न सिर्फ़ उनसे स्किल सीखना, बल्कि उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना विरोधाभासी है। भारतीय संस्कृति अगर उन्नत थी तो सुकरात और अरस्तू भी सुशिक्षित संस्कृति के ही थे। संभवतः उपन्यास में इसका ध्येय बिखरे हुए और आपस में लड़ते राज्यों का एकीकरण है। इसके लिए शत्रु का ऐसा छवि-निर्माण कथा की ज़रूरत होगी। न सिर्फ़ अलक्षंद्र बल्कि मगध नरेश घनानंद की छवि भी क्रूरतम ही दिखायी गयी है।
लेखक ने वर्ण-व्यवस्था पर लगभग दो तिहाई पुस्तक में तार्किक रुख़ अपनाया है। मसलन चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र परिवार से कहना और एक शूद्र को सर्वसम्मति से भारत के सम्राट का पद देना साधारण बात नहीं। यह उस सोच पर मज़बूत प्रहार हो सकती है जो वर्ण व्यवस्था की असमानता को कायम रखना चाहती है। आखिरी तिहाई में यह रुख़ कुछ बदलता दिखाई देता है, जिसका एक तकनीकी पक्ष पुस्तक में है। बहरहाल, अगर समाज इससे यह सीख ले रहा है कि जात-पाँत की ऊँच-नीच निराधार हैं, तो यह तिहाई गणित किनारे रखी जा सकती है।
2
उपन्यास सत्यता पर कितनी खरी उतरती है?
अभी इस विषय में वर्णित मूल स्रोत देखे नहीं हैं, लेकिन इसकी संरचना ही उपन्यास रूप में है। यह ऐसी रुचि जगाती है कि स्रोत खंगाल कर, साक्ष्य ढूँढ कर इस इतिहास की तह में जाया जाए।
इस पर सम्मति है कि अलेक्ज़ेंडर भारत की सीमाओं पर आया, और उसके कुछ ही वर्षों बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल शुरू हुआ।
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान से आगे तक हुआ, जो इतिहास की स्कूली पुस्तकों में भी है। यूनानियों से पाटलीपुत्र का संपर्क बना, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, यह बातें तो सर्वविदित है।
इस कथा में दो हायपोथेसिस हैं, जिस पर शंकाएँ रही है। पहला कि अलेक्ज़ेंडर ने किसे हराया, किससे पराजित हुआ, किसने साथ दिया, और किस परिस्थिति में वह वापस लौटा। इस पुस्तक में कहीं जीत तो कहीं हार दिखायी गयी है, जो ऐतिहासिक रूप से संभव है।
दूसरा कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्ज़ेंडर कभी मिले, और क्या चाणक्य उस क्षेत्र में मौजूद थे? सैद्धांतिक रूप से यह संभावना भी दिखती है, और उसके बाद चंद्रगुप्त का उदय और यूनानी क्षत्रपों से संवाद भी इसका समर्थन करता है। लेखक ने इस पक्ष को बहुत ही रोचक तरीके से लिखा है।
बाकी, शंकाएँ तो इस पर भी रही हैं कि चाणक्य कौन थे, कहाँ से आए थे, थे भी या नहीं। ऐसी शंकाओं का कोई अंत नहीं है। पुस्तक में चाणक्य को द्रविड़ (दक्षिण भारतीय) मूल का लिखा गया है, और इसके समर्थन के लिए एक नाम भी वर्णित है।
पुस्तक के एक पक्ष में शूद्र चंद्रगुप्त और द्रविड़ चाणक्य का भारत के शिखर पर बिठा कर एकीकृत भारत राष्ट्र की अवधारणा को रखा गया है।
3
अब आखिरी या बर्निंग क्वेश्चन- इस पुस्तक का आज की दुनिया या भारतीय राजनीति से क्या संबंध?
2021 में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंद्रगुप्त ने अलेक्ज़ेंडर को हराया था, इस पर लिखा जाना चाहिए। इस पर अखबारों में चर्चाएँ हुई। हालाँकि इस पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वारा अलेक्ज़ेंडर को हराने का कोई वर्णन नहीं, लेकिन यूनानियों की पराजय का वीर-रस के साथ वर्णन है। क्या यह उसी राजनीति से प्रेरित लेखन है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुस्तक रोमिला थापर अथवा योगी आदित्यनाथ के कहने पर अलग-अलग धाराओं से लिखी जा सकती है।
एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत की संघीय गणतंत्र संरचना (Federal/Union) पर बल दिया गया है, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता काफ़ी हद तक कायम है। सिर्फ़ सुरक्षा और कुछ अन्य मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप है। यह अपने समय से बहुत आगे की सोच दिखती है, जो वर्तमान भारत में भी लागू नहीं है।
भारत की सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ श्रेष्ठता का वर्णन तो खैर है ही। लेकिन विभाजक स्वर नहीं दिखता। इसमें भारत के अलग-अलग संस्कृतियों और विचारों को एक सूत्र में बाँधने और विदेशी शक्तियों के आक्रमण से लड़ने की रणनीति दिखायी गयी है। नैतिक रूप से बौद्ध मत की कुछ आलोचना और अहिंसा की उस मत से भिन्न व्याख्या भी दिखती है। अधिक गिरहें न खोलते हुए यह प्रश्न खुला रखता हूँ कि इसका राजनीतिक कोण क्या-क्या हो सकता है।
इसे लेखक के कलम की शक्ति ही कहूँगा कि यह पुस्तक बहुकोणीय चिंतन-मनन के मार्ग खोलती है। जिसे जो भी गाँठ पकड़नी है, पकड़ कर विमर्श कर सकते हैं। चार सौ पृष्ठ की किताब मैं अपनी व्यस्तताओं के मध्य तीन बैठक में पढ़ गया। चूँकि घटनाक्रम पूरी तरह से अज्ञात नहीं थे, तो अगले प्रकरण की प्रतीक्षा भी रहती। उनकी तत्समनिष्ठ भाषा अवरोध की बजाय सहायक ही बनी है, क्योंकि वह प्रवाह में है।
इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए और अपने विचार भी खुल कर रखने चाहिए कि कौन सी चीज खटक गयी, कौन सी चीज भा गयी। हालाँकि मुझे लगता है कि मैंने खुल कर कई चीजें नहीं लिखी, मैं बैटन अगले पाठक को पकड़ा रहा हूँ।
Author Praveen Jha shares his experience about book Abhyutthanam by Ajeet Pratap Singh published by Vani Prakashan.


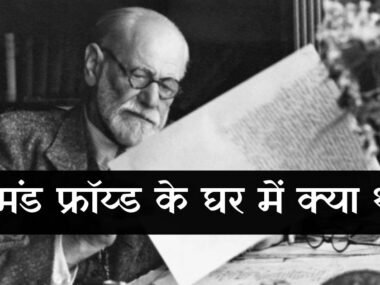
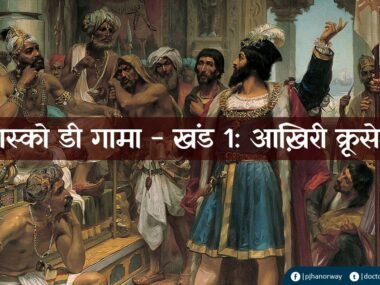
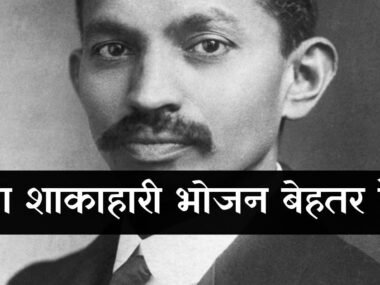
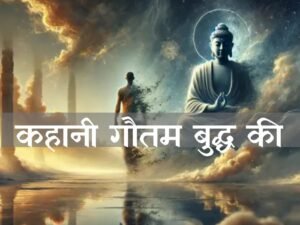
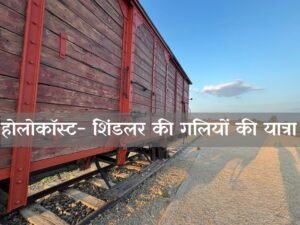
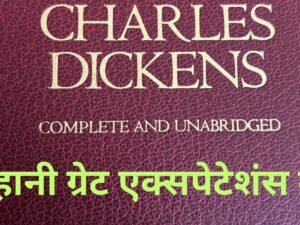
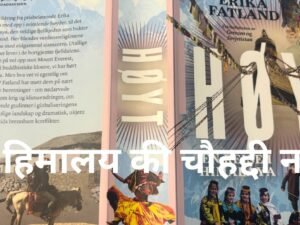
1 comment
धन्यवाद प्रवीण जी