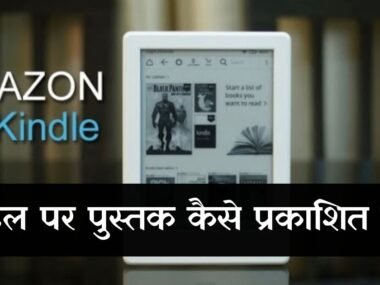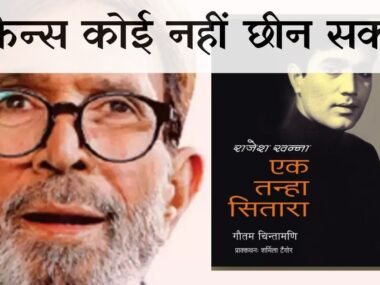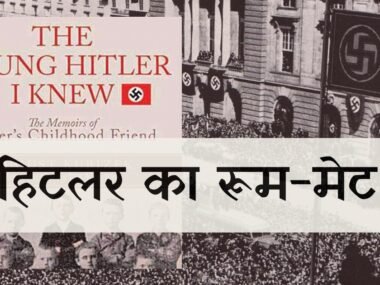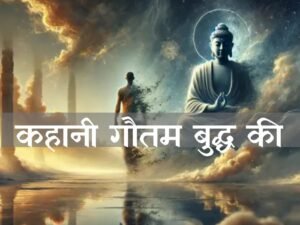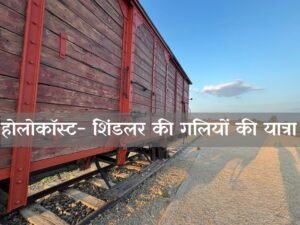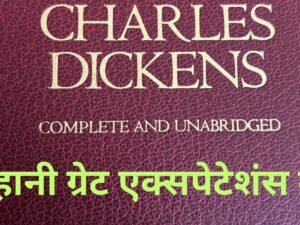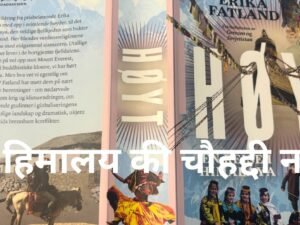पंद्रह वर्ष पहले प्रगति मैदान से एक किताब लाया था- दिल्ली जो एक शहर है (महेश्वर दयाल)। उसमें पुरानी दिल्ली की संस्कृति लिखी थी कि क्या होता जब घर में कोई किन्नर/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर बच्चा जन्म लेता। उसका परिवार उसकी पहचान यथासंभव छुपा कर रखने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठता, और उसे किन्नर सिंडिकेट उठा कर ले जाते। जबरन छीन कर। चाहे वह किसी रईस घर का हो या गरीब घर का, अगर वह किन्नर है तो उसका समाज अलग है। लेकिन, ऐसे लोग आखिर जाते कहाँ हैं? क्या वे बस-ट्रेनों में समूह बना कर, ताली पीटते, पैसे माँगते घूमते हुए जीवन बिता देते हैं? क्या उनका कोई स्पेशल स्कूल है? उनके दोस्त कौन होते हैं? क्या भारत के बाहर भी यही प्रणाली है?
पुस्तक ‘पोस्ट बॉक्स नं 203 नाला सोपारा’ को जब साहित्य अकादमी पुरस्कार (2018) मिला तो इसका शीर्षक देख कर बहुत आकर्षित हुआ। मगर जैसा पुरस्कृत किताबों के साथ कई बार होता है, ऐसे आक्षेप दिखने लगे कि सत्ता से नजदीकी की वजह से मिल गया। सरल सपाट गद्य को पुरस्कार दे दिया गया। मैंने भी इसके बाद यह जानने की कोशिश नहीं की इस किताब में है क्या।
स्टोरीटेल ऑडियो पर यह किताब नज़र आयी, तो सुनने लगा। एक किन्नर और उसकी माँ के बीच चिट्ठियों से संवाद। कोई भारी-भरकम संवाद नहीं। जैसे आत्मीय और रोजनामचा चिट्ठियाँ होती हैं, वैसी ही। आज और कल का ब्यौरा। एक किन्नर का। एक किन्नर के उस परिवार का जो कहीं छूट गया। मुझे मशहूर दास्तानगो हिमांशु वाजपेयी ने बताया कि इस कहानी को पढ़ कर उन्हें रुलाई आ गयी थी। यह संवाद किसी को भी नम कर देगा, जब एक संतान अपने उन पिता, उन भाई, उस समाज को बड़ी सहजता से याद करता है जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था। वह अपने उस भतीजे के जन्म के लिए आशान्वित है, जिसका वह कभी मुँह भी नहीं देख पाएगा। वह समाज से छुपा कर अपनी माँ को चिट्ठी लिख पा रहा है, लेकिन फ़ोन पर दो शब्द कहने-सुनने की इजाज़त नहीं।
मुझे शंका थी कि यह संवाद यूँ ही गोल-गोल घूमता न रह जाए। जब उसे उठा कर ले जाया गया, तो किसी सरकारी या विशेष फ़ैसिलिटी में तो नहीं ले जाया गया। फिर शिक्षा-दीक्षा और करियर का क्या? एक चिट्ठी के अनुसार वह गणित में इतना तेज़ था कि उसने गणितज्ञ शकुंतला देवी से संपर्क किया था। मगर यह तो तब की बात थी जब उसका लिंगदोष सार्वजनिक नहीं हुआ था। अब वह किन्नरों के बीच था, और उसके लिए गणित पढ़ना मुनासिब नहीं था। लेकिन वह पढ़ता है। छुप-छुप कर अपनी राह बनाता है। इग्नू (IGNOU) नामक संस्था से पत्राचार कोर्स कर पढ़ाई करता है।
इसे आगे पढ़ते हुए लगता है कि वह तो शिक्षा, श्रम और करियर में उतना ही सक्षम है, जितने अन्य। हाशिए पर धकेले जाने के बाद भी वह गाड़ी सफाई कर कमाता है। पढ़ाई करता है। नयी दुनिया के कंप्यूटर से संवाद करता है। रोजगार पाता है। अपने दोस्तों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भला वे क्यों घर-घर घूम कर नाच-गा कर जीवन गुजारें? वे भी स्कूल जाएँ, बिजनेस करें, काम पर जाएँ, चुनाव लड़ें। समाज में उनकी भूमिका आखिर स्टीरियोटाइप और अलग-थलग क्यों हो? इससे भला किसका होगा?
उपन्यास का स्वर इतना सहज है कि कुछ स्थानों पर वह खटकता भी है। ख़ास कर अगर पाठक की सोच स्टीरियोटाइप प्रगतिवादी हो। इसमें कहीं भी विनोद उर्फ़ बिन्नी उर्फ़ बिमली को कोई क्रांतिकारी या चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं दिखाया। वह सिस्टम से लड़ता नहीं कि उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। बल्कि जब उसके दोस्त पूनम के साथ यौन हिंसा होती है, वह प्रतिकार नहीं करता। वह इसे समाज का ऐसा रोग मानता है, जो एक पल में नहीं खत्म हो सकता। वह सभी तिरस्कार, हिंसा और अन्याय को स्वीकारते हुए आगे बढ़ता है। जब इस तरह धक्के खाते वह अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है, तो समाज की शक्ल भी जैसे अपने-आप बदलती दिखायी देती है। जैसे कहते हैं खुद को बदलो, समाज भी बदलेगा, वह किन्नरों को भी स्ट्रीमलाइन में आने के लिए आह्वान करता है।
मुझे इस उपन्यास को सुन कर लगा कि कहानी बिंबों और अलंकारों के ताने-बाने से कम, मानवीय संवेदनाओं की जड़ तक पहुँच कर अधिक गढ़ी जानी चाहिए। ख़ास कर अगर उसका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना हो। प्रगति करना हो। ऐसा अभिनेता उत्पल दत्त को कहते सुना था कि कई बार हम हर चीज को इतना प्रबुद्ध (intellectualise) करने की कोशिश करते हैं, कि उससे लोक जुड़ ही नहीं पाता। इस कहानी में वह ख़ामख़ा तत्व कम है, और इससे किसी भी उम्र, किसी भी अर्हता, किसी भी समाज के लोग बहुत आसानी से जुड़ते जाएँगे। यह कहानी उन्हें जीवन भर याद भी रहेगी।
Author Praveen Jha shares his experience about book Post Box no 203 Nala Sopara by Chitra Mudgal.