कुछ किताबें हम इतनी बार देख चुके होते हैं कि शुबहा होता है हम पढ़ चुके हैं। अनुराधा बेनीवाल की ‘आज़ादी मेरा ब्रांड’ के बारे में इतना सुन रखा था कि कभी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। लगा कि मेरे लिए आखिर इस किताब में क्या नया होगा। किसी ने यूरोप घूमने के अनुभव लिखे, और मैं तो रहता ही यूरोप में हूँ। जिन जगहों में वह घूमी होगी, जो संस्कृति देखी होगी, जो तुलनाएँ की होगी, वह तो मैं सब देख और महसूस कर ही चुका हूँ। मगर किताबों के साथ एक ऐसी भौतिकी होती है कि आप उससे दूर जाते-जाते भी एक दिन उससे टकरा जाते हैं। ख़ास कर अगर किताब ही घुमक्कड़ी की हो।
बहरहाल हुआ यूँ कि एक यायावर मिज़ाज के व्यक्ति अखिल रंजन यूरोप की यात्रा करते हुए नॉर्वे आए। उन्होंने इस किताब की चर्चा की। मैं उनके साथ ही गाड़ी में यात्रा करते हुए स्टोरीटेल पर यह किताब सुनने लगा। मैंने पहले कुछ अध्याय सुन कर कहा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। इसे भारत में रहने वाले ही पसंद करेंगे।
लेकिन सोचा कि किताब पूरी कर लेता हूँ। धीरे-धीरे मेरे पूर्वाग्रह टूटने लगे। लगा कि यात्राएँ एक जैसी होकर भी कितनी अलग होती है। स्थान एक होकर भी अलग होते हैं। दो लोगों को एक ही चीज अलग दिख सकती है। ख़ास कर जब एक भारतीय पुरुष और एक भारतीय स्त्री अलग-अलग यात्रा कर रहे हों, तो उनके अनुभव बिल्कुल ही दो ध्रुव पर हो सकते हैं।
अनुराधा की किताब का मूल तत्व ही एक असंभव कल्पना लगने लगती है। एक भारतीय (विवाहित?) लड़की कम बजट पर अकेली यूरोप में भटक रही है। हॉस्टलों और कम्युनिटी डॉर्म में वक्त गुजार रही है। अनजान लड़कों के बीच देर रात तक रह रही है। एक-दो नहीं, दर्जनों स्थानों में घूम रही है। यूरोप को पूरब से पश्चिम तक नाप रही है। निर्भय, निःसंकोच, निश्चिंत। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या यह कर पाता? यह सोचते ही एक झुरझुरी सी कौंध गयी।
एम्सटरडम, पेरिस, प्राग, वियना इत्यादि के चक्कर मैंने भी लगाए हैं। अकेले घूमा हूँ। संस्कृतियों की तुलना की है। संस्मरण लिखे हैं। लेकिन मेरे फलक में इतिहास और समाज के अन्य पहलू अधिक हैं। जब मैं रेड लाइट एरिया में एक युवती (वेश्या) से मिलता हूँ, तो एक पुरुष ग्राहक की निगाह से मिलता हूँ। एक स्त्री उसी स्थान पर उसी युवती को अलग नज़रिए से देखती है। वह इस तिलिस्मी दुनिया को उस भाव से सामने रखती है, जो मेरे लिए समझना कठिन है। तमाम किताबों में वह बातें नहीं लिखी कि मैं पढ़ कर वह दृष्टिकोण बना सकूँ।
मैं कहीं न कहीं इस पुस्तक में इतिहास की बारीकियाँ तलाश रहा था, मगर यह यात्रा कुछ तेज गति से की गयी है, तो इतिहास कुछ हवा के झोंके जैसा ही है। बर्लिन की दीवार कब आयी, और कब गयी, यह पता नहीं लगता। मगर यह अच्छा ही है कि इसे ख़ामख़ा ज्ञान से सराबोर नहीं किया। यात्रा के मानवीय पहलुओं पर बातें की गयी।
आखिरी पड़ाव में धर्म और पितृसत्ता पर संवाद और आत्म-संवाद है। वह मीमांसा से आक्रोश की तरफ़ बढ़ता दिखता है। भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए ललकारता है। यह लेखक के कलम रखने की अपनी शैली होगी कि काग़ज़ पर चाकू की तरह गोद-गोद कर आख़िरी पन्ने लिखें जाएँ। मगर ऐसा लगा कि वह उसी सहजता से भी हो सकता था, जैसी बाकी किताब थी।
बहरहाल यह किताब अब पुरानी हो चुकी है, और लेखक का नया संस्मरण भी प्रकाशित हो चुका है। संभवतः ये दोनों किताबें बैक-टू-बैक पढ़ने लायक हों। मगर वह किताब अभी मेरे हाथ आयी नहीं है।
एक ज़रूरी किताब। यात्रा से आगे। यात्रा से अलग। एक ख़ूबसूरत यात्रा।
Author Praveen Jha shares his experience about book Azaadi Mera Brand by Anuradha Beniwal published by Rajkamal Prakashan.



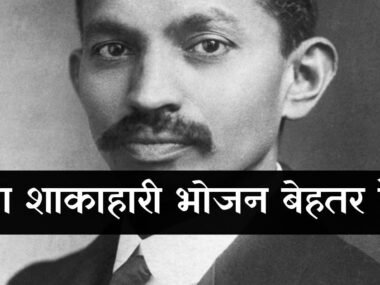
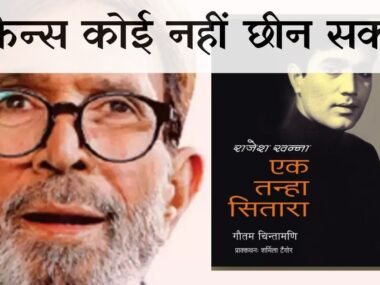


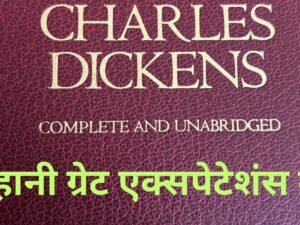

1 comment
इस सिरीज की दूसरी पुस्तक “लोग जो मुझ में रह गये” भी यूरोप में घुमक्कड़ी जीवन का वृतांत है। इसमें यात्रा के दौरान मिले अलग-अलग क़िस्म के लोगों एवं उन लोगों की समझ को पुस्तक में बढ़िया तरीक़े से प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय सामाजिक सोच के बारे में लेखिका का ग़ुस्सा यहाँ भी उसी रूप में प्रस्तुत है और जायज़ भी लगता है (तब तो और लाज़िमी हो जाता है जब किसी ने यूरोपीय आबो-हवा की आज़ादी को दिल से महसूस किया हो।)