यह ऐसा क्षेत्र था, जिसमें मैंने कदम रखा नहीं था। विस्तृत संदर्भ-सूची (सौ से अधिक) में एक महत्वपूर्ण पुस्तक ज़रूर कुछ महीने पहले पढ़ी, लेकिन वह लोकगीतों की समझ के लिए थी। स्त्रीवाद पर अब तक कुछ व्यवस्थित नहीं पढ़ना एक पाठकीय ग्लानि तो दे गया। मेरी गति मद्धिम हो गयी, और प्रथम पाठ में भी बीस घंटे लग गए!
इस पुस्तक से परिचय कुछ यूँ हुआ कि मैंने एक प्रश्न सुना, “हिंदी फ़िल्मों में अब तक स्त्री गीतकार की संख्या क्यों नगण्य है, जबकि गीत लिखना तो स्त्री के लिए सहज रहा है?”
एक पाठ का अनुमोदन मिला, तो धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया। पुस्तक की शुरुआत बहुत ही कैजुअल ढंग से सोशल मीडिया विमर्शों को सम्मिलित करते हुए होती है जब एक प्रश्न रखा जाता है- “लिखना स्त्री के लिए क्या है? कोई सत्ता है जो इससे मिलनेवाली है?“ [उत्तर के लिए पुस्तक पढ़ें]
उसके बाद आगे एक झकझोर देने वाला कथन है- “मनुष्यों के बीच लैंगिक आधार पर भेदभाव दमन का प्राचीनतम रूप है”
इस कथन के साथ ही पुस्तक आदिम मानवों के ‘हंटर-गैदरर’ जीवन शैली में ले जाती है, जब पुरुष ‘हंटर’ और स्त्री ‘गैदरर’ बनी। कार्य-विभाजन की प्राचीनतम पद्धति, जो लिंग के आधार पर जन्मने लगी। ‘सेक्स’ और ‘जेंडर’ के फाँक बनने लगते हैं, एक जो पैदाइश से मिली, दूसरी जो समाज ने दी।
इस भूमिका के बाद पुस्तक साहित्य की गहराइयों में ले जाती है, जिसे तीन खंडों में बाँटा गया है- पद्धति, परंपरा और पाठ।
पद्धति में जो भी पाश्चात्य या भारतीय मॉडल बने हैं या नहीं बने, उनकी विवेचना है। कई मूलभूत बातें गिरह खोल कर समझायी गयी हैं- जैसे स्त्री लेखन (ecriture feminine) और स्त्रीवादी लेखन का अंतर क्या है? स्त्रीवाद की परिभाषा क्या है? भारतीय मॉडल क्या होगा? लेखक पूछती हैं- ‘दलित साहित्य अंबेडकर, ज्योतिबा फुले या बुद्ध के दर्शन अपनाती है। स्त्रीवादी साहित्य ने किन्हें अपनाया?’
उन्होंने एक पश्चिमी संदर्भ दिया कि स्त्री-लेखकों की अस्सी प्रतिशत पाठक स्त्री ही होती है। भारत में स्त्री-लेखन के समालोचक भी अधिकांश पुरुष ही रहे, जो अपने खाँचे और सहूलियत से इसे देखते रहे। वहीं एक उद्धृत कथन है- ‘स्त्री विमर्श से दयनीय कोई विमर्श नहीं’।
दूसरा खंड यानी ‘परंपरा’ मेरे लिए अधिक सहज और रुचिकर था। इसमें प्राचीन काल से स्त्री-लेखन पर चर्चा है, जिसमें बौद्ध थेरी गाथाएँ, ललद्यद, मीरा, ताज, मुद्दुपलानी, कई स्त्रियों के लेखन पर रोचक चर्चा है। पढ़ कर लगता है कि वाकई ‘हिंदी साहित्य का आधा इतिहास’ (जो एक पुस्तक भी है) कितना समृद्ध है। लेखक पूछती हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ सभी जानते हैं, खगनिया की पहेली कितने लोग जानते हैं? इसी खंड में एक कथन इसका आंशिक उत्तर है-
‘पुरुष का समय ऊर्ध्व दिशा में बढ़ता है। स्त्री का समय वृत्ताकार घूमता है’
मुझे महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान का अ-तुलनात्मक अध्ययन भी खूब भाया। वह लिखती हैं-
“सुभद्राकुमारी चौहान और महादेवी वर्मा समकालीन थीं और दोनों भिन्न प्रतिभाओं की कवि थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ीं। दोनों सखा। दोनों का नाम हिन्दी की आधुनिक कविता के इतिहास में अमिट हो गया। हम कथा साहित्य में प्रेमचन्द और प्रसाद की परम्पराएँ पढ़ते हैं, हिन्दी स्त्री कविता का स्वाभाविक विकास होता तो सुभद्राकुमारी और महादेवी की दो भिन्न परम्पराएँ विकसित होतीं कौन जाने!”
उसके बाद वह चिंता जताती हैं कि इन दोनों के बाद जहाँ स्त्री-लेखन को नयी ऊँचाइयाँ पानी थी, वह ढुल-मुल क्यों हो गयी?
मेरे लिए सबसे कठिन रहा तीसरा खंड यानी ‘पाठ’। हालाँकि साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह सबसे ज़रूरी खंड है, जहाँ कुछ चुनिंदा समकालीन कवियों के पाठ हैं। एक-एक कविता चुन कर उसे कुशल शिक्षक की तरह समझाया गया है। मगर मेरे सामने चूँकि वह पूरी कविता नहीं थी, तो उसे संदर्भित करना कठिन हो रहा था। अब मैं वे कविताएँ मंगा कर दुबारा उन्हें पढ़ूँगा तो यह रोचक पाठ होगा। ख़ास कर आदिवासी स्त्री कविता पर लेखक भी ठिठक जाती हैं कि इनका मॉडल आखिर क्या हों? वहाँ तो द्वंद्व ही अलग है। लेकिन, उसके कठिन गाँठ भी धीरे-धीरे सुलझाने का प्रयास करती हैं।
हर स्त्री जो लेखन-पठन से जुड़ी हैं, वह इसे अपनी सूची में रख सकती हैं। इसलिए भी कि इस पुस्तक की संदर्भ सूची एक बोनस पैकेज है। पुरुषों के पढ़ने का तर्क मेरी नज़र में तो यही है कि किताबों के अंबार लगाने वाले पुरुषों की भी स्त्रीवाद पर कितनी समझ है? यह तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ शंकराचार्य से सिगमंड फ्रायड तक उलझ गए।
धीरे-धीरे कदम रखिए। एक के बाद एक पढ़िए। इसे ‘लूज टॉक’ न बना कर, समझ-बूझ कर दो पंक्ति कहें। पुरुष की समझ में यह कमजोरी तो है ही कि वह स्त्री नहीं है।
[यह पुस्तक Rajkamal Prakashan Samuh से प्रकाशित है]
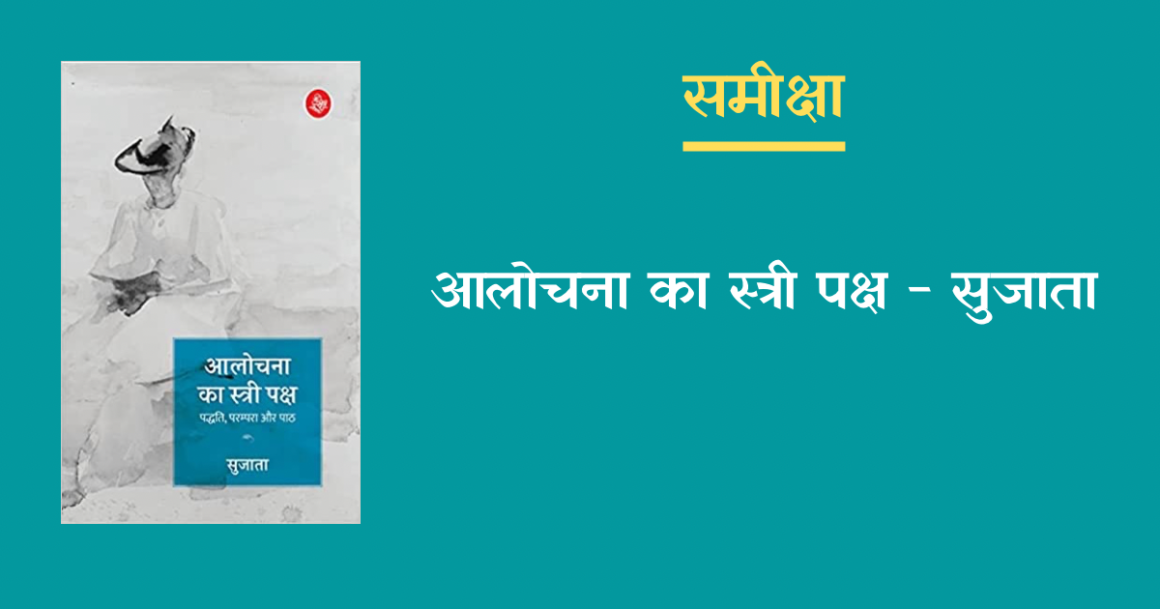
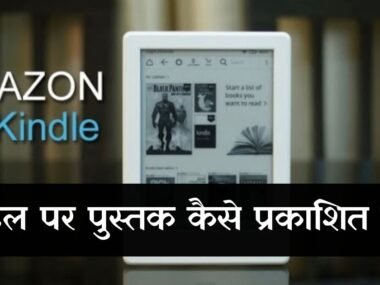
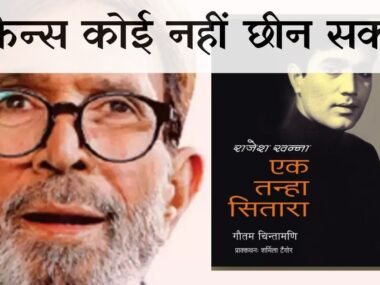
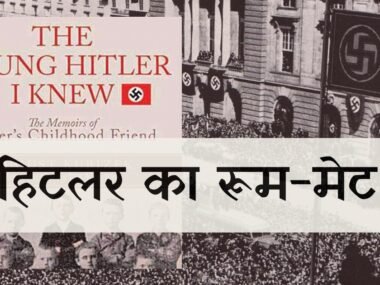
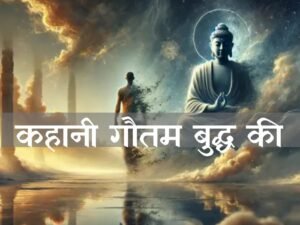
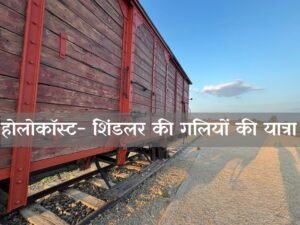
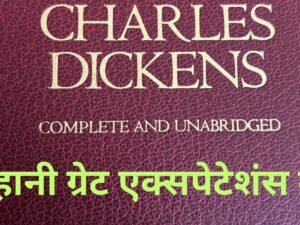
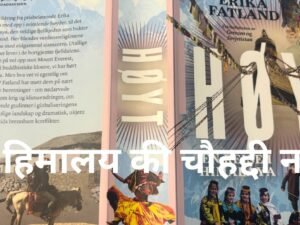
1 comment
Hi