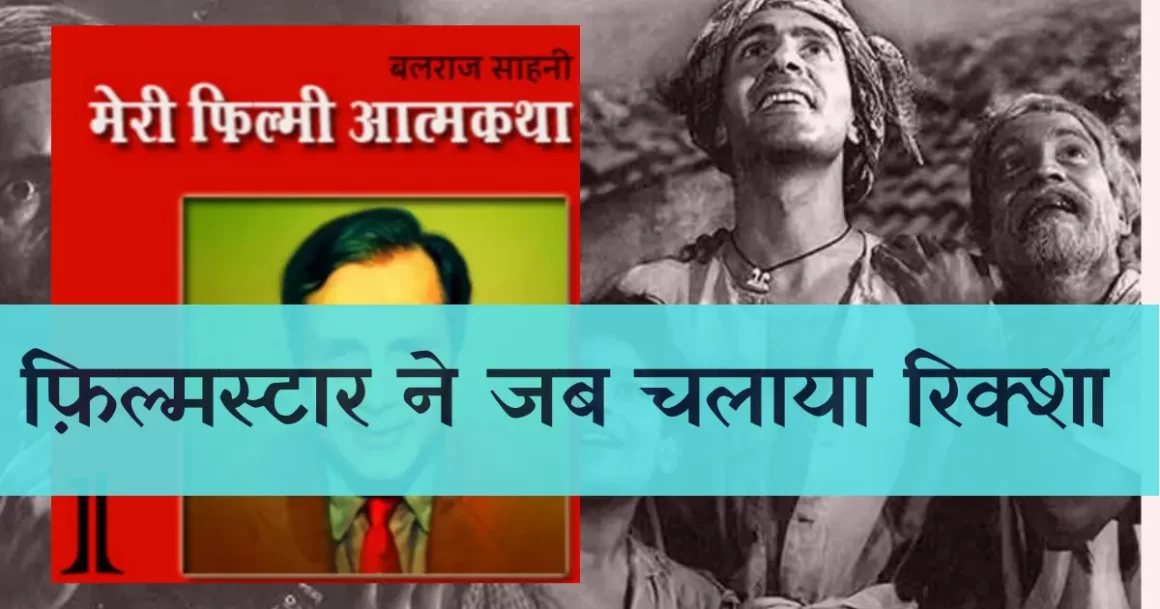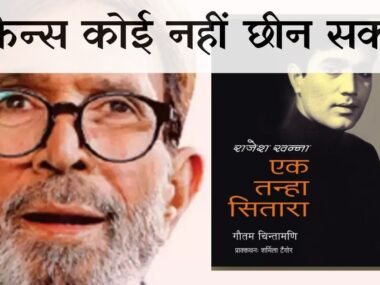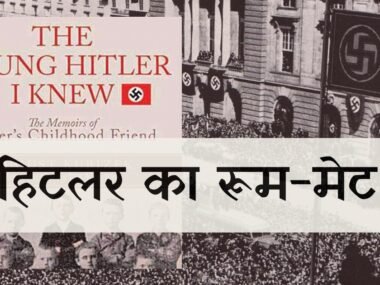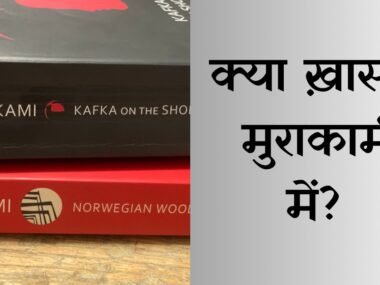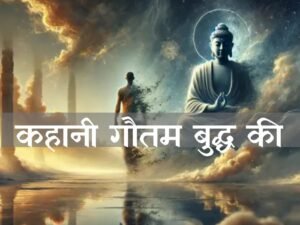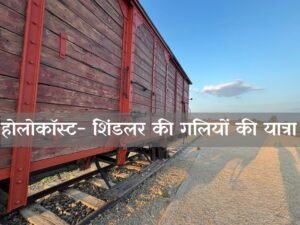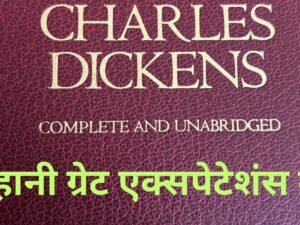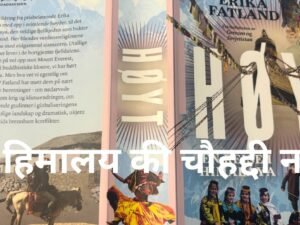मैंने सिनेमा हॉल में फ़िल्में देखनी देर से शुरू की। इसकी एक वजह यह थी कि नयी फ़िल्मों की टिकटों के लिए छोटे शहरों में मारा-मारी बहुत होती थी। ऐसा अक्सर होता कि जब तक हम काउंटर तक पहुँचते, टिकटें खत्म हो जाती। ब्लैक में टिकटें बिकती, लेकिन परवरिश कुछ यूँ थी कि यह बात अनैतिक लगती। वहीं कुछ दूर एक और सिनेमा हॉल था, जहाँ कोई भीड़-भाड़ नहीं होती। मैं और मेरे भाई वहीं जाने लगे। वहाँ टिकटें सस्ती थी, बड़े आराम से मिल जाती और सिनेमा हॉल भी खाली पड़ा होता।
इन फ़िल्मों में सबसे पहले देखी ‘मर्यादा’ जिसमें माला सिंहा, राजेश खन्ना और राजकुमार थे। इसके बाद देखी ‘एक फूल दो माली’। मुझे याद है उस फ़िल्म में अच्छी-ख़ासी भीड़ भी आ गयी थी। जबकि ये दोनों फ़िल्में मेरी पैदाइश से एक दशक पुरानी थी। दूसरी फ़िल्म में मुझे बलराज साहनी अभिनीत किरदार पसंद आए थे। हालाँकि संजय ख़ान जैसे पठान हीरो भी इस फ़िल्म में थे। लेकिन, बलराज साहनी के सूट-बूट-बंगले में भी जैसे एक मध्य-वर्ग पिरोया हुआ था।
इस बात को अब कुछ दशक बीत गए और मैंने बलराज साहनी की दर्जनों फ़िल्में देख ली। उनमें से अधिकांश में तो वे थोड़ी देर के लिए ही नज़र आते। इन्हें ‘चरित्र अभिनेता’ कहा जाता। मुख्य अभिनेता चोर हो सकता था, शातिर हो सकता था, अश्लील और हिंसक हो सकता था। लेकिन चरित्र अभिनेता हमेशा चरित्रवान ही होते। इसलिए अभिभावक भी यही जोर देते कि इनकी तरह बनो। बलराज साहनी की तरह।
जब मन में ऐसी बातें गढ़ जाती तो क्रिकेट के खेल में भी सचिन और सौरव के बजाय राहुल द्रविड़ पसंद आने लगते। यह अच्छा हुआ हो या बुरा, लेकिन जीवन का कुछ ऐसा ही मूल्य बनता गया। अगर भटकाव हुए भी तो रास्ते पर आता रहा।
बलराज साहनी का लिखा कभी ढंग से पढ़ नहीं पाया था। उनके छोटे भाई भीष्म साहनी मुझे बहुत पसंद थे। उनका उपन्यास ‘तमस’ छुटपन में ही बाँच गया था, और उसके किरदार जरनैल का अभिनय करने का भी प्रयास करता। विदेशों में प्रवास के बाद उनकी कथा ‘ओ हरामजादे’ ने बहुत साथ दिया। इस कथा का नाम यह क्यों है, यह तो पढ़ कर पता लगेगा। इस कथा के नाम पर एक संस्मरण मैंने नीदरलैंड यात्रा में भी लिखा।
बलराज साहनी का लिखा (या कहा) कुछ ही वर्षों पहले पढ़ा। वह कभी घोर कम्युनिस्ट रहे थे, और बाद में उसके आलोचक बने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के दीक्षांत समारोह में दिया उनका वह भाषण ज़रूर पढ़ना चाहिए।
इरफ़ान से अच्छे कथावाचक और साक्षात्कार लेने वाले विरले ही होते हैं। उनको तो सिर्फ़ इसलिए देख या सुन लेना चाहिए, ताकि पता लगे बोला और सुना जाता कैसे है। कितना विराम, कितना उतार-चढ़ाव, कितनी गंभीरता, कितना विनोद और कितना प्राकृतिक संवाद। राज्यसभा टीवी के सफ़र के बाद इरफ़ान साहब ने अपने पॉडकास्ट शुरू किए हैं। मैं उन्हें गाड़ी चलाते वक्त, कंप्यूटर पर बैठे हुए, टहलते हुए सुनता रहता हूँ।
उन्होंने बलराज साहनी की फ़िल्मी आत्मकथा पढ़ कर सुनायी। उन्नीस छोटे-छोटे एपिसोड में। इसे सुन कर लगा कि फ़िल्मी दुनिया तो बलराज के जीवन का उत्तरार्ध है। उससे पहले तो बलराज एक कथाकार, एक बीबीसी अनाउंसर, एक कम्युनिस्ट, एक रंगकर्मी, और कई अन्य चीजें थे। वे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय लंदन में थे, और लाइव ऐक्शन देख रहे थे। आज़ादी के बाद जब कम्युनिस्टों को जेल में डाला गया, वह जेल में थे। बल्कि जेल से एक घंटे की छुट्टी लेकर शूटिंग में जाना शुरू किया!
वे फ़िल्मों में तब ठीक से आने शुरू हुए जब अभिनेत्री पत्नी का देहांत हो चुका था, बेटे परीक्षित साहनी बाल-कलाकार बन चुके थे, और बलराज के बाल पक चुके थे। उन्होंने जीवन भर अपने बाल रंग कर अभिनय किया। इस आत्मकथा की शुरुआत भी वहीं से होती है जब वह मेकअप रूम में बैठे बाल रंग रहे होते हैं। अपने समय की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी तंज करती है- ‘क्या दिन आ गए। अब अपनी किस्मत में मुआ बलराज ही लिखा है’
यह अपनी कमियों को बिना लाग-लपेट के कहते हुए बहुत ही ईमानदार आत्मकथा है। चरित्र अभिनेता बलराज साहनी का वास्तविक चरित्र आखिर कैसा था, यह उभर कर आता है।
अपनी कालजयी फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ की शूटिंग में निर्देशक बिमल राय चाहते थे कि बलराज साहनी यथार्थ लाएँ।
बलराज कलकत्ता की सड़कों पर असल सवारी लेकर हाथ-रिक्शा खींचते हुए धूप में चल रहे थे। पीछे गाड़ियों में छुपे कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही थी।
बलराज थक कर चूर हो गए। वह रुक कर एक दुकान पर दूध पीने के लिए गए।
उन्हें दुकानदार ने दुत्कार दिया। उन्होंने पैसे निकाल कर दिए। फिर भी उन्हें दुकानदार ने डाँट कर भगा दिया। वह आगे एक दुकान पर सिगरेट का एक पैकेट माँगने गए। दुकानदार चौंक गया कि यह रिक्शे वाला सिगरेट कैसे माँग रहा है। उन्होंने जो पाँच रुपया निकाल कर दिया, उसने अलट-पलट कर देखा। उसे शक हुआ कि यह चुरा कर लाया होगा या नकली नोट दे रहा है।
वह आगे चौरंगी में उसी वेश-भूषा में हाथ-रिक्शा लिए चल रहे थे। वहाँ उन्हें और निरुपा राय को देख कर भीड़ जमा हो गयी। विमल रॉय ने उन दोनों को एक रेस्तराँ में जाकर बैठने कहा। वे जब पसीने से लथ-पथ फटी बनियान और गमछा लिए रेस्तराँ में दाखिल हुए, उन्हें वहाँ भी प्रवेश नहीं मिला।
बलराज ने लिखा- मुझे उस दिन लगा कि गरीबी ऐसी चीज है कि आदमी पैसे देकर भी कुछ नहीं खरीद सकता।
Author Praveen Jha shares his experience about film autobiography of Balraj Sahni