देश की समृद्धि का रास्ता गाँव के खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है
– चौधरी चरण सिंह
भारत में किसान ‘अन्नदाता’ कहलाते रहे हैं। इस नामकरण ने अच्छा-बुरा जो भी किया हो, किसान की छवि एक दीन-हीन छवि वाले गरीब व्यक्ति की बना दी है। क्या वाक़ई किसान की यही नियति रही है? क्या किसान होना दीन-हीन होना है? अगर किसान समृद्ध नहीं हुए, तो देश कैसे समृद्ध होगा?
मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है,
“हो जाये अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहाँ
खाते, खवाई, बीज ऋण से हैं रंगे रक्खे जहाँ
आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में
अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में
बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा
है चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा
देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे
किस लोभ से इस आँच में, वे निज शरीर जला रहे”
यह कविता यूट्यूब पर सुनने के लिए क्लिक करें
आज भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है, और सकल घरेलू उत्पाद के 18 प्रतिशत तक की भागेदारी दे रही है। अगर हम तीन-चार दशक पीछे चले जाएँ, तो भारत कृषि-प्रधान देश रहा है और अधिकांश भारतीयों के पूर्वज खेती-बाड़ी करते रहे हैं। अस्सी के दशक तक उत्तर प्रदेश की तीन चौथाई जनसंख्या कृषि से जुड़ी थी। हरित क्रांति के बाद भारत एक निर्यातक देश भी बन गया। आज जो शहरी आधुनिक भारत हमारे सामने है, उसकी नींव इन खेतों में ही है।
लेकिन, इस देश में सेना, शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनियर, और तमाम अन्य दिवस तो मनाए जाते रहे, लेकिन किसान दिवस नहीं मनाया जाता था।
2001 से ही हर 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस की तरह मनाना शुरू किया गया। किसान दिवस अगर नहीं मनाया गया, इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के किसान कभी एकजुट होकर रहे ही नहीं। यह भारत का सबसे बड़ा असंगठित व्यवसाय कहा जा सकता है। इतने वर्षों से चल रहे इस व्यवसाय में एक मज़बूत संगठन क्यों नहीं बन पाया?
अमरीकी समाजशास्त्री बैरिंगटन मूर जूनियर इस विषय में लिखते हैं, “भारतीय समाज में जातिवाद इतना गहरा है कि एक बैनर तले सभी किसानों को लाना नामुमकिन है”
आज भी ये सवाल उठते हैं कि पंजाब से किसान विरोध करने आए, मगर तमिलनाडु या बिहार से क्यों नहीं आए? जाट आए, मगर अन्य जातियाँ क्यों कम आयी? विरोध तो पहले भी ऐसे ही बँट कर होते रहे हैं, भले ही समस्या पूरे देश की हो।
1919-20 में एक बड़ा किसान आंदोलन अवध में हुआ। उस समय फ़िजी देश में गिरमिटिया मजदूरी कर लौटे बाबा रामचंद्र ने किसानों के शोषण के खिलाफ़ बीड़ा उठाया। उन्होंने संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में घूम-घूम कर किसान सभाएँ और पंचायत आयोजित की। किसानों ने सामंतों और अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह किया, जिसे अंग्रेज़ों ने बल-प्रयोग से दबा दिया। कांग्रेस स्वयं सामंतों के चंदे पर काफ़ी हद तक आश्रित थी, तो वह भी मदद नहीं कर पायी। काशी विद्यापीठ के उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी की उपस्थिति में किसान नेता बाबा रामचंद्र की गिरफ़्तारी हुई।
पुस्तक अवध का किसान विद्रोह के लिए क्लिक करें
बाद में गांधी के अनुयायी चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता बन कर उभरे। उन्होंने 1939 में ऋण विमोचन (debt redemption) और भूमि उपयोग (land utilisation) जैसे अधिनियम लाने में मदद की। आज़ादी के बाद जब वह कृषि मन्त्री बने, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से ज़मींदारी प्रथा खत्म करने का बीड़ा उठाया। 1950 में लाया गया ‘उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम’ इस दिशा में एक मील का पत्थर था। हालाँकि उत्तर प्रदेश में लेखपाल व्यवस्था के कारण इस अधिनियम में कई भ्रष्ट ‘लूपहोल’ थे। इतिहास गवाह है कि आखिर कितनी ज़मींदारी खत्म हुई। चौधरी चरण सिंह के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सके।
संवैधानिक क़ायदे-कानून अपनी जगह थे। यक्ष प्रश्न तो ज्यों का त्यों था। किसान संगठित कैसे हों?
इतने बड़े देश में ऐसा संगठन होना कठिन है, ख़ास कर जब अधिकांश किसान कम पढ़े-लिखे या निरक्षर हों। भारत का सबसे पुराना व्यवस्थित किसान संगठन अगर ढूँढें, तो 1929 में सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा (पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा) का नाम ले सकते हैं। इस संगठन से समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण भी जुड़े थे। बाद में इस संगठन पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया, और समाजवादी नेता इससे छिटक गए। आज के समय यह कम्युनिस्टों के दो फाँक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में बँट चुका है। ऐसा नहीं कि वे माँग नहीं उठाते, आंदोलनों में लाल झंडा तो लहराते ही हैं। लेकिन, देश के किसान-वर्ग पर इनकी पकड़ सीमित ही कही जाएगी।
समस्या यह है कि राजनैतिक दलों से जुड़ते ही किसानों के अधिकार से अधिक राजनैतिक लामबंदी शुरू हो जाती है। अगर वामपंथी किसान संगठन हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन भी हैं। सभी मुख्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अपने किसान विंग बने हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक आदि के अपने-अपने किसान संगठन हैं।
कुछ व्यक्ति-विशेष के बनाए छोटे कृषक संगठन भी हैं। पिछले दशक में योगेंद्र यादव का स्वराज अभियान उभरा है। आज देश में सौ से अधिक कृषक संगठन बिखरे पड़े हैं, और उनका एक साझा प्लैटफ़ॉर्म नहीं। जब कोई अत्याचार होता है, किसानों की मौत होती है, तब जाकर उन्हें एक होने का ख़याल आता है।
उदाहरणार्थ जब 2017 में कथित पुलिस फ़ायरिंग में छह किसानों की मृत्यु हुई तो देश के 130 किसान संगठनों ने मिल कर ‘ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमिटी’ बनायी। यह कमिटी भी ‘कृषि बिल’ के मुद्दे पर एक साथ नहीं रही। सच यही है कि संगठन भले ही दर्जनों हों, उनमें न एकजुटता है, न उनका एक साझा एजेंडा है, और न ही ऐसी कमिटी या नेता है जो सरकार से सीधे वार्तालाप कर मामला सुलझा सके।
आज़ादी के बाद पूरे उत्तर भारत में एक भी दमदार संगठन नहीं था। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्यों में भी नहीं। यह शुरुआत 1972 में भूपिन्दर मान और कुछ उनके साथी कृषकों ने की, जब उन्होंने पंजाब खेती-बाड़ी यूनियन बनाया। हरियाणा में भी एक किसान संघर्ष समिति बनी। संगठनों का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि उत्तर भारत में हरित क्रांति का लाभ इन्हीं दो राज्यों ने सबसे अधिक उठाया।
चौधरी चरण सिंह खेती-बाड़ी की दुनिया से अधिक राजनीतिक गलियारों में समय बिता रहे थे। 1967 में कांग्रेस से अलग होकर वह उत्तर प्रदेश के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1974 में भारतीय लोक दल की नींव रखी, और जनता पार्टी सरकार में जुड़ कर अति-अल्पकालिक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। 1978 में पंजाब खेती-बाड़ी यूनियन को लोक दल के किसानों से मिला कर उन्होंने एक ‘भारतीय किसान यूनियन’ की स्थापना की। इस माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान कुछ एकजुट हुए, जो स्थिति आज-तक दिखती है। भारतीय किसान यूनियन भी उस समय कई थे। 1980 में आंध्र प्रदेश के सी नारायणस्वामी नायडू ने ‘इंडियन फार्मर्स यूनियन’ की स्थापना की थी, जिसका शब्दार्थ भारतीय किसान यूनियन है। 1981 में हरियाणा के राव हरलाल सिंह ने भी एक भारतीय किसान यूनियन बनाया। एक नाम से इतने यूनियन बन गए कि यह बताना कठिन था, असली कौन सा है।
1980 में एक अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अतिरिक्त हरियाणा की कृषक संघर्ष समिति, कर्नाटक की रायतु संघ, और तमिलनाडु की व्यवसायीगल संघम शामिल थे। यह पहला मौका था जब उत्तर से दक्षिण तक के किसान एक मंच पर आए थे। लेकिन, इस यूनियन में भी फाँक होने लगे। उन दिनों महाराष्ट्र के एक बड़े किसान नेता हुआ करते- शरद अनंतराव जोशी। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों का शेतकारी संगठन बनाया था। उन्होंने 1982 में पुन: सभी राज्यों के किसानों को एक मंच पर लाकर एक समन्वय समिति बनायी। यही तय हुआ कि हर राज्य के भिन्न किसान यूनियन एक समिति के माध्यम से जुड़े रहेंगे।
मगर एक नेता की कमी खल रही थी, जो उत्तर भारत के किसानों को जोड़ सके। चौधरी चरण सिंह बूढ़े हो चले थे। 1985 में उनको लकवा मार गया, और धीरे-धीरे वह मृत्युशय्या पर चले गए। उनके बेटे अजीत सिंह उत्तराधिकारी तो थे, मगर वह ठहरे IIT से पढ़े, IBM कम्पनी में काम कर चुके कम्प्यूटर इंजिनीयर। उनकी जमीन पर पकड़ कमजोर थी। वह आख़िर क्या प्रतिनिधित्व करते? तभी आए महेंद्र सिंह टिकैत!
17 अक्तूबर 1986 को सिसौली गाँव में महेंद्र सिंह टिकैत ने ‘भारतीय किसान यूनियन’ बना कर उसे ‘ट्रेड यूनियन ऐक्ट’ के तहत पंजीकृत करा लिया। भले ही संगठन का नाम ‘भारतीय किसान यूनियन’ था, इनका क्षेत्र मुख्यत: पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले थे। सामान्य सदस्यता शुल्क पाँच रुपया रखा गया, और आजीवन सदस्यता शुल्क पचास रुपए। इसके अलावा प्रति एकड़ ज़मीन के हिसाब से एक रुपया शुल्क था। इसका एक संविधान बना जिसके अनुसार यूनियन का कोई भी प्रबंधक सदस्य राजनैतिक दल से नहीं जुड़ेगा। इसका अर्थ था कि अजीत सिंह इसमें तभी शामिल हो सकते थे, अगर वह चुनाव न लड़ें। इस आधार पर अजीत सिंह का पत्ता कट चुका था। यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत और सचिव हरपाल सिंह बने।
अब महेंद्र सिंह टिकैत इस संगठन के लिए कोई ज्वलंत मुद्दा ढूँढ रहे थे। किसानों की समस्या तो कई थी, मगर शुरुआत कहाँ से हो?
सितंबर, 1986 में बरौत (बागपत जिला) में देश खाप के चौधरी सुखबीर सिंह ने एक पंचायत बुलायी थी।
सुखबिर सिंह ने कहा, “गाँव वालों! सरकार बिजली की दर बढ़ाती जा रही है। हम किसान आख़िर कैसे खेती करेंगे? हमारे पम्प कैसे चलेंगे? हमें कुछ करना होगा”
गाँव वालों ने एक साथ हुंकार भरी। सुखबिर सिंह के साथ ही हुक्का लेकर महेंद्र सिंह टिकैत बैठे थे। वे पारिवारिक रिश्तेदार भी थे। टिकैत ने देखा कि गाँव वालों में आक्रोश है, और पूरा देश खाप इस मुद्दे पर एकजुट है। उन्होंने अपने गाँव लौट कर अगले ही महीने बालियान खाप की पंचायत बुलायी।
महेंद्र सिंह टिकैत का पहला आंदोलन अब शुरू होने को था।
Author Praveen Jha narrates the story of farmer unions in India

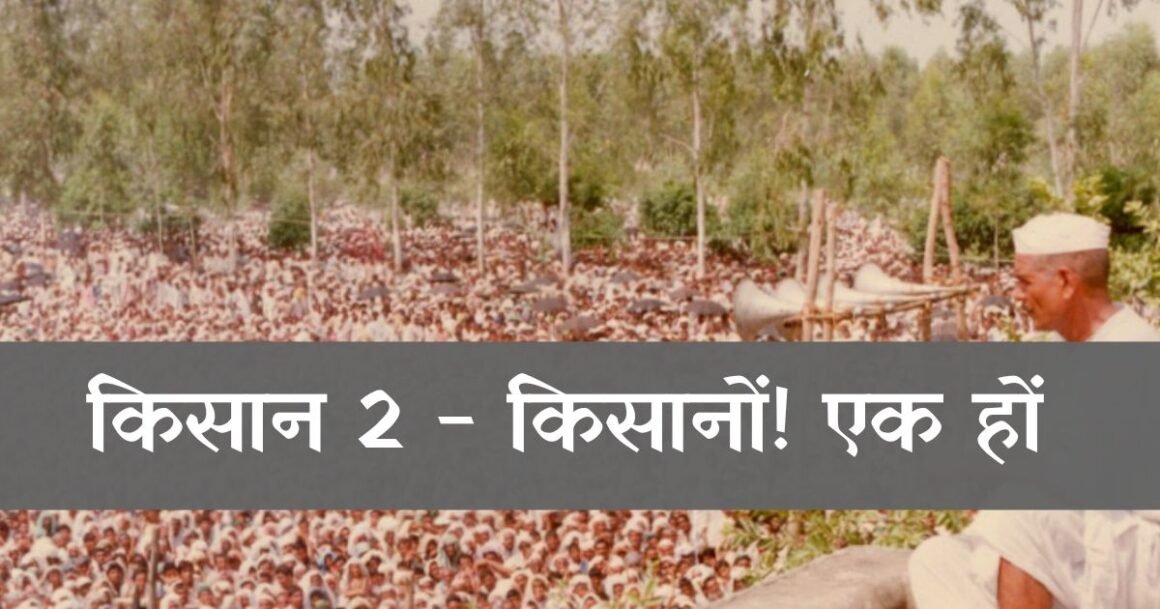
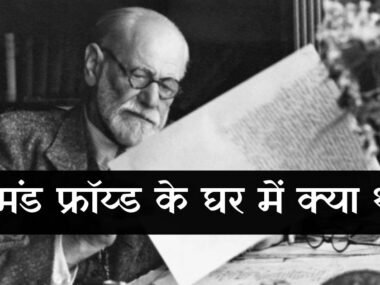
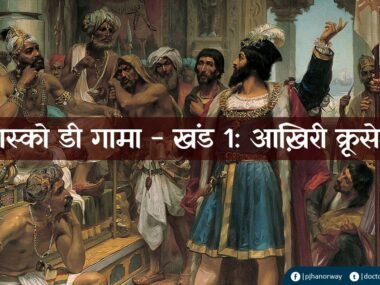
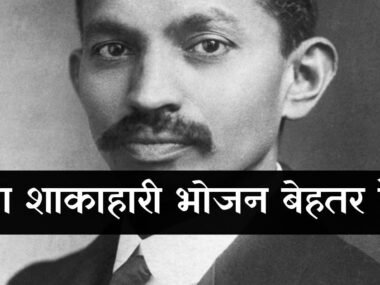
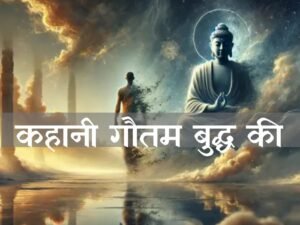
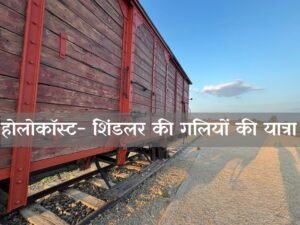
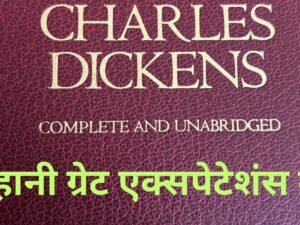
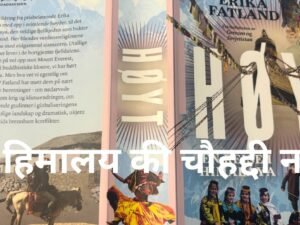
3 comments
आपका यह आलेख में स्वामी सहजानंद पर बहुत ही कम या न के बराबर टिप्पणी है। जबकि वे भारत में किसान आंदोलन के प्रतीक है। किसानों के मुद्दो पर वे गांधी एवम पटेल से भी भीड़ गए ।