1
‘हाँ! भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को पैसे दिए गए थे!’
6 जून, 1993 को राम जेठमलानी ने मुंबई के प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में जब यह आरोप लगाया, तो उनके साथ सफ़ेद शर्ट में हर्षद मेहता बैठे थे।
हर्षद मेहता ने एक ख़ाकी रंग के बड़े सूट्केस को दिखाते हुए कहा, ‘हम इस सूट्केस में 67 लाख रुपए लेकर प्रधानमंत्री आवास गए और उनके निजी सचिव राम खांडेकर को दिए। अगले दिन बाक़ी के 33 लाख भी पहुँचा दिए गए’
पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर इस तरह रिश्वत लेने का आरोप लगा था। कुछ ही महीनों पहले मुंबई ने बाबरी मस्जिद कांड के बाद बम के धमाके झेले थे। अब यह धमाका पूरे देश को हिला गया था। अगले ही महीने नरसिम्हा राव सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के मतों की वजह से नरसिम्हा राव की सरकार बच गयी। बाद में यह सिद्ध हुआ कि इन सांसदों को रिश्वत दी गयी थी।
जब प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगे थे, तो उन्होंने कहा था, ‘मैं इस अग्नि-परीक्षा से उसी तरह बाहर आऊँगा, जैसे माता सीता आयी थी’
इस मध्य उनके 7, रेस कोर्स आवास पर एक व्यक्ति उनसे मिलने आए। चेहरे पर पड़ी झुर्रियों और पके हुए बालों से वह साठ वर्ष से ऊपर की उम्र के लग रहे थे। सफ़ेद धोती-कुर्ता, पैरों में चप्पल और गांधी टोपी पहने वह व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री के कमरे में पहुँच गए। ज़ाहिर है, वह प्रधानमंत्री के निकट सम्पर्क के व्यक्ति होंगे, तभी इतनी अकड़ से दाखिल हो गए।
अंदर जाकर उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें की। फिर अचानक प्रधानमंत्री से कहा, ‘राव साहब! क्या आपने एक करोड़ रुपया लिया था?’
यह सवाल सुन कर प्रधानमंत्री सन्न रहे गए। ऐसे सवाल पत्रकारों ने भी पूछे थे, लेकिन यह आवाज़ जैसे उन्हें हिला कर रख गयी।
उन्होंने कहा, ‘क्या आप भी ऐसा सोचते हैं?’
यह सवाल करने वाले न कोई पत्रकार थे, न सांसद, न ही कोई पूँजीपति। वह एक किसान थे, जो अपनी तनी हुई पीठ के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे।
उनका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत!
वह इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, ‘यह हर्षद मेहता 5000 करोड़ का घपला कर के बैठा है, कई मंत्री घपला कर के बैठे हैं, और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही। लेकिन किसानों को 200 रुपए वसूली के लिए जेल भेजा जा रहा है?’
आज भी यह वाक्य पत्थर की लकीर की तरह है, जब विजय माल्या से मेहुल चोकसी तक देश से बाहर ऐश कर रहे हैं, और किसानों की कुर्की-ज़ब्ती हो रही है। लेकिन, आज किसान चुप नहीं बैठे। उन्हें ज़बान मिल गयी है, और यह ताक़त देने में मुज़फ़्फ़रनगर के सिसौली गाँव के उस किसान का हाथ है जिनकी कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ।
2
‘हम अपना तन, मन, धन अपने चौधरी को समर्पित करते हैं। चौधरी के लिए हम जान भी देने को तैयार हैं।’
– बालियान खाप पंचायत का समर्पण पत्र, 1941, सिसौली पंचायत
वर्ष था 1935। भारत का पहला संविधान ‘गवर्न्मेंट ओफ़ इंडिया ऐक्ट’ के तहत तैयार हुआ था। इसे कुछ लोग देश की आज़ादी की पहली सीढ़ी कह रहे थे।
पंडित नेहरू ने इस संविधान के संबंध में कहा, “यह मज़बूत ब्रेक वाली ऐसी मशीन है, जिसमें इंजन ही नहीं है”।
मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, “यह एक वाहियात संविधान है”।
और आम आदमी? भारत के किसान? उनके लिए यह क्या था? एक किसान के लिए इस स्वराज या आज़ादी का आख़िर क्या मतलब था? वे तो सामन्तवाद के पाँव तले दबे पड़े थे, और उन्हें मालूम नहीं था कि आज़ादी के बाद उनके जीवन में क्या बदल जाएगा।
कुछ वर्षों पहले अवध में एक किसान ने पंडित नेहरू से कहा था, “खाए के मीले, हमका सुराज नाही चाहीत”
एक हल चलाते, पसीना बहाते किसान के लिए राष्ट्र का अर्थ आखिर है क्या? उसे स्वराज में भी नाउम्मीदी क्यों नज़र आती है? यह सोचने की बात है।
उसके लिए राष्ट्र दुनिया के मानचित्र में बने कुछ निशान नहीं, उसकी वह मिट्टी है जो उसे और पूरे देश को रोटी देती है। खुशी देती है।
खुशी का माहौल उस दिन मुज़फ़्फ़रनगर के सिसौली गाँव में भी था। अश्विन का महीना था, अगले दिन दशहरा, और चौधरी के घर एक शिशु ने जन्म लिया। यह किसी साधारण चौधरी का घर नहीं था, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत बालियान खाप के चौधरी टिकैत का घर था। यह शिशु भविष्य का चौधरी था। उसे भी कहाँ पता था कि कुछ वर्षों बाद ही उस पर पूरे खाप की ज़िम्मेदारी आ जाएगी।
महज़ आठ वर्ष की अवस्था में महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना पिता खो दिया, और उन्हें बालियान खाप का चौधरी बना दिया गया। गाँव के स्कूल में मामूली शिक्षा ले रहे महेंद्र अब एक ऐसे किसान थे, जिन पर हज़ारों किसानों की ज़िम्मेदारी थी।
मगर ऐसा क्यों था? क्या वह कोई राजा-महाराजा थे? आख़िर इस पंचायत के चौधरी होने का क्या अर्थ था? खाप आख़िर है क्या?
आज हम अक्सर खाप पंचायत का नाम ‘हॉनर किलिंग’ जैसी घटनाओं की सुर्ख़ियों में पढ़ते हैं। शहर में बैठे यूँ लगता है कि जैसे यह कोई रूढ़िवादी आदम-युगीय प्रथा है। यह बात पूरी तरह ग़लत नहीं है। अगर बालियान खाप का उदाहरण लें तो यह पिछले 1400 वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल रही है।
सातवीं सदी में उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासकों में एक कहे जाने वाले हर्षवर्धन का राज था। उनकी राजधानी स्थानेश्वर (अब थानेसर, हरियाणा) थी, जो बाद में कान्यकुब्ज (कन्नौज) आ गयी। उनके राज में (या सम्भवतः उनसे पहले भी) उस इलाके के ग्रामीण पंचायतों को खाप पंचायत कहा जाता। बालियान भी ऐसी ही एक पंचायत थी, जिसके चौधरी को स्वयं राजा हर्षवर्धन ने ‘टिकैत’ पदवी दी थी।
खाप शब्द ‘ख’ यानी आकाश और ‘आप’ यानी जल से जन्मा। एक ऐसा संगठन जिसके आदर्श आकाश जैसे ऊँचे, और जल जैसे स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी हों। उस समय गाँवों में इस तरह के पंचायत बनाए गए, जो सामाजिक न्याय-व्यवस्था रखते। उनका काम अपने समाज के झगड़े या विवाद निपटाने से लेकर गाँव की समस्याओं को राजा तक पहुँचना भी था।
आज तो दुनिया बदल चुकी है। भारत में लोकतांत्रिक पंचायत मौजूद है। अब भला इस खाप का क्या औचित्य? क्या गाँवों में समानांतर सरकार चल रही है?
पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जाट समुदाय आज भी इन रिवायती पंचायतों को महत्व देते हैं। वे इसे एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह देखते हैं, जो उनके समाज को बांध कर रखती है। उनका यह भी मानना है कि वह लोकतांत्रिक राजनीति के दांव-पेंच से मुक्त है। आज जाटों के एक गोत्र या कुछ गोत्रों को मिला कर एक खाप बनता है। इसके अंतर्गत कई गाँव आ सकते हैं। गुर्जरों के भी अपने खाप हैं। भारत में 3500 से अधिक खाप पंचायत मौजूद हैं, हालाँकि उनमें से कई पंचायत अपना अस्तित्व खो रहे हैं।
खाप का संचालन उसके बुजुर्ग और ख़ानदानी चौधरी मिल कर करते हैं। गाँव की समस्याओं में उनका निर्णय ही सर्वमान्य होता है। इसका एक फ़ायदा यह है कि कई जमीनी या ग्रामीण मसले इसी पंचायत के माध्यम से जल्दी निपट जाते हैं, और कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। नुक़सान यह है कि यह लोकतांत्रिक नहीं है, और युवा-वर्ग की भूमिका संचालन में कम या नहीं के बराबर है। इसी तरह महिलाओं और पारंपरिक रूप से निचले पायदान की जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो बड़े खाप हैं – बालियान खाप और देश खाप। बालियान खाप काली नदी के दोनों तरफ़ लगभग बीस वर्ग मील में फैला है, और इस में 84 गाँव शामिल हैं। इन इलाक़ों के गाँव काफ़ी हद तक संपन्न और शक्तिशाली हैं। बालियान खाप के दो बड़े गाँव सिसौली और शोरम हैं। शोरम का चौपाल ही सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय है।
इस चौपाल के विषय में मुझे उम्मीद थी कि एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई चबूतरा होगा। लेकिन जब उसकी तस्वीर देखी तो लगा जैसे किसी मुग़ल शहंशाह की बैठक हो। क्या नक्काशीदार खम्भे, क्या ऊँची दीवारें और गुम्बज! यूँ लगता है जैसे सदियों से यहाँ पंचायत बैठती आ रही हो। कहा जाता है की तेरहवीं सदी में यहाँ एक महापंचायत का आयोजन हुआ था। बाद में जब मुग़ल बादशाह बाबर ने यहाँ की व्यवस्था देखी तो ईनाम में एक रुपया दिया और 125 रुपया वार्षिक राशि का वादा किया।

आज भी चुनावों में तमाम राजनीतिक दल उनके समर्थन की बाट जोहते हैं। मात्र महेंद्र सिंह टिकैत में हाथ में लगभग 2.75 करोड़ वोट माने जाते थे, जो जाट-बहुल 12 लोकसभा और 35 विधानसभा क्षेत्र में फैले थे। उनके एक इशारे पर सभी एक चुने हुए दल को वोट देते थे। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि वह इस लिहाज़ से ‘किंग-मेकर’ थे।
लेकिन, इस आठ वर्ष के चौधरी से ‘किंग मेकर’ बनने का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। यूँ भी उनकी पहुँच अपने गाँव और खाप पंचायत तक ही सीमित थी। उनसे पहले चौधरी नाम सुनते ही भारतीयों के मन में एक ही नाम कौंधता था।
चौधरी चरण सिंह!
(आगे की कहानी खंड 2 में। पढ़ने के लिए क्लिक करें)
Author Praveen Jha narrates a short history of farmer protests and Mahendra Singh Tikait.

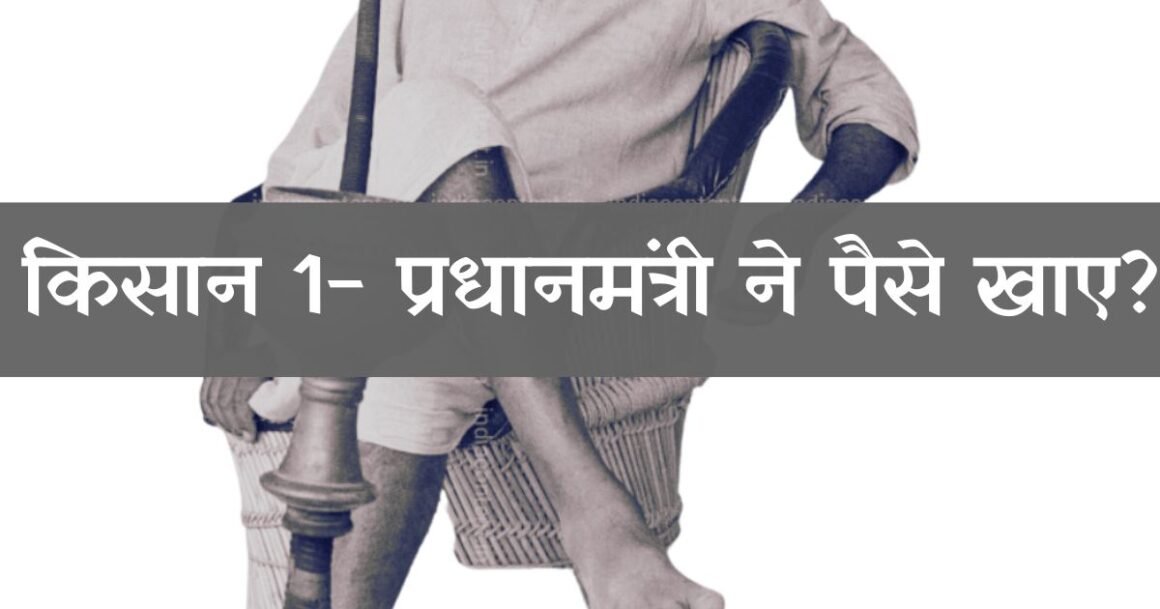
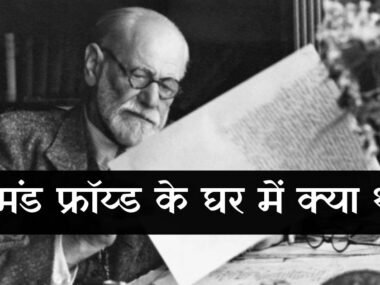
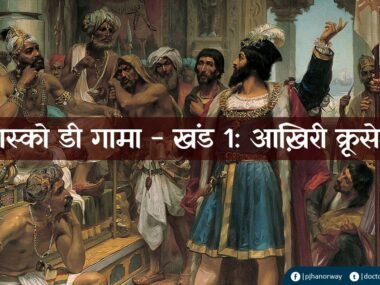
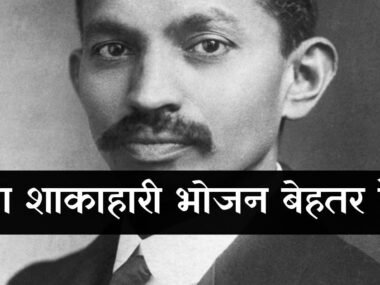
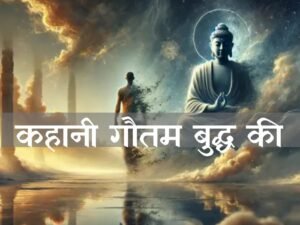
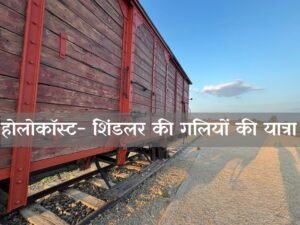
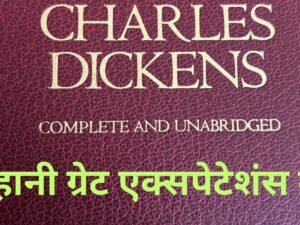
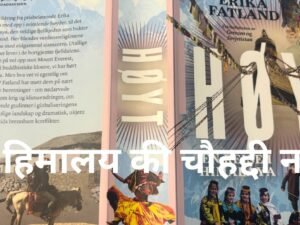
8 comments
Bahut hi sundar lekhani….rochak.
Sath hi gyaanvsrdhak