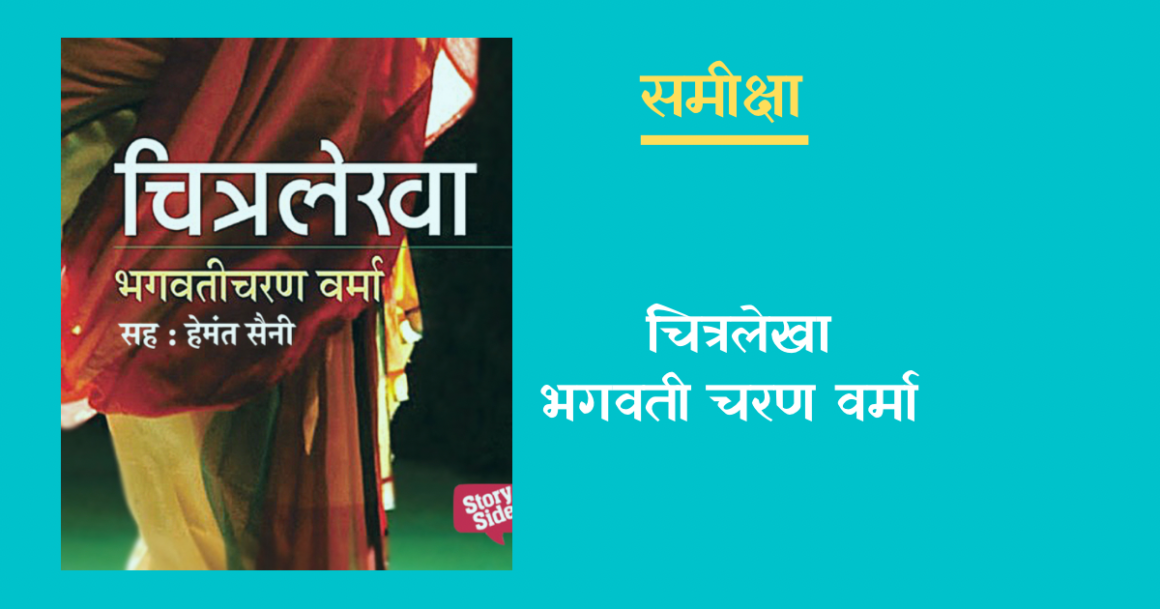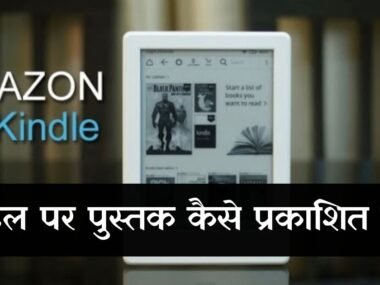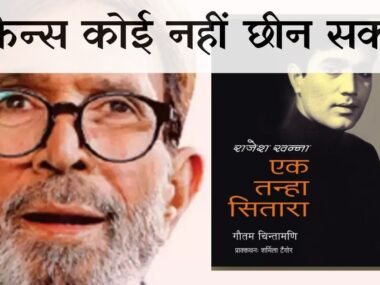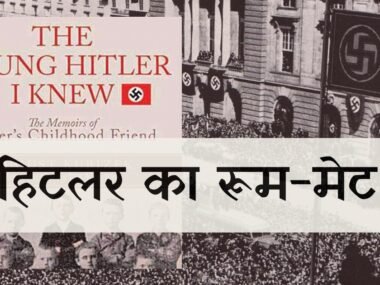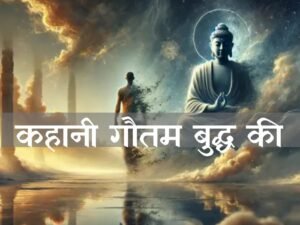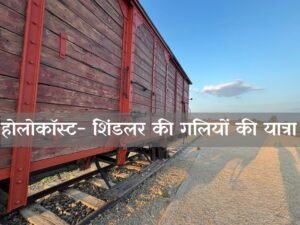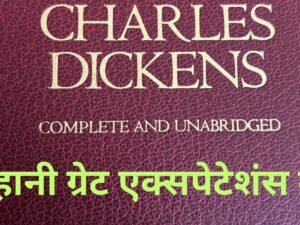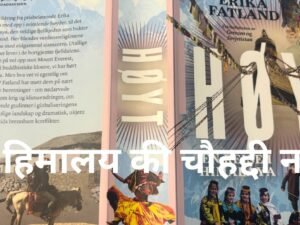आज के समय अगर एक क्लासिक उपन्यास का महत्व बढ़ गया है, तो वह है ‘चित्रलेखा’। इसका कारण है कि आज के समाज का रंग काला या सफ़ेद न होकर धूसर (ग्रे) है। संभवत: ऐसा समाज पहले भी रहा हो, लेकिन आज से मेरा तात्पर्य एक पूँजीवादी और व्यक्तिवादी दुनिया से है। अगर पूछा जाए कि क्या सही या क्या ग़लत है, तो यह उस व्यक्ति, उसकी परिस्थिति के अतिरिक्त उस पर भी निर्भर करती है, जो यह निर्णय ले रहा है। सत्य की परतें बढ़ गयी है।
मैं पश्चिम की दुनिया में रहता हूँ। किसी व्यक्ति को अगर शराब, काम-वासना और भोग-विलास में डूबा रह कर भी उसे एक अच्छा आदमी मानता हूँ, तो वह क्यों मानता हूँ? अगर कोई इन सभी वासनाओं से मुक्त है, तो सिर्फ़ इस आधार पर क्या उसे एक बेहतर व्यक्ति माना जा सकता है? भगवतीचरण वर्मा आज की कहानी नहीं कहते, लेकिन उस जमाने की कहानी कहते हैं जब पाटलिपुत्र आज के एम्सटर्डम की तरह था। सुंदर गणिकाओं (वैश्याओं) का ओहदा ऊँचा था, और उनकी चाहत में शहर के धनाढ्य सामंत रहा करते थे। जब मदिरा के प्याले वहाँ हर शाम टकराते थे। जब नौकायन करते हुए चाँदनी रात में नर्तकियों का नृत्य देखा जाता था। जब भोग-विलास की पराकाष्ठा थी, और स्त्री-पुरुषों के अनेक संबंध होते थे। जब पश्चिम का सूर्य उगा नहीं था, और पूरब ही आज की पाश्चात्य जीवन-शैली जीता था। यह कथा उस मौर्यकालीन पाटलिपुत्र की है।
यह ऑडियो पुस्तक लगभग छह घंटे की है। मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को इस पुस्तक को पढ़ने में कोफ़्त हो सकती है, लेकिन सुनने में यह ‘थ्रिलर’ के गति की लगेगी। अपने ऑडियो अनुभव में मैंने पाया है कि तत्सम-निष्ठ भाषा को पढ़ने से अधिक आसान सुनना है। शायद इसलिए कि भाव के साथ उच्चारण के कारण वे शब्द परिचित लगने लगते हैं। जब कथावाचक हेमंत सैनी कहते हैं- ‘श्वेतांक ने अध्ययन-भवन में प्रकाश देखा और अध्ययन-गृह में प्रवेश किया’ तो सुन कर असहज नहीं लगता। यही आभास होता है कि वह ‘स्टडी’ या ‘रीडिंग रूम’ में गए। बोल-चाल की भाषा या साहित्य में भी अब ‘अध्ययन गृह’ प्रयोग में नहीं है, लेकिन यह अटपटा नहीं लगता। मेरे ख्याल से इतिहास कथाओं में सुनना इसलिए भी सहज लगता है, क्योंकि सुनते हुए आँखें बंद कर हम आसानी से उस काल-खंड में चले जाते हैं। यूँ लगता है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पहुँच गए, जहाँ चाणक्य सामने बैठे हैं, और नर्तकियाँ नृत्य कर रही है। पढ़ते हुए तो आँखें खुली रहती है, इस कारण यह माहौल नहीं बन पाता।
यह कथा अगर आज की चलताऊ भाषा में कहूँ तो कुछ यूँ है कि एक गुरु अपने दो चेलों को यह पता करने भेजते हैं कि पाप क्या है। उस जमाने में ऐसे ही दार्शनिक होमवर्क होते होंगे। उनको छह महीने की इंटर्नशिप पर भेज दिया और कहा कि अपना प्रोजेक्ट बना कर लाएँ कि पाप आखिर है क्या। इसके लिए जो मॉडल है, वह बहुत ही सहज है। एक चेले को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया जो शराब और लड़कियों के नशे में धुत्त है। वहीं दूसरे चेले को ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो योगी है और तमाम वासनाओं से मुक्त है। कथा शुरू होने से पहले ही इनमें ‘पापी’ तो पहला व्यक्ति ही लगता है।
तभी इस कथा में इंट्री होती है चित्रलेखा की। ऐसी सुंदरी कि आप ऑडियो सुनते हुए ही उसकी पूरी कल्पना मन में बना लेते हैं। इस मामले में यह कथा बहुत ही आधुनिक लगती है कि एक उन्मुक्त मिज़ाज की स्त्री की चर्चा हो रही है। ऐसी स्त्री जो पाटलिपुत्र की ‘पोस्टर गर्ल’ है। जिसे पाने की इच्छा सबकी है, लेकिन उन्हें बस देख कर ही मन मसोसना पड़ता है। वह नर्तकी है, किंतु वेश्या नहीं। उसका शरीर सिर्फ़ उसी का भोग करता है, जिसे वह स्वयं चाहती है। वह जिसे चाहे, उसे लुभाती है, नचाती है, मोह-पाश में बाँध लेती है। जिसके स्पर्श-मात्र से सभी बंधन टूट जाते हैं, कर्तव्य बिखर जाते हैं। जब मैं यह उपन्यास सुन रहा था, चित्रलेखा से तो मैं भी आकर्षित हो गया। जिस तरह इस कथा के पात्रों में ईर्ष्या पनपती है, वह श्रोता के मन में भी पनपती चली जाती है। भगवतीचरण वर्मा ने चित्रलेखा का तीन पुरुषों से आकर्षण प्रस्तुत किया है, और तीनों ही तर्कसंगत हैं। यह अपने आप में ही चाणक्य जैसे नीतिशास्त्री के क्षेत्र में नीति की अलग परिभाषा रखते हैं। चाणक्य का इस उपन्यास में कैमियो भूमिका है, लेकिन उसके कारण उपन्यास रोचक बन गया है।
इस प्रेम-त्रिकोण में चित्रलेखा के एक हाथ में योगी का हाथ, तो दूसरे में भोगी का हाथ है। वह इन हाथों को कैसे बदलती है? क्या यह संभव है कि एक विश्वामित्र सरीखा तपस्वी भी अपनी साधना खो दे? एक भोगी प्रेम में पड़ कर वासनाओं से मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाए? यह उत्तर तो उपन्यास सुन कर मिलेगा। यह कमाल का मनोविज्ञान रचा गया है, जिस पर एक नए कलेवर के साथ फ़िल्म बन सकती है। हालाँकि दो फ़िल्में पहले ही बन चुकी है, लेकिन एक नए जमाने के लाइट-कैमरा-ऐक्शन के साथ भी संभव है। ऑडियो सुनते हुए फ़िल्म का आधा आनंद तो ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि उपन्यास संवाद-शैली में है और कथावाचक ने टोन बदल-बदल कर पाठ किया है। एक पुरुष वाचक होने के बावजूद उन्होंने चित्रलेखा का शोख़ रूमानी अंदाज़ खूब निभाया है।
जो कथा का क्लाइमैक्स है, वह अकीरो कुरोसावा की फ़िल्म ‘राशोमोन’ की याद दिलाती है, जहाँ एक ही घटना को भिन्न-भिन्न पात्र अलग नज़रिए से देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यह उस पर निर्भर है कि आप कहाँ खड़े हैं। आपकी अपनी सोच कैसी है, अनुभव कैसा है। योगी कुमारगिरी और सामंत बीजगुप्त में आखिर पापी कौन? पात्रों की नज़र में कौन, और श्रोता की नज़र में कौन? इस तरह की कथा एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो प्रबंधन से जुड़े हैं। यह व्यक्तियों और ‘कंफ्लिक्ट’ को समझने में कारगर सिद्ध होगा। उलझी मानसिकता को सुलझाने में। गिरहों को खोलने में। स्त्रियों के मनोविज्ञान को समझने में। सही निर्णय लेने में।
इस ऑडियो को मैंने दो खंडों में सुना, और मेरे विचार से इसे विराम देकर चार-पाँच खंडों में भी सुना जा सकता है। कथा इस तरह से विभाजित भी है कि सातत्य नहीं टूटता। इसे किसी धारावाहिक की तरह समयानुसार सुना जा सकता है। एक व्यस्त व्यक्ति के ऑडियो-लिस्ट में यह किताब काम की होगी। एक सुझाव यह रहेगा कि पात्रों के नाम मन में बिठा लें, अन्यथा श्वेतांक, कुमारगिरी, यशोधरा, बीजगुप्त, चित्रलेखा जैसे नामों में श्रोता उलझ सकते हैं। भगवतीचरण वर्मा की भाषा हालाँकि बहुत अधिक क्लिष्ट नहीं है, और सिर्फ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण ही शब्द भिन्न हैं। जो लोग नरेंद्र कोहली की किताब पढ़ते-सुनते आ रहे हैं, उन्हें भी यह किताब अपनी सूची में शामिल कर लेनी चाहिए। एक बेहतरीन रोमांटिक कथा रूप में भी इसे देखा जा सकता है, और एक भावनाओं से लदी पुस्तक रूप में भी। जैसा पहले कहा है, यह आज से ढाई हज़ार वर्ष पुरानी कथा है जो सौ वर्ष पूर्व लिखी गयी है, लेकिन इसकी महत्ता आज सबसे अधिक है। ऐसा क्यों है, यह तो सुन कर ही पता लगेगा।