यह लेख लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं। जिसने संगीत की शिक्षा ही नहीं ली, वह भला क्या राग पहचानेगा? मुझे ऐसे सूरमा मिले तो नहीं, लेकिन सुने हैं जिन्होंने पाँच सेकंड के आलाप में राग पहचान लिया। छुटपन में ‘सुरभि’ नामक टी.वी. सीरियल में इंदौर के किसी झरोखे से गाते हुए गायक की एक मिनट की क्लिप सुनाई गयी। हमने दस पोस्ट-कार्ड पर दस राग लिख कर गिरा दिए कि कहीं तुक्का लग जाए। वह राग अहीर भैरव था, और मैंने एक कार्ड में भैरव भी लिख कर गिराया था। भैरव में भी इतने भैरव, कहाँ खबर थी, और कितने तुक्के लगाता? लेकिन अब तो इतने वर्षों से सुन रहा हूँ, किताब भी लिखी। क्या अब बता पाऊँगा? शायद अब भी नहीं। लेकिन यह जरूर है कि दस मौके मिले तो कुछ आस-पास रह सकता हूँ। बस वह रहस्य कुछ खोल देता हूँ। बाकी, जो प्रशिक्षित संगीतकार हैं, उनके लिए यह अध्याय व्यर्थ है। शायद इसलिए पढ़ लें कि हम सुनने वालों का ज्ञान कहाँ तक है, कि आप जब प्रस्तुति दें तो लोगों को बताते भी चलें कि उस राग के गुण क्या हैं।
पुणे में उस्ताद सईदुद्दीन डागर यह बेहतरीन समझाते थे। उनके बताने का तरीका सुलभ है, और अगर रागों में श्रोता-रूप में क्रैश-कोर्स लेना हो तो उनका साक्षात्कार देखें। वह भैरव से शुरु कर केदार और राग देस तक भंगिमाएँ बनाते हुए, गाते हुए, रस के साथ समझाएँगे। वह ध्रुपद परंपरा से हैं, लेकिन वह संगीत के मूल तक समझाते हैं जो खयाल में भी लागू है। उनको सुन कर आप राग को सुनने ही नहीं, देखने भी लगेंगे। एक तस्वीर बन जाएगी, रागमाला पेंटिंग की तरह। मैं उस पेंटिन्ग का संग्रह भी अपने कंप्यूटर पर रखता हूँ, और जब कोई राग सुनता हूँ तो उन तस्वीरों को ग़ौर से देखता हूँ। राग से मन में चित्र बनना सहज है। जैसे भैरव सुनते हुए आप गंगा में खड़े हैं, और सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। दुर्गा सुनते हुए आप भगवती की आराधना कर रहे हैं और भगवती सिंह पर बैठी आ रही हैं। जब मल्हार सुन रहे हों तो बादलों की कल्पना करें, बिजली चमकने और बरखा होने की। इन रागों के स्वरों का संयोजन ही इन दृश्यों के हिसाब से है। लेकिन इस तरह शुरुआत न संगीत सीखने वाले करते हैं, न सुनने वाले। रस समझने के लिए संगीत में ही नहीं, जीवन में ही भावात्मक परिपक्वता की आवश्यकता है। एक किशोर से बेहतर वयस्क, एक चिकित्सक से बेहतर साहित्यकार, एक गद्यकार से बेहतर कवि, एक दफ्तर कर्मी की अपेक्षा शायद एक यायावर या चित्रकार या शोधार्थी या राजनीतिज्ञ या एक समाजशास्त्री बेहतर समझें। वीर रस, करुणा रस, शांत रस जैसे रस कोई शिक्षक क्या सिखाएगा? यह तो अनुभूति है।
एक श्रोता के लिए राग पहचानने के फेर में अधिक पड़ना आवश्यक नहीं। गायक-वादक यूँ भी राग और ताल पहले बता देते हैं। सी.डी. या यू-ट्यूब पर भी यह लिखा ही होता है, तो यह कोई छुपा रहस्य नहीं कि इसे जानना ही हो। लेकिन रागों की समझ हो तो आनंद बढ़ने लगता है, और मष्तिष्क भी ‘कंडीशन’ होता जाता है। शुरुआत में सबसे सुलभ है बंदिशों से जुड़ना। यह सुगम संगीत और फ़िल्मी संगीत का युग है, और हमें गीत याद रहते हैं। जो बंदिश फ़िल्म में आ गए, उनसे जुड़ना अधिक आसान है। जैसे- ‘मन तड़पत हरि दर्शन को आज’ राग मालकौंस की हू-ब-हू बंदिश है। इस धुन से मिलता-जुलता राग सुनते ही दिमाग में मालकौंस कौंधेगा। ‘निगाहें मिलाने को जी चाहता है’ से कुछ मिलता सुनते ही राग यमन का ख्याल आए। ‘बोले रे पपीहरा’ से मल्हार याद आए। और कई बंदिशें राग सुनते-सुनते भी मन में बैठ जाती हैं। ‘जा जा रे अपने मंदिरवा’ सुना तो भीमपलासी; ‘कवन बटरिया’ सुना तो अल्हैया बिलावल। बंदिश के बोल भी बहुत कुछ कहते हैं। ‘जागो, मोहन प्यारे’ फ़िल्मी बंदिश है, जिसमें यह स्पष्ट ही है कि सुबह का राग है- भैरव। सावन या बरखा की बात हो तो मेघ, मल्हार और देसकर जैसे राग मन में आते हैं। शंकर/शिव पर बंदिश हो तो राग शंकरा, मालकौंस या अडाना जैसे राग। भवानी पर बंदिश हो तो दुर्गा, भैरवि या अडाना। बसंत पर बंदिश हो तो बसंत, बहार, या मालकौंस। बंदिश धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि यह नियम नहीं कि शिव पर बनी बंदिश राग दुर्गा न हो। लेकिन, यह कुछ मामूली संकेत दे रहा हूँ।
व्यवस्थित तरीका तो यह है कि एक-एक कर रागों को लगातार सुनना शुरू करें। जैसे एक महीने तक एक नियत समय पर बस राग यमन के गायन और वादन सुनते गए। एक मन में पैटर्न बनता गया कि एक हफ्ते बाद ही यह कह सकें कि यह राग यमन के चलन पर ही है। या यह बंदिश बार-बार यमन में आ रही है। सितार में भी वही बंदिश बजायी जा रही है। इस तरह कुछ जाने-माने रागों को नियमित सुन सकते हैं, जैसे- भैरव/भैरवि, भीमपलासी, भूप, मालकौंस, दरबारी, यमन, बागेश्री, मल्हार, बिहाग, और हंसध्वनि।
यह प्रश्न मन में उठ सकता है कि बंदिश तो गायकी का बहुत ही छोटा अंग है। बड़ा और मुख्य अंग तो आलाप है, जिसमें गीत ही नहीं। वहाँ तो बस स्वर हैं, और स्वर के विस्तार हैं। यह भी नहीं कि वे सरगम बोलें और हम कम्प्यूटर/मोबाइल पर ढूँढ मिला लें। वहाँ तो जैसे आss (आकार आलाप) से ही स्वर पहचानना है। अब अगर वह ‘सा’ बोले ही नहीं, तो हम कैसे समझें कि वह ‘सा’ कह रहे हैं? यह वाकई टेढ़ी खीर है। यह कानों के प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं, और इसमें वर्षों लग सकते हैं। अब तकनीकी युग है, तमाम ऐप्प आ गए हैं कि हम एक-एक स्वर को सुन कर समझ सकते हैं। या कीबोर्ड पर उंगलियाँ चला कर समझ सकते हैं कि अगर ‘सा’ ऐसा है तो ‘म’ कैसा होगा। लेकिन इसके लिए श्रोता को आधा संगीतकार ही बन जाना होगा। गाकर सुनना होगा, या सुन कर गाना होगा।
आलाप में यह ध्यान दिया जाए कि नीचे के स्वर (सा रे ग) अधिक लग रहे हैं, या ऊपर के स्वर (प ध नी)। यही पूर्वांग और उत्तरांग कहलाता है। सभी स्वर लग रहे हैं या कुछ स्वर नहीं भी लग रहे? जैसे भूप में मध्यम (म) और निषाद (नि) नहीं मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं, तो वह भूप नहीं। कौन सा स्वर अधिक लग रहा है? यानी वादी स्वर कौन सा है? यह सब बहुत ही कठिन ज्ञान है। इसलिए भी कि हर गायक का स्केल अलग है। किशोरी अमोनकर का ‘सा’ और भीमसेन जोशी का ‘सा’ बिल्कुल ही अलग स्केल पर हैं, तो सरगम ही अलग सुनाई देगी। इसके लिए कानों (मष्तिष्क) के अंदर भी कई खाने बनाने होंगे, जिनमें हम स्विच कर सकें। और उसके बाद की सबसे ऊँची सीढ़ी है, स्वर गाने का अंदाज और उनको सजाने का चलन या पकड़ समझने। यानी उस ख़ास राग में कौन सा ‘फ़्रेज’ अधिक गाया जाता है। किस राग में धैवत आंदोलित कर या हिला कर गाते हैं? किस राग में हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर मींड से आते हैं? यह सब मेरे विचार से एक लंबे समय के बाद ही शुरु करें। बिना तैरना सीखे गहरे पानी में उतर गए तो डूबने का भय है।
(लेखक प्रवीण झा की पुस्तक ‘वाह उस्ताद’ इस लिंक पर उपलब्ध है- https://www.amazon.in/Wah-Ustad-Praveen-Kumar-Jha/dp/9389373271 )


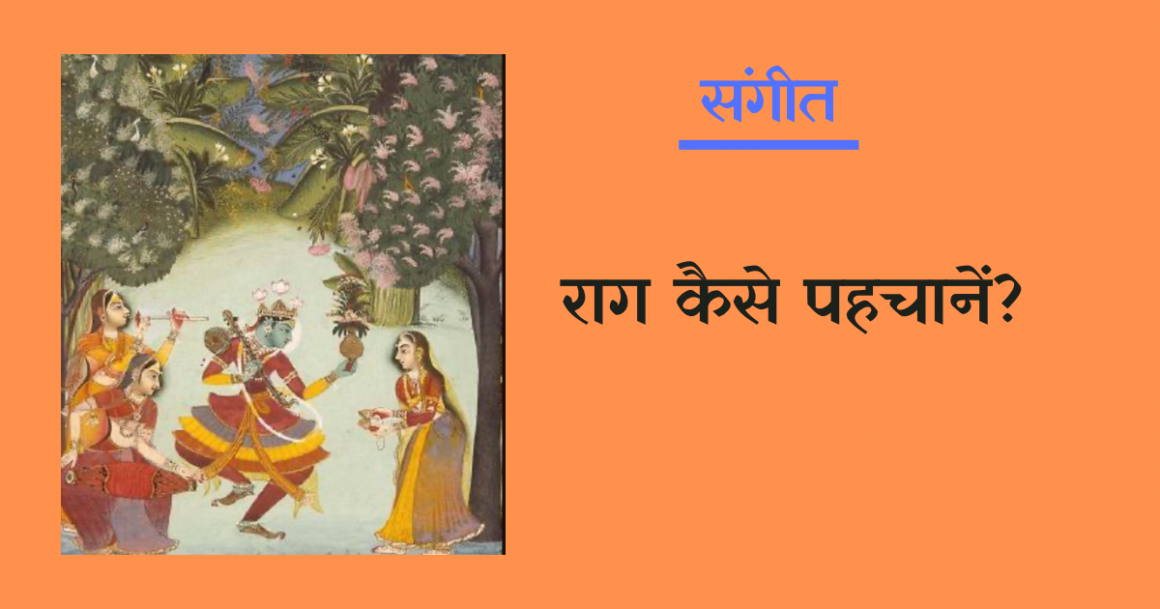


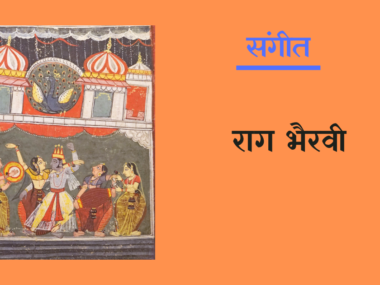
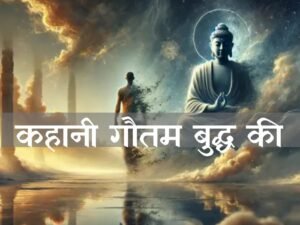
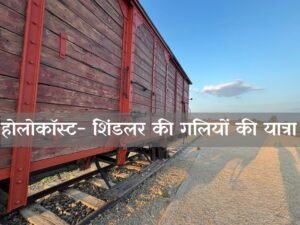
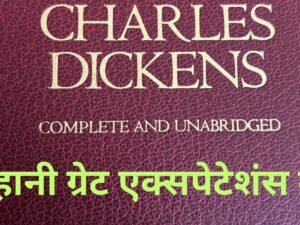
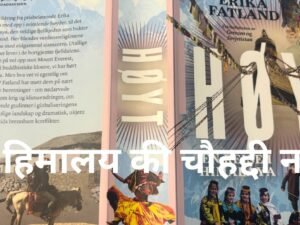
2 comments
वाह! आपने बहुत ही संक्षेप में इतनी सारी जानकारी दी है और मुझे लगता है एक नए उत्सुक श्रोता के लिए इससे सरल कुछ और नहीं हो सकता.
ये लेख पढ़कर किसी की भी शास्त्रीय संगीत और रागों में रुचि स्वतः जाग जाएगी। बहुत सुंदर लेख है। संगीत प्रेमियों को तो पढ़ना ही चाहिये और जो संगीत के रसिक ना हों तो उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए।