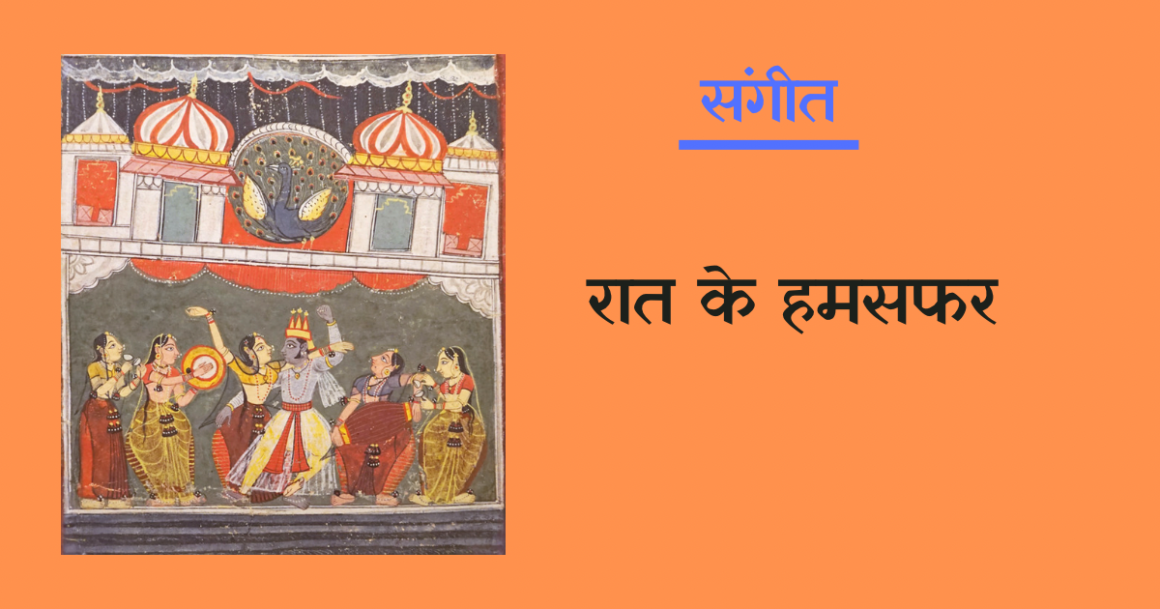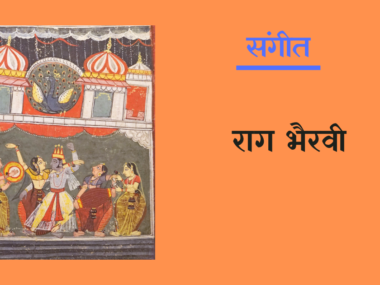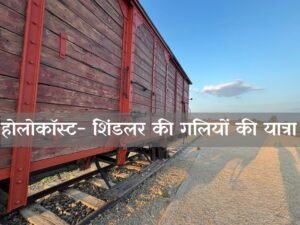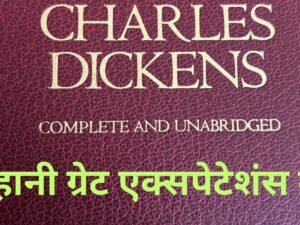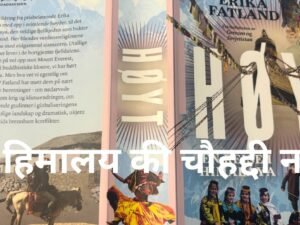6-9 बजे (साँझ के राग)
“छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाय के”
– अमीर ख़ुसरो
राग यमन अमीर खुसरो का बनाया राग है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ‘यमुना’ से यमन बना, कुछ कहते हैं फ़ारसी के ‘ईमान’ से। यह भी मुमकिन है कि यह वैदिक काल से हो और अमीर ख़ुसरो ने लोकप्रिय बनाया हो। अक्सर हर गायक राग यमन कल्यान से सीखना शुरू करता है। वजह है कि बाकी इसमें सातों स्वर हैं। इसे अगर पियानो पर बजाने बैठे तो बस सफेद खानों को दबा कर बजाया जा सकता है, उंगली ऊपर-नीचे नहीं करनी। लेकिन यह जितना सुलभ दिखता है उतना है नहीं।
राग के स्वरों पर ख़ास तकनीकी बात तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इसका केंद्र मध्यम (म) है। कहा गया है कि एक पर्दानशीं की तरह मध्यम झांक कर वापस पर्दे में चला जाता है। यह बारीकी समझनी मुश्किल है, लेकिन शायद सुनते-सुनते वह मध्यम पकड़ में आ जाए। वादी स्वर गंधार (ग) है, लेकिन मध्यम की छटा निराली है। सुनते वक्त जो मुझे इस राग में सौंदर्य नजर आता है कि यह निषाद (नी) से ही उठाया जाता है। जैसे-
नी रे सा- नी रे ग म प ध नी सा’
सा’ नी ध प म ग रे सा
महफ़िलों की शुरुआत इसी राग से अक्सर होती है और यह रागों का राजा है। शांत रस का राग है तो जाहिर है यह मन के शांत कर देता है। यही वजह है कि फ़िल्मी संगीतकारों का चहेता राग भी यमन ही है। इसमें भक्ति भी हो सकती है और प्रेम भी। ‘चितचोर’ फ़िल्म में येशुदास का गाया ‘जब दीप जले आना’ भला किसे नहीं पसंद? इसका सबसे सुंदर फ़िल्मी उदाहरण है- ‘निगाहें मिलाने को जी चाहता है’।
इस राग की सबसे अजीज पेशकशों में एक है जब पं. रविशंकर सितार पर हैं, और उनकी प्रथम पत्नी अन्नपूर्णा देवी जी सुरबहार पर। यह जुगलबंदी अप्रतिम है और कभी इत्मीनान से शाम को बैठ जरूर सुनी जानी चाहिए। एक मशहूर बंदिश जिसे कई गायकों ने गाया है-
“सखी ए री आली पिया बिन/कलन परत मोहे/घड़ी पल छिन दिन
जबसे पिया सौतन घर बन कीनो/रतियन कटत मोरे तारे गिन गिन”
इस राग के दो भाई-बहन भी हैं। इसी राग में अगर ऋषभ (रे) कोमल हो तो यह पुरिया कल्यान बन जाता है, और अगर साथ-साथ धैवत (ध) भी कोमल हो तो पुरिया धनश्री। अगर राग यमन राजा है, तो पुरिया धनश्री रागों की रानी है। राग मारू बिहाग भी यमन के काफी नजदीक है। मालवा के राजा बाज बहादुर की खूबसूरत प्रेमिका रूपमती ने राग शुद्ध कल्याण रचा था। अब इसके न जाने कितने रूप हैं। कुमार प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है कि एक बार उस्ताद फैयाज ख़ान और विष्णु भातखंडे कश्मीर गए। वहाँ फैयाज ख़ान साहब ने महारानी को दस दिन में 18 प्रकार के राग कल्याण सुनाए! यहाँ से जब वह भातखंडे जी के साथ लौटने लगे तो उन्होंने अपना प्रिय शिष्य श्रीकृष्ण रतण्जनकर ही उनको सौंप दिया।
राग यमन का परिचय यहाँ देखें
सभी गायक यमन से ही नहीं शुरु करते। कुछ भूपाली से भी करते हैं, कुछ ने तो दरबारी से भी शुरुआत की। लता मंगेशकर का प्रियतम राग यमन है, लेकिन उन्होंने राग यमन से अपनी शास्त्रीय संगीत शिक्षा नहीं शुरु की। यतींद्र मिश्र ‘लता सुर गाथा’ में जिक्र करते हैं कि जब लता मंगेशकर ने भिंडीबाजार के उस्ताद अमान अली ख़ान से गंडा बँधवाया, तो सबसे पहले राग हंसध्वनि सीखा। उनकी सिखाई दो बंदिशों में एक थी ‘पतिदेवन महादेवन’ और दूसरी थी –
“लागी लगन पति सखी संग/परम सुख अति आनंदन
आए नए बदन कामन सबन बन/अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे/दृगन नयनन अंजन फबनते/‘अमर’ हो नित पति काजे सदन”
उस्ताद अमान अली ख़ान से यह उस्ताद अमीर ख़ान ने भी सीखा होगा। इसके मेरे पास दो तर्क हैं। एक तो उनका गाया एक हंसध्वनि में तराना इससे मिलता-जुलता है। दूसरा यह कि उनके मित्र ऋत्विक घटक ने पं. कन्नन की आवाज में यही गीत फ़िल्म ‘मेघे ढके तारा’ में गवाया। फ़िल्म में इस बंदिश को यूँ ही झूमते हुए गाते नायक चलते जा रहे हैं, जैसे कितना सहज राग हो। मेरे मन में यह भी कौतूहल हुआ कि भिंडीबाजार के उस्ताद के पास यह राग कहाँ से आया? जितने संदर्भ मिले, उस हिसाब से वह कार्नाटिक संगीत से हंसध्वनि को लेकर आए। और यह उत्तर-दक्षिण का मिलन पं. अजय चक्रवर्ती की गायी बंदिश ‘लगन मोरी लागी’ में स्पष्ट हो जाता है। उस प्रस्तुति में पंडित जी वातापी गणपति का मंत्र कार्नाटिक शैली में ही गाते हैं। उनकी बेटी-दामाद कौशिकी चक्रवर्ती और पार्थसारथी देसीकन ने भी ‘लागी लगन पति सखी संग’ बेहतरीन गाया है।
हंसध्वनि का परिचय यहाँ देखें
कौशिकी चक्रवर्ती जी एक और राग बेहतरीन गाती हैं- मधुवन्ती। इसमें उनकी गायी बंदिश है- ‘काहे मान करो’। यह बंदिश पं. भीमसेन जोशी जी ने गीत की तरह लेकिन लंबी तान लेकर गाया है। इसी बंदिश को अपने सूफ़ियाने आवाज में श्वेता झवेरी जी ने बड़ा खयाल गाया है। मधुवन्ती आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। दरभंगा घराने की बेटी प्रियंका मलिक पांडे तो द्रुत लय में गमक के साथ जब मधुवन्ती गाती हैं, तो हॉल गूँज उठता है। मधुवन्ती में ही मशहूर फ़िल्मी बंदिश है- ‘अजहु न आए बालमा, सावन बीता जाए’।
यह राग मुल्तानी से मिलता-जुलता बड़ा रूमानी राग है। मुल्तानी के कोमल ऋषभ और कोमल धैवत की जगह शुद्ध ऋषभ और शुद्ध धैवत प्रयोग हो तो मधुवन्ती बन जाता है। तो इसमें भी वही स्वर, वही चलन – म ग म ग रे सा।
मधुवंती में कुछ और प्रस्तुतियों का जिक्र करुँगा, जो सुननी चाहिए। पं. रविशंकर और पं. हरिप्रसाद चौरसिया की बजायी मधुवन्ती। अश्विनी देशपांडे जी की बंदिश- ‘शिव आद’, और ग्वालियर से मीता पंडित की बंदिश ‘कृपा करो नाथ’। आपने यह गौर किया कि यह महिला गायकों में लोकप्रिय राग है? गिरिजा देवी जी और प्रभा अत्रे जी की मधुवंती भी लिस्ट में जोड़ लें।
मधुवंती का राग परिचय यहाँ सुने
किशोरी अमोनकर जी की मधुवन्ती मैंने नहीं सुनी। उनकी पहचान भूपाली की बंदिश ‘सहेला रे’ से बन गयी। जैसे उस्ताद अमीर ख़ान के लिए राग मारवा, वैसे ही किशोरी अमोनकर के लिए भूप/भूपाली। इस राग में वह पूरी तरह डूब जाती है। भूपाली पाँच ही स्वर का राग है, और अक्सर संगीत की स्कूल कक्षाओं में एक बंदिश सीखायी जाती है- ‘लाज बचाओ कृष्ण मुरारी’। तो भूपाली से भक्ति जुड़ी हुई है। इसी धुन की मूल सदारंग की बंदिश ‘इतना जोबन पर मान न करिए’ को गौहर जान ने ठुमरी में गाया। यह ठुमरी बस इसलिए सुननी चाहिए कि कैसे शब्द बदलने और गाने के अंदाज से से भूपाली का रस बदल गया। इस राग को रटाने के लिए संगीत शिक्षक कहते हैं कि यह राग कंगाल है। इसके पास ‘मनी’ नहीं है। यानी इसमें मध्यम (म) और निषाद (नि) वर्जित है।
भूप का राग परिचय यहाँ सुनें
मुझसे अगर साँझ का प्रियतम राग पूछा जाए तो मैं कहूँगा- राग तिलक कामोद। अधिकतर सर्दियों की शाम जब मैं ऑफ़िस से लौट कर अलाव में लकड़ियाँ लगा कर कुर्सी पर बैठता हूँ तो तिलक कामोद ही सुनता हूँ। इसमें एक सम्मोहन है। तिलक कामोद राग देस का ही चचेरा भाई है, लेकिन इसके कोमल निषाद (नि) की छटा अलग है।
कोमल निषाद से एक कुमार प्रसाद मुखर्जी का लिखा वाक्या याद आया।
रामपुर के नवाब हामिद अली ख़ान संगीत के ख़ास शौकीन थे और गायक भी, लेकिन अफ़ीम का खूब सेवन करते। एक बार उस्ताद फैयाज़ ख़ान उनके सामने गा रहे थे।
नवाब ने बीच में रोक कर पूछा, “यह कौन सा राग गा रहे हैं आप?”
उस्ताद ने कहा, “हजूर! तिलक कामोद”
“क्या बकवास कर रहे हो? तिलक कामोद में निषाद नहीं होता!”
“जी हुकुम! फिर से गाता हूँ।” फैयाज़ ख़ान ने कहा और बिना निषाद (नि) के गाया।
बाद में फैयाज़ ख़ान के शागिर्दों ने टोका?, “उस्ताद! बिना निषाद के तो तिलक कामोद नंगा है!”
उस्ताद ने हँस कर कहा, “अब सरकार का हुकुम था तो कौन जिरह करे?”
तिलक कामोद में दो बंदिशों का जिक्र करूँगा। एक रामाश्रय झा ‘रामरंग’ की बंदिश है, जो द्रौपदी चीर-हरण पर आधारित है-
“मेरो पत राखो मुरारी/भीष्म-द्रोण बैठे पावर भए/सूर सभा सब क्रूर भए बैठे/रामरंग बैठे पारथ पाथर भए
बेगि बेगि आए हरि/आरत सुनि बनि धाए पग उघारे/दीनानाथ अनाथ की पथ राखी/रामरंग जन-हित बसन रूप धरे।”
दूसरी बंदिश नवाब वाजिद अली शाह (अख़्तरपिया) की लिखी है जिसको एक होली में उन्होंने नाचते हुए मटियाबुर्ज (कलकत्ता) में गाया था। आज भी यह ठुमरी बहुत लोकप्रिय है, और शुभा मुद्गल जी ने भी गाया है-
“नीर भरन कैसे जाऊँ सखी रे/डगर चलत मोसे करत रार सब
ऐसो चंचल चपल हट नटखट/मानत न काहू की बात/बिनती करत मैं तो हार गयी अब”
तिलक कामोद का परिचय यहाँ देखें
इस प्रहर के एक राग का जिक्र किए बिना चर्चा खत्म नहीं हो सकती- जयजयवंती। लता जी का गाया – ‘मनमोहना! बड़े झूठे’ ध्यान में रख कर इस राग के चलन का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे आगरा और ग्वालियर वाले कुछ अलग तरीके से गाते हैं (गारा अंग या बागेश्री अंग) और बाकी घराने में अलग तरीके (देस अंग) से। लेकिन वह तकनीकी बातें हैं। इसकी एक प्यारी बंदिश है विनायक पटवर्धन जी की-
“सुंदर श्याम देखन की आशा/नैनन बान परी; चार जाम मोहि तड़पत बीते/रह गई एक धरी
भूषण बसन भवन नहि भावे/बिरह बियोग भरी; ‘दयासखी’ अब बेगि मेलि क्यो न/हौ अकुलत खरी।”
राग जयजयवंती का परिचय यहाँ देखें
9-12 बजे (रात की महक)
राग शंकरा तो बना ही शिव के नाम पर है, इसलिए यह रागों का भगवान् है। और इसका रस भी स्पष्ट ही है। रूद्र या वीर रस। पं. सियाराम तिवारी (दरभंगा घराना) के गर्जन में ‘हर हर महादेव’ सुनना इस राग की परिणति है। इस राग की कई बंदिशों में डमरू बजाते शिव, या महादेव का स्वर मिलेगा ही। तो राग पहचानने के लिए एक ट्रिक यह भी है कि शंकर डमरू बजा रहे हैं, यानी शंकरा!
गोवा की प्रचला अमोनकर जी की एक प्रस्तुति रेडियो पर सुन रहा था तो गौर किया कि इसमें जब आरोह लेते हैं तो ऊँचे स्वरों पर अधिक रहते हैं। ख़ास कर ‘निषाद’ पर। तो यह भी उत्तरांग प्रधान राग है। बल्कि आरोह में पूर्वांग (सा रे ग म) के दो स्वर ऋषभ (रे) और मध्यम (म) वर्जित ही हैं। नि नि नि सा, नि नि सा की अावृति सुनने को मिलती है।
लेकिन यह मैंने स्पष्ट महसूस किया है कि जब सियाराम तिवारी (और अन्य ध्रुपद गायकों) को सुनता हूँ तो शंकरा का अलग मूड, अलग रस है। बल्कि खयाल गायकी का शंकरा तो वीर रस का नजर ही नहीं आता। वहाँ करुणा और भक्ति का तत्व अधिक है। ध्रुपद में ही डमरू बजाते शिव की छवि नजर आती है। यह मेरा आकलन है, ग़लत भी हो सकता है।
इस राग में विलायत ख़ान की बजायी एक प्रस्तुति यू-ट्यूब पर है, जिसमें शायद तबले पर किशन महाराज हैं। विलायत ख़ान अपने अंदाज में न सिर्फ बजा रहे हैं, बल्कि बतियाते हुए गा भी रहे हैं।
हम डाक्टरी में कहते हैं कि अगर सर्ज़री की किताब से अपेन्डिक्स का पन्ना फाड़ दें तो आधे सर्ज़न भूखे मर जाएँ। मैं रागों में बागेश्री के लिए यही कहता हूँ। यह तो साक्षात् सरस्वती ही है, जो नाम से ही स्पष्ट है। कहा जाता है कि तानसेन ने सबसे पहले यही राग गाया था। ऐसा शायद ही कोई सम्मेलन हो, जिसमें बागेश्री नहीं गाया-बजाया जाता हो। बल्कि अक्सर एक ही शाम कई बागेश्री सुनने को भी मिल जाते हैं। बागेश्री और दरबारी ऐसे राग हैं जिसमें विस्तार (इम्प्रोवाइज़ेशन) का जम कर स्कोप है। इसमें कलाकार खुल कर अपने रंग दिखाते हैं। गायकी में भी, और वादन में भी।
लता जी ने फ़िल्म मधुमती में गाया है- ‘आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार’। यह गीत इस राग के मूड और चलन, दोनों को समझने के लिए उपयुक्त है। यानी इसमें शृंगार भी है, और एक वेदना भी। इसलिए यह राग भक्ति-संगीत (इबादत) में भी जमता है। यह दरअसल सुकून देने वाला राग है। दरबारी कन्हड़ा और बागेश्री उन रातों को जरूर सुनना चाहिए जब तनाव और चिन्ता से सर फटा जा रहा हो। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ओंकारनाथ ठाकुर और पं. जसराज ने इस राग से एक उत्तेजित शेर को शांत कर दिया था।
एक कौशिकी चक्रवती सरस्वती वंदना के लिए बागेश्री में बंदिश गाती है, जो मुझे प्रिय है-
“याद करुँ ध्यान धरुँ माता सरस्वती,
तू ही हमारी गति माता सरस्वती।”
मेरी नजर में संगीत सीखना बड़ा धैर्यपूर्ण और शुरुआती समय में नीरस काम है। मुझे याद है स्कूल में हारमोनिया लेकर हमारे संगीत शिक्षक आँख बंद कर शुरू होते, ‘भगवान…ओ दुनिया के रखवाले…सुन दर्द भरे मेरे नाले’ और मैं भाग लेता। ये संगीत शिक्षकों का शायद प्रिय गाना है, और स्वरमान (पिच) ऐसा है कि अक्सर बेसुरा निकलता है। सुन दर्द भरे…मेरे नाले…
यह गाना राग दरबारी पर आधारित है। तानसेन को अकबर को खुश करना था। उस जमाने की पहली ‘पाइरेसी’ हुई। एक पुराना राग ‘कन्हड़ा’ उठाया गया, कोमल गन्धार (ग) को आंदोलित किया गया। आंदोलित करना मतलब स्वर को ज्यादा समय खींचना, लहराना। राग में ऐसी शक्ति आ गई कि अकबर को भगवान के पैदान पर बिठा दिया। इस राग में गांधार और धैवत का आंदोलन गर कायदे से न हो, यह राग बिखर कर कुछ और बन जाता है। जैसे, यह जौनपुरी बन जाएगा। इसे पकड़ कर रखना कठिन है। दरबारी का यह कोमल गांधार (ग) इस कदर लोकप्रिय है कि सुनने वाले उछल कर कहते हैं कि यह तो दरबारी का गांधार है, वाह!
यह राग भगवान के लिए उपयुक्त है और भजन इस राग में बनते हैं। लगभग एक साल मैं ISKCON में कृष्ण-भक्ति में फँस गया था। फँस गया था इसलिए कहूँगा क्यूँकि नियम-कानून कई थे और गीता भी सड़कों पर बेचनी होती। लेकिन सुबह-सुबह राग दरबारी में ‘जय राधा माधव…कुंजबिहारी…’; ये हिस्सा गजब था। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन तक ने यह भजन ठीक-ठाक गाया है। आशा जी का इसी राग में ‘मोरा मन दर्पण कहलाए’ तो लोकप्रिय है ही।
उस्ताद हाफिज अली ख़ान (अमजद अली ख़ान के पिता) को जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पद्म विभूषण दे रहे थे तो पूछा, “ख़ान साहब! आपको कोई तकलीफ हों तो बताएँ।”
उन्होंने कहा, “हजूर! हो सके तो दरबारी को बचा लें।”
राजेंद्र प्रसाद ने कहा, “मैं समझा नहीं।”
उन्होंने कहा, “आजकल लोग राग दरबारी के साथ बहुत छेड़खानी कर रहे हैं। आप तो आलाकमान हैं। आप कुछ संविधान लाएँ कि दरबारी तरीके से ही गायी-बजायी जाए।”
इस राग में प्रस्तुतियाँ तो कई हैं, और एक से एक हैं; कुछ हट कर रोशन आरा बेगम का गाया ‘परदेसवा न जाओ सजनवा’ का जिक्र करता हूँ। इसको सुन कर मैं अब्दुल करीम ख़ान के इकहरा तान को महसूस करने की कोशिश करता हूँ। आखिर वह उनकी भतीजी ही तो थी।
फ़िल्मी भजनों में अगर दरबारी प्रमुख है, तो केदार भी पीछे नहीं है। भक्ति के लिए यह मेरे प्रिय रागों में है। मशहूर भजन ‘दर्शन दो घनश्याम नाथ’ और ‘हमको मन की शक्ति देना’ इसी राग पर आधारित हैं। इसी गत पर निखिल बनर्जी की सितार पर प्रस्तुति गजब की है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को देखते हुए केदार का रंग निखर उठता है, ख़ास कर इसके राग चांदनी केदार रूप का। चांदनी केदार में बसवराज राजगुरु और सोमनाथ मर्दुर जी की प्रस्तुति यू-ट्यूब पर सुननी चाहिए। और सितार में निखिल बनर्जी का चांदनी केदार। इसी कड़ी में है मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया- बसंत केदार।
ऐसा ही एक राग है अभोगी। अभोगी और अभोगी कान्हड़ा में मामूली सैद्धांतिक अंतर है, लेकिन श्रोता रूप में यह समझना कठिन है। यह किराना घराना के प्रिय रागों में है जिसे उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान, पं. भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, सभी नियमित गाते रहे। इस राग को सुन कर मुझे दरबारी कन्हड़ा से कोई साम्य नहीं नजर आता, सिवाय इसके कि इसमें भी गांधार (ग) आंदोलित है।। हाँ! बागेश्री से जरूर मिलता-जुलता है लेकिन अभोगी में पाँच ही स्वर है- सा रे ग म ध। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यह बागेश्री की तरह ही चित्त को शांत करने यानी तनाव (स्ट्रेस) को कम करने में सहायक है। पं. भीमसेन जोशी की बंदिश ‘मोरी लाज रखो’ सुन लें, यह वाकई स्ट्रेस-बस्टर है। यही बंदिश उस्ताद अमीर ख़ान ने पहले गाया है। उनके भी सबसे प्रिय रागों में एक है- अभोगी कन्हड़ा। झपताल में उनका एक बड़ा खयाल सम्पूर्णता में गायी गयी है। इसमें जो तान बनाए गाए हैं, वह इस राग को समझने के लिए काफी हैं, अगर बार-बार सुना जाए। इतना ही मधुर तराना भी है, जिसे उस्ताद खूब समझाते हैं। ऐसे ही एक दरभंगा घराने के प्रेम कुमार मलिक और प्रशांत मलिक की लंदन के दरबार फ़ेस्टिवल में गायी प्रस्तुति मैंने सुनी। खुले गले से गर्जन करते हुए तेज गति से गाना ध्रुपद के अमता (दरभंगा) घराना की विशेषता है। ‘री रा ना ना..’ से इस राग का संचारी गायन उस्ताद अमीर ख़ान के ‘ता ना दे रे ना’ से भिन्न नजर आएगा।
भक्ति की बात लिख रहा था, तो पटना का दुर्गा पूजा सहसा याद आ गया। पटना में गायकी या बजाना हर संगीतकार आज भी चाहता है। वहाँ पकिया श्रोता मिलते हैं, जो खर्च करें न करें, सुनते जरूर है। कभी सवाई गंधर्व फेस्टिवल, पुणे से बेहतर हुआ करता था पटना के दुर्गा पूजा का संगीत महाकुंभ। सब सुनी बाते हैं, मेरे किशोरावस्था के पूर्व की। कुछ झिलमिल यादें हैं, पर सच पूछिए तो एक पक्की स्मृति नहीं जिसे बयाँ कर सकूँ। उसकी बातें सुनी है।
पटना जंक्शन पर निखिल बनर्जी बजा रहे हैं, वहाँ से चलकर लोग गाँधी मैदान पहुँचते हैं तो बिरजू महाराज मिलते हैं। वह तो पटना से आज भी मोहब्बत करते हैं। कुछ वहीं रूक गए, कुछ लंगरटोली निकले तो पं. जसराज पंडाल पर राग भीमपलासी सुना रहे हैं। यहाँ जसराज हैं तो गोविंद मित्रा रोड पर भीमसेन जोशी। जो हल्का-फुल्का समझता है, जसराज को सुनने लगे, जो हार्ड-कोर हैं वो जोशीजी के पास खिसक लिए। यह गैंग आज भी बँटा हुआ है। जो जोशीजी के फैन हैं, उनमें कई जसराज को नहीं सुनते या सुनकर आलोचना करते हैं। सप्तमी की रात इनकी है तो अष्टमी को विलायत खान का दिन है। बिसमिल्लाह खान ने रात बिता दी, तो सुबह वी.जी. जोग भैरवी बजाकर नींद को छू-मंतर कर रहे हैं। रात इन शास्त्रीय गायकों की, और शाम के स्लॉट में अनूप जलोटा सरीखे भजन गा रहे हैं। सब की कद्र होती। पर सवाल ये होता कि दुर्गा पूजा में ‘राग दुर्गा‘ कौन गाएगा या बजाएगा? सीनीयर कौन है? उमर के हिसाब से कौन, घराने के हिसाब से कौन और तालीम के हिसाब से कौन? इस द्वंद्व में सुना है अक्सर वी.जी.जोग और बिसमिल्लाह खान की जुगलबंदी बाजी मार लेती। दुर्गा में इनका सानी नहीं। जगह भी गाँधी मैदान, पटना का केंद्र। क्या आलम होता होगा? अब तो सब मिट गया, खत्म हो गया। तिलिस्म था, टूट गया। जाने कहाँ गए वो दिन।
“जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में…”
यह गीत राग शिवरंजिनी में है। यह राज कपूर का प्रिय राग था और शंकर-जयकिशन ने कई गीत इस राग पर बनाए। चूँकि यह एक आसान राग है, तो भी इस पर गीतों का बनना लाजमी है। यह भूपाली की तरह मात्र पाँच स्वरों का राग है – सा रे ग (कोमल) प ध। इसमें भी भूपाली की तरह ‘मनी’ यानी मध्यम (म) और निषाद (नि) नहीं हैं। भूपाली और शिवरंजिनी में मामूली सा फर्क है कि भूपाली में गंधार (ग) शुद्ध है, और शिवरंजिनी में कोमल। इतनी बारीकी पकड़ना सबके बस की नहीं। लेकिन इस हल्के से परिवर्तन से ही मूड रूमानी (रोमांटिक) बन जाता है।
मेरा यह भी मानना है कि पाँच स्वर वाले औडव रागों का फ़िल्मी संगीत में काफी उपयोग हुआ है। जैसे राग जोग पर आधारित भी कई गाने हैं। पहाड़ी के आरोह में भी पाँच ही स्वर हैं। हालांकि पाँच स्वरों वाले हिंडोल पर अधिक गीत नहीं बने। शिवरंजिनी में एक राजन-साजन मिश्र का गाया भजन ‘राधा तुम्हरे नैनन में श्याम बसे’ मेरा प्रिय है। ऐसे ही एक संजीव अभ्यंकर जी ने गाया है- ‘तुम बिन कौन लेत खबर मोरी’।
एक दिन ख्याल आया कि विनाशकारी या श्रापित या वर्जित राग कौन सा है? यह कल्पना ही अजीब है। मशहूर पियानो वादक रैक्मैनिनोफ़ के कन्सर्टो 3 बजाने वाले पगलाने लगे थे। तांत्रिक पद्धतियों में कई मंत्र छुपा कर रखे जाते हैं कि किसी के हाथ लग गया तो विनाश कर देगा। कुछ ऐसा ही लोग ‘राग दीपक’ के विषय में कहते हैं। गुरु सिखाते नहीं। गायक मंच पर गाने से कतराते हैं। यू-ट्यूब पर ढूँढिएगा तो गिनती से मिलेंगे। यह राग तकनीकी रूप से लुप्त है। मृत है। भूत है। जब तानसेन ही इस राग से जल गए, तो बाकी कौन बचेगा?
यू-ट्यूब पर बैजू बावरा फिल्म का ‘आज गावत मन मेरो झूम के’ कुछ जगहों पर दीपक राग नाम से लिखा है, जो ग़लत है। वह राग देसी में है। के.एल. सहगल का ‘दिया जलाओ जगमग’ भी राग दीपक से मेल नहीं खाता। मुकेश का ‘दिल जलता है तो जलने दे’ भी कुछ लोग जबरदस्ती दीपक से जोड़ते हैं, पर वह भी इस राग में नहीं। शंकर महादेवन का ‘गजगामिनी’ में एक छोटा गीतोच्चारण है, जो इस राग पर लिखा कहते हैं।
एक गर्मी की दोपहर पं. रामचतुर मलिक (दरभंगा) का ‘राग दीपक’ सुनने लगा। पंडित जी पहले ही कह देते हैं कि इस राग को असल रूप में गाने वाला अब कोई नहीं। यह कोशिश भी अब कोई नहीं करता। ध्रुपद में राग दीपक सुन कर कुछ विचित्र अनुभव नहीं हुआ। शुक्र है, जलने से बच गया! फिर पं. भीमसेन जोशी (किराना) की सत्य साई बाबा के लिए प्रस्तुति सुनी। यह सुन कर महसूस होने लगा कि पंडित जी के पसीने छूट रहे हैं। भक्ति में भी भला क्या पसीने छूटते हैं? अब राग ही कुछ ऐसा है।
आखिर में ग़ुलाम मुस्तफा ख़ान (रामपुर सहसवान) को सुनने बैठा। चिड़चिड़े से उत्कट तीव्र, प्रचंड तक का स्पेक्ट्रम रहा। बस ये कहिए कि एक संगीत-प्रेमी भी पक गया। गमक तक पहुँचने के बाद तो इच्छा हुई कि अब बंद कर दूँ। जैसे-तैसे निपटा कर शॉवर में नहाया तो चैन मिला।
कुछ रागों का विलुप्त होना जनहित में ही है। लेकिन यह जिज्ञासा तो होती ही है कि संगीत के बंद दरवाजों को एक बार खोल कर देखा जाए। कौन से सच के जल जाएँगे? दीपक से हट कर इस प्रहर के एक खूबसूरत राग की बात करता हूँ।
उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान की राग झिंझोटी जब पंडित भीमसेन जोशी ने एक दुकान पर सुनी, वह घर छोड़ कर उनसे संगीत शिक्षा के लिए भाग गए। वह बंदिश थी-
“पिया बिन नाही आवत चैन/का से कहूँ जी की बात
याद आवत है निस दिन हाँ/उदासी बीति पूरी रैन।”
इसे कई संगीतकार हल्का-फुल्का या क्षुद्र राग कहते हैं, कि इस पर दादरा, टप्पा-ठुमरी खूब बनती है। वहीं दूसरी ओर, भारतीय विवाहों का मंगलाष्टकम् भी इसी राग में गाते हैं। दादरा-ठुमरी बनने का कारण यह भी है कि राग खमाज थाट में है, जो इनके लिए उपयुक्त है। एक शोभा गुर्टू जी का दादरा है- ‘हाँ पिया जावो जावो, मोसे ना बोले’। जब इस गीत में शोभा जी कहती हैं- भोर भए घर आए हो मेरे…तो एक करुणा का दर्द छलकता है, जो दादरा की रूह है। शुजात ख़ान ने अपने पिता की प्रिय भटियाली धुन को झिंझोटी में खूब निभाया है। स्वयं विलायत ख़ान और इसी घराने से शाहिद परवेज़ ने भी बेहतरीन झिंझोटी सितार पर बजाया है। एक मैहर की ख़ास खोज है – पहाड़ी झिंझोटी! इस राग ने अमरीका में खूब धूम मचाई। उस्ताद अली अकबर ख़ान और पं. रविशंकर, दोनों ने खूब बजाया। एक प्रस्तुति मैंने एक मित्र के माध्यम से सुनी जिसमें अली अकबर ख़ान और उस्ताद जाकिर हुसैन ने खूब जुगलबंदी की है। मुझे यह पूस की ठंडी रात में सुनना पसंद है, जब पहाड़ों पर बर्फ लदे हों और चाँद सामने मुस्कुरा रहा हो।
झिंझोटी की तरह, विवाहों के तीन और सुंदर राग हैं- बिहाग (या मारू बिहाग), मालकौंस और सोहनी। विवाह का मंडप सजा है। ढोल-तासे बजने बंद हुए, और शहनाई की धुन मद्धिम हुए। वर-वधू आकर मंडप में बैठ चुके हैं, और तभी राग बिहाग बज उठता है। प मं ग म ग/प नि सा ग…। गर मुझसे कोई पूछे तो इस माहौल के लिए इससे बेहतर कोई विवाह का राग नहीं। बिहाग हो या जयपुर-अतरौली वालों का बिहगड़ा हो। इसमें न विरह है, न प्रेम की लालसा है, न प्रेम की अभिव्यक्ति है, यह प्रेम की परिणति है। चिकित्सकीय भाषा में कहूँ तो जब प्रेम का ‘होमियोस्टैसिस’ हो यानी संतुलन स्थापित हो चुका हो, तब बिहाग सुनें। यह शृंगार का गंभीर रूप है। वह फ़िल्मी गीत इसे खूब कहता है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान शहनाई बजा रहे हैं और लता जी गा रही हैं, ‘तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिल कर बनेगी प्रीत’।
एक विलायत ख़ान साहब की भैनी साहब में बिहाग की रिकॉर्डिंग है। गुरुद्वारा में बैठ कर सितार बजाते विलायत ख़ान को करीब से देखना, और उनके सामने माला जपते सिख रसिकों की शांति। देवालयों में संगीत तो बजता ही रहा है। पर शास्त्रीय संगीत का जो समावेश गुरूग्रंथ में है, वह अद्भुत् है। जो सितार थोड़ा-बहुत बजाते हैं, उनको उस्ताद की उंगलियाँ बिल्कुल करीब से इस रिकॉर्डिंग में दिखेगी। इसमें वह समझाते हैं कि गर्मी से कैसे सितार के तार प्रभावित होते हैं और स्वर बदल जाते हैं। इसकी बंदिश में सुनिए कैसे सितार गाने लगता है- ‘री माँ! रंग है जी आज रंग’। यही है गायकी अंग। आखिर में तबला की जुगलबंदी पर भी गौर करिए।
बिहाग की एक मशहूर बंदिश ‘लट उलझे सुलझा जा बालम’ बड़े ग़ुलाम अली ख़ान और पं. जसराज से लेकर फ़िल्मी गीत तक आई है। यह छोटा खयाल को कभी पसीने से लथ-पथ अपने आखिरी दशक में गाते भीमसेन जोशी की आवाज में सुनिए।
लेकिन एक बिहाग प्रस्तुति जो दुर्लभतम है, वह है सत्यजीत रे की फ़िल्म ‘जलसाघर’ में सुरबहार पर बैठे संगीत के फकीर उस्ताद वाहिद ख़ान साहब। यह इकलौती रिकॉर्डिंग है जिसमें इनको देखा जा सकता है। अब उनके पोते शाहिद परवेज़ को भला कौन नहीं जानता? यह फ़िल्म तो हर संगीत-प्रेमी को देखनी ही चाहिए। एक और दुर्लभ प्रस्तुति है पं. रामेश्वर पाठक के बिहाग की, जो पं. रवि शंकर के आदर्श थे और जिनकी यह इकलौती रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।
12 बजे रात – 3 बजे सुबह (अर्ध रात्रि के स्वर)
“मालकौंस ऐसा राग है जिससे कोई कलाकार अपने जीवन में अछूता नहीं रह जाता।”
– रामाश्रय झा ‘रामरंग’ (राजन पर्रिकर की रिकॉर्डिंग से)
मालकौस को मैं अक्सर इसे भूत-प्रेतों का राग कह देता हूँ, जबकि राग मारवा इस उपमा के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन सोचिए, मालकौश का अर्थ ही है ‘कौशिक (साँप) की माला’ पहनने वाला। साक्षात् शिव। जब सती का मृत शरीर को लेकर शिव अपने रूद्र रूप में विचरण करने लगे, तो सती पार्वती रूप में ‘राग मालकौस’ गाने लगी। शिव क्रोध में तांडव कर रहे थे, और यह राग ही उन्हें शांत कर पाया। तो यह वीर रस का राग है। तलवारबाजी वाला वीर रस नहीं, आपके अंदर की दुर्भावनाओ के अंत का। जब क्रोध हावी हो जाए, सर पर खून सवार हो, राग मालकौस सुन कर ही शांति मिलेगी। यह आज की विश्व-स्थिति और ‘स्ट्रेस’ के समय में बिल्कुल उपयुक्त राग है। कभी-कभी सोचता हूँ, इस पाँच स्वरों के राग में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? संभवत: साक्षात् सती पार्वती से?
कहते हैं कि यही राग जब स्वामी हरिदास के मुख से अकबर ने छुप कर सुना तो कहा, “सुभानअल्लाह! मौसिक़ी ख़ुदा से रू-ब-रू हो रही है।”
मालकौंस और चंद्रकौंस का अंतर पकड़ना कठिन है। चंद्रकौंस में बस निषाद (नि) कोमल न होकर शुद्ध है। यह दोनों ही राग गंभीर प्रवृत्ति के हैं, और इसे सुनने के लिए भी गंभीर होना पड़ता है। नौशाद साहब जब मो. रफी से इसी राग में ‘मन तड़पत हरि दर्शण’ गवा रहे थे, तो पूरे सेट पर सबको पहले ही कह दिया कि रिकॉर्डिंग के लिए पाक (पवित्र) होकर ही आएँ। वाकई मैं भी जब मालकौंस सुनने बैठता हूँ तो यह माहौल बना लेता हूँ कि अब बीच राग में न उठना पड़े। इस राग में खलल पड़ी तो जिस तनाव से आप मुक्ति चाह रहे थे, वह फिर से आप पर सवार हो जाएगा। तभी तो कहा कि भूत-प्रेत का राग है।
यह गीत मालकौंस की ऐसी बंदिश पर आधारित है, जिसे हर संगीत-शिक्षक सिखाते हैं,
“कोयलिया बोले अम्बुआ की डार पर/ऋतु बसंत की देत संदेसवा
नव कलियन पर गूंजत भँवरा/उन्हीं के संग करत रंगरलिया/वही बसंत के देत संदेसवा”
बेतिया घराने के लोग मालकौस को प्रात:कालीन राग मानते रहे, जबकि अधिकतर घराने इसे देर रात का राग मानते हैं। मालकौस दरअसल एक प्राचीन राग है और इसका रूप समय के साथ बदलता गया। कुमार प्रसाद मुखर्जी मुग़लकालीन ‘राग दर्पण’ और ‘मान कुतूहल’ का संदर्भ देकर लिखते हैं कि यह प्रात:कालीन राग है। इंद्रकिशोर मिश्र (बेतिया घराना) के साक्षात्कार में सुना कि उन्होंने पटना रेडियो स्टेशन में मालकौस सुबह में गा दिया कि हंगामा हो गया।
मालकौस तो ऐसा राग है, जिसे हर गायक ने गाया है। इसकी वजह यह भी है कि यह इकलौता राग है जिसमें पाँच में से किसी भी स्वर पर न्यास ले सकते हैं यानी वहाँ रुक कर सुस्ता सकते हैं। इसमें दो प्रस्तुतियों का मैं जिक्र करुँगा। एक में गुरु ओंकारनाथ ठाकुर और उनकी शिष्या एन. राजम (वायलिन) पर वह मशहूर बंदिश ‘पग घुँघरू बाँध कर नाची रे’ गा रहे हैं। यह मीरा भजन कई लोगों ने गाया है; और यह स्पष्ट कर दूँ कि ‘नमकहलाल’ फ़िल्म में इसके पैरोडी गीत में किशोर कुमार ने राग दरबारी कन्हड़ा के सरगम को गाया है, मालकौस के नहीं। एक दूसरी प्रस्तुति सलामत-नजाकत अली ख़ान की धुआँधार मालकौस है, जिसे सुना ही जाना चाहिए। मालकौस की यह द्रुत लय (फ़ास्ट-पेस) अद्भुत है। यही बंदिश ‘तोरे बिना मोहे चैन नहीं आवे’ उस्ताद राशिद ख़ान ने राग किरवानी में गाया है।
राग दरबारी कन्हड़ा से मिलता राग है अडाना, लेकिन इसकी अलग खूबसूरती है। जो गंधार (ग) दरबारी में महत्वपूर्ण है, वह अडानी के आरोह में है ही नहीं। तो सोचिए, राग क्या बन कर निकलेगा? जो दरबारी और अडाना में फँसे हैं, वह इस स्वर पर विशेष ध्यान देकर सुलझा सकते हैं। लेकिन यह दोनों राग उलझे ही ठीक हैं। जहाँ दरबारी में कोमलता, नज़ाकत और नफ़ासत है; अडाना उत्साह भरा जोश लाने वाला, तेज गति का राग हैं। राजन पर्रिकर ने मजाकिए लहजे में लिखा है कि दरबारी अगर प्रिय धर्मपत्नी है, तो अडाना वह ‘हॉट बेब’ है जिसे कनखियों से देख लेते हैं। जो देर रात लिखा-पढ़ी करते हैं, उनके लिए काली कॉफ़ी के साथ राग अडाना मेरा अनुमोदन है। यह राग ध्रुपदियों का प्रिय राग है, जिसके मध्य में अगर शूल ताल हो तो इसकी गति देखते बनती है। शूल ताल ध्रुपद का दस मात्रा वाला मोहक ताल है, जो चौताल से भिन्न और अधिक ऊर्जा वाला नजर आता है। तो इसमें अडाना का वीर रस निखर जाता है, ख़ास कर जब पखावज बजा कर महादेव या भगवती वंदना करनी हो। यह प्रस्तुति मैंने प्रशांत मलिक (दरभंगा घराना) की सुनी है- ‘त्रिवेणी कालिंदी माँ’। भगवती काली की एक बंदिश पं. जसराज भी अडाना में गाते हैं- ‘माता काली भवानी’ (लिंक की शुरुआत में गलती से बसंत लिखा है)। इस राग का समय ही काली-पूजा (निशा पूजा) के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह अन्य अवसरों पर भी गायी जाती है। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे ने अडाना में होरी (होरी खेलत नंदलाल) भी गायी है।
अडाना की एक बंदिश का मुखड़ा मन से चिपकने वाला है- ‘झनक झनक पायल बाजे’। यह उस्ताद अमीर ख़ान से कौशिकी चक्रवर्ती तक ने गाया है। फ़िल्मी बंदिश में अडाना का एक उदाहरण है- ‘राधिका तूने बँसुरी चुरायी’, जिसमें दरबारी और अडाना का घालमेल है। यह मेरी अपनी धारणा है कि अडाना की गति और जोश के साथ न्याय या तो ध्रुपदिए कर सकते हैं, या खयालियों में पटियाला के तान कप्तान। जैसे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की गायी- ‘सबहि गुन मिले’; या फतेह अली ख़ान की गायी बंदिश- ‘तान कप्तान’!
रात का समय राग जोग का भी है। राग जोग और राग तिलंग को फर्क करना टेढ़ी खीर है। दोनों एक से ही हैं, बस एक शुद्ध गांधार का अंतर है। यह राग यूँ तो नया राग है, लेकिन इसके तार अकबर के समय के हाजी सुजान ख़ान तक से मिलता है। उनकी बनायी बंदिश ‘प्रथम माना अल्लाह’ इसी राग में गायी जाती रही, और आगरा घराने में लोकप्रिय रही। पं. रविशंकर ने जोग और बागेश्री मिला कर ‘जोगश्री’ राग की रचना की, जो सितार पर खूब जमता है। ऐसे ही जगन्नाथबुवा पुरोहित (आगरा घराना) ने राग जोग और चंद्रकौंस मिला कर ‘जोगकौंस’ की रचना की। यह राग भी आधुनिक काल में बहुत प्रचलित हुआ।
इसकी प्रस्तुतियों में एक 1962 ई. में उस्ताद अमीर ख़ान का गाया जोग है, जिसका तराना सुनना चाहिए। उस्ताद तराना के निरर्थक शब्दों में भी अर्थ ला देते थे। यह राग एक बार पं. हरिप्रसाद चौरसिया ने हॉलैंड की महारानी के लिए उनके राजमहल में 1990 ई. में बजाया था। इनकी बाँसुरी के साथ पं. जसराज और उस्ताद जाकिर हुसैन की जुगलबंदी राग जोग का खूबसूरत माहौल बनाती है। एक एन. राजम की वायलिन पर बजायी जोग भी अद्भुत् है।
दूरदर्शन के युग में सुबह ‘वंदे मातरम्’ से होती, और बाद में दूरदर्शन पर एक और विडियो आया ‘बजे सरगम हर तरफ से’। इन गीतों से कड़कड़ाती ठंड में भी नींद अच्छी खुलती। यह दोनों ही राग देस में हैं। तो जब रात सुबह की ओर बढ़ने लगे, तब देस सुनना चाहिए। मुश्किल यह है कि इतनी रात तक जगेगा कौन? लेकिन अगर मौका मिले तो ब्रह्म-मुहूर्त के कुछ पूर्व ढाई-तीन बजे रात को राग देस सुनना चाहिए। संगीतकार इसको राग तिलक कामोद के करीब बताते हैं, और यह भी कि देस को निभाना कठिन है। लेकिन सुनने में खमाज थाट का यह राग सहज लगता है। ‘वन्दे मातरम्’ तो हम छुटपन से गाते रहे हैं।
Buy book Wah Ustad here – https://www.amazon.in/Wah-Ustad-Praveen-Kumar-Jha/dp/9389373271
Buy book Wah Ustad here – https://www.amazon.in/Wah-Ustad-Praveen-Kumar-Jha/dp/9389373271
Buy book Wah Ustad from this link – https://www.amazon.in/Wah-Ustad-Praveen-Kumar-Jha/dp/9389373271