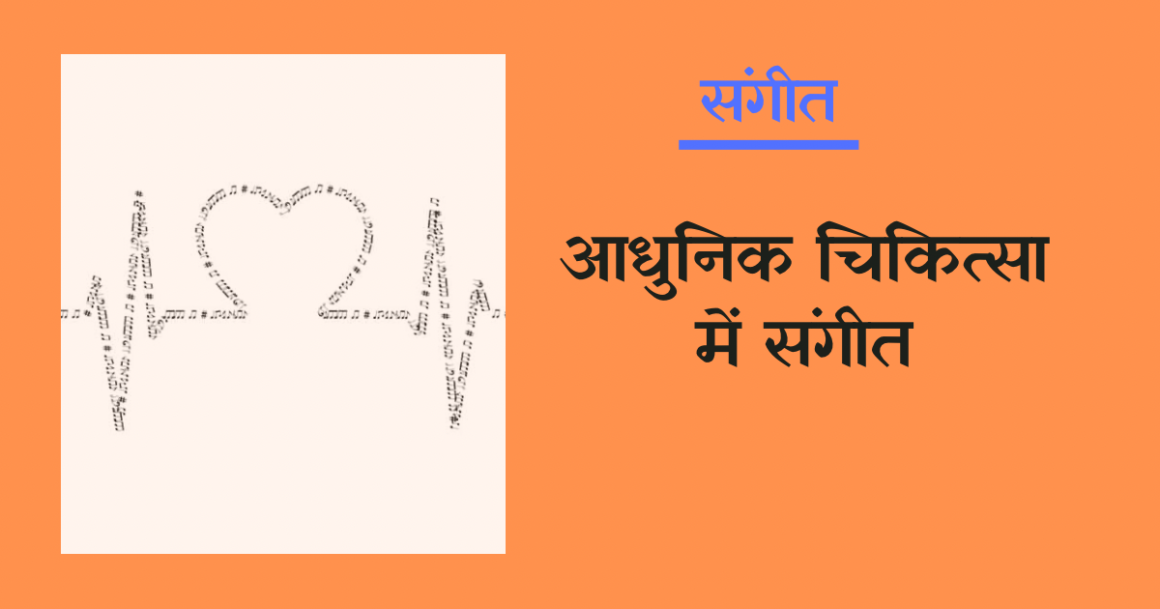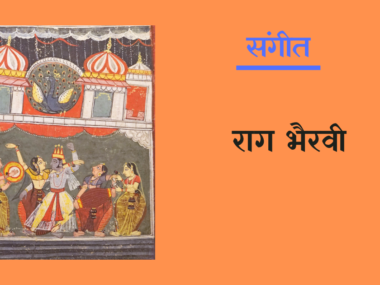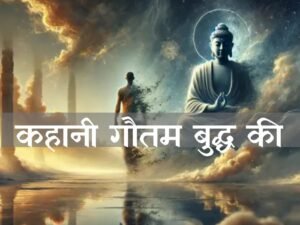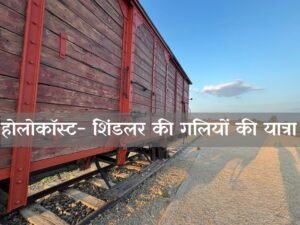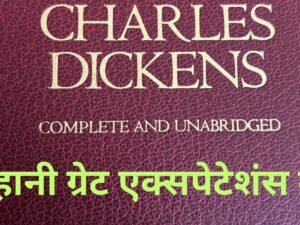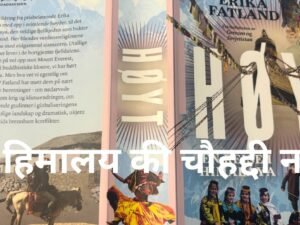संगीत चिकित्सक या ‘म्यूजिक थेरापीस्ट’ मेरे लिए भी नया शब्द है। या यूँ कहिए ऐसी किसी भी विधा को फिलहाल एलौपैथी ने पक्की मंजूरी नहीं दी है। आयुर्वेद में अगर इसकी चर्चा है भी, तो आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्रयोग में नहीं है। पश्चिम में इसका प्रयोग अलग-अलग स्थानों पर एक प्रयोग के तौर पर ही हो रहा है। महाराष्ट्र में कई हस्पतालों और एलोपैथिक संस्थानों में इसका प्रयोग दो दशक से हो रहा है, लेकिन इसकी समीक्षा नहीं हुई। हिंदुस्तानी संगीत से थेरैपी की बात आजादी से पूर्व से ही चलती आ रही है, लेकिन उस पर भी किसी इंडेक्स जर्नल में लेख ढंग से नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति ‘संगीत चिकित्सक’ का बोर्ड लगा कर बैठे तो मध्य-वर्ग से एक भी व्यक्ति उनके केबिन में दाखिल होगा। इस तरह की रिलैक्सिंग थेरैपी, नाद-योग या पैरासाइकोलॉजी आदि उच्च वर्ग के चोंचले ही माने जाते हैं। लेकिन, मैं इस विषय को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता रहा हूँ, और दिमाग के फंक्शनल एम.आर.आई. पर काम करते समय कुछ प्रयोग भी किए। हालांकि मैं भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा क्योंकि इस तरह के शोध के लिए बहुत अधिक समय, संसाधन और डाटा चाहिए। झारखंड में रांची मेडिकल कॉलेज (रिम्स) में इस पर शोध हुअा है, जो प्रकाशित भी हुए। दरभंगा में भी लावण्य कीर्ति जी ने इस विषय पर शोध किया है या शायद कर रही हैं, जिसकी जानकारी मुझे हाल में मिली। मेरी स्वयं हिंदुस्तानी संगीत में रुचि भी है, कुछ लिखता-पढ़ता भी रहा हूँ और पेशे से चिकित्सक हूँ, तो एक सोच बनाने की चेष्टा करता रहा हूँ। इसमें कई तर्क मुझे ठीक भी लगते हैं, कुछ में शंका है, और कुछ मुझे बेतुके भी लगते हैं। जैसे संगीत से कर्करोग (कैंसर) का ठीक हो जाना न सिर्फ असंगत लगता है, बल्कि अनैतिक भी। ठीक इसी तरह गठिया ठीक होने पर मुझे शंका है कि यह अतिशयोक्ति है। एक बार ओंकारनाथ ठाकुर, जो अपने समय के संगीत थेरापी में विख्यात नाम रहे, ने शायद कहा कि, “हिन्डोल राग से गठिया ठीक हो जाता है”। ऐसी चर्चा कुमार प्रसाद मुखर्जी की पुस्तक में है। तो श्रोताओं ने टोंट कसा कि फिर आपका गठिया क्यों नहीं ठीक होता?
तो हमें विज्ञान की सीमाओं के हिसाब से ही संगीत-चिकित्सा की भी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कि क्या प्रैक्टिकल (प्रायोगिक) है। ख़ास कर जब हम पश्चिम के वैज्ञानिकों को यह समझाना चाहें और इसे वैश्विक रूप से स्थापित विद्या बनाना चाहें। क्योंकि पश्चिमी संगीत ने तो धीरे-धीरे अपने तर्कों को सत्यापित कर इसे अमरीकी चिकित्सा बोर्ड द्वारा पास करा लिया है। हर रोग में तो नहीं, लेकिन कुछ रोगों में इसको एक सहायक विधि रूप में स्थान मिल गया है। दूसरी बात कि हमें इसे आधुनिक चिकित्सा के मानकों पर ढालना होगा, जो मुश्किल नहीं, बस शब्द बदल जाएँगे।
मैं अमरीका में अलझाइमर पर शोध से जुड़ा था। उस समय मुझे एक शोध-पत्र मिला कि अलझाइमर के मरीज जिनकी स्मृति क्षीण हो चुकी है, वह गीत की धुन या पहली पंक्ति सुन कर अगली पंक्ति गुनगुनाने लगते हैं। बाद में यह मैंने मरीजों में देखा भी कि अखबार पढ़ने की क्षमता खत्म हो गयी, लेकिन संगीत का आनंद ले रहे हैं। नॉर्वे में एक पार्किंसन से ग्रस्त वृद्ध जिनका पूरा शरीर काँपता रहता, अस्पताल के लॉबी में आकर पियानो बजाने लगते। उनकी तो यह हालत थी कि कपड़े का बटन खुद नहीं लगा पाते, लेकिन पियानो बजाते वक्त ऊँगलियाँ बिल्कुल ठीक। गजेंद्र बाबू ने अपने संस्मरण में लिखा है कि पं. रामचतुर मल्लिक पटना के इंदिरा गांधी हृदय संस्थान में बीमार लेटे हुए हैं। निर्बल रोगी रूप में। लेकिन, अचानक उनको देखते ही गुनगुनाने लगते हैं और फिर वही पुरानी आवाज। लेकिन संगीत के अतिरिक्त उनकी आवाज शिथिल है। भला यह कैसे संभव है? पहले लोग मानते थे कि दिमाग का दाहिना हिस्सा कला और संगीत का हिस्सा है, और बायाँ हिस्सा भाषा और गणित का है। लेकिन जब संगीत सुनते हुए ‘फंक्शनल एम.आर.आई.’ किया गया, तो दिमाग के दोनों हिस्सों में कई स्पॉट नजर आए। यानी अगर दिमाग के कई हिस्सों में लकवा मार जाए, स्ट्रोक हो जाए, फिर भी संगीत की क्षमता खत्म नहीं होगी। क्योंकि यह एक मकड़े के जाले की तरह नेटवर्क से बनता है। अगर दाहिने-बायें वाली बात को सही भी मानें तो संगीत में भाषा भी है, और गणित भी। तो इसकी सत्ता दिमाग के दोनों हिस्सों में है। जाहिर है कि इसका प्रभाव कई बिंदुओं पर होगा। इसलिए सोए मष्तिष्क को जागृत करने का, या जागृत मष्तिष्क को सुलाने का यह सबसे कारगर साधन सिद्ध हो सकता है। माँएँ तो कब से लोरी सुना कर बच्चों को सुलाती ही रही हैं। या जब वह अधिक रोते रहते हैं, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए भी ताली बजा-बजा कर गाने लगती हैं। कई परिवारों में नींद खुलती ही है जब पूजा की घंटियाँ या भजन बजने लगता है, या मस्जिद का अजान पढ़ा जाता है। तो जागृत मष्तिष्क को सुलाना, या सुसुप्त मष्तिष्क को जगाना। दोनों ही संभव है।
दूसरी बात है संगीत से भावनाओं का संचार। राग और रस की व्याख्या से पहले यह तो साधारण सा अनुभव है कि फ़िल्मों के बदलते सीन के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बदलता है। किसी डरावने सीन का संगीत अलग, किसी रोमांटिक सीन का संगीत अलग। हमें डायलॉग से अधिक वह बैकग्राउंड म्यूजिक उस मूड में ले जाता है। आप संगीत बदल दीजिए, उसी डायलॉग पर मूड बदल जाएगा। यह बात मिथिला में ही सदियों पहले कार्नाट वंश के संस्थापक राजा नान्यदेव ने अपनी पुस्तक ‘भरत भाष्य’ में बहुत सरल रूप में समझाया है। उनके अनुसार जब विलंबित लय (स्लो पेस) में गाया जाए तो करुणा रस जन्मेगा; मध्य लय में गाया जाए तो हास्य और शृंगार रस; और द्रुत लय (फास्ट पेस) में गाया जाए तो वीर रस, रूद्र रस या भयानक रस जन्मेगा। यही फ़िल्मिस्तान के लोग भी अपनाते हैं। आप अमिताभ बच्चन वाला वह गीत याद करिए- ‘प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया’। देखिए कैसे गीत करुणा रस से प्रारंभ होता है और लय तेज होते-होते वीर रस में बदल जाता है। तो यह कोई रॉकेट-साइंस नहीं है कि संगीत से भावनाओं का संचार होता है। मनोरोग में जब भावना-शून्यता हो या एक भावना (जैसे अवसाद) अधिक प्रधान हो गयी हो, तो उसे बदलने के लिए संगीत का प्रयोग हो ही सकता है। तनाव में, अवसाद में, या भावना-शून्य ‘वेजिटेटिव स्टेट’ में। और यही प्रयोग दिमागी चोटों के बाद महाराष्ट्र में किया भी जा रहा है। पश्चिम में तो पहले से है।
हम जब संगीत सुनते हैं, तो दिमाग में एक साथ कई घटनाएँ होती है। एक ध्वनि तब तक ही ध्वनि है जब उसे सुनने वाला कोई हो। अगर सुनने वाला कोई न हो तो वह एक कंपन मात्र है। उस कंपन को ही जब मनुष्य या पशु का दिमाग सुनता है, तो उसके कान से गुजर कर दिमाग से होते हुए, एक ध्वनि बनता है। तालाब से ध्वनि नहीं सुनते, लेकिन नदी से सुनते हैं। जबकि हैं दोनों पानी ही। हमारा दिमाग कंपन को पकड़ लेता है, ध्वनि के माध्यम से। यह कि आस-पास कुछ हिल रहा है। अगर एक बेहोश व्यक्ति के कान में यह संगीत डाल दिया जाए, तो उसके कानों की हड्डियों में कंपन होगा, और उसे शायद ध्वनि सुनाई दे। अगर उसका दिमाग इस कंपन को पकड़ पा रहा है, तो वह शायद यह भी समझ जाए कि कमरे में एक व्यक्ति चहल-कदमी कर रहा है। क्योंकि दोनों दरअसल एक ही चीज हैं अलग-अलग फ्रिक्वेंसी की।
हम यह भी समझ पाते हैं कि यह पुरुष की आवाज है या स्त्री की। यह किशोर कुमार की आवाज है या मुकेश की। क्योंकि दोनों के गले का पिच (स्वर-मान) अलग-अलग है। किसी की आवाज भारी है, तो किसी की पतली। जैसे फर्श पर एक स्टील की प्लेट गिरे और एक टेनिस बॉल गिरे, तो अलग-अलग पिच की ध्वनि निकलेगी। और हमें एक मरीज, जिसे सर में चोट लगी है, उसे इसी काबिल बनाना है। तो हम अलग-अलग पिच से परिचय कराते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में जैसे राग दरबारी मंद्र सप्तक का राग है, जिसे पुरुष ही अक्सर गाते हैं। महिलाओं में जिनकी आवाज भारी रही, जैसे गंगूबाई हंगल, वही गा सकी। वहीं खमाज या काफी में ठुमरियाँ बनी, जिसे महिलाओं ने खूब गाया। मधुवन्ती महिलाएँ पसंद करती हैं। उसका पिच अलग है। इसी बदलाव को संगीत-चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है कि दिमाग अलग-अलग स्वरमानों को पहचान सके, और आँख बंद कर भी कह सके कि यह उसके पिता की आवाज है और यह माँ की आवाज है। अलग-अलग पिच पर संगीत सुना कर पहचानने की क्षमता बढ़ते हुए देखा गया है।
इतना ही नहीं, एक ही स्वर जब सितार से निकलता है और जब गिटार से निकलता है तो उसमें फर्क आप कर पाते हैं। यह ‘टिम्बर’ है। इसके लिए संगीतज्ञ होना जरूरी नहीं है। यह तो कोई भी कह देगा कि अमुक ध्वनि सितार की है, अमुक ध्वनि बाँसुरी की, भले स्वर एक ही हों। तो राग बदलने के साथ हमें वाद्य-यंत्र भी बदल-बदल कर सुनाने होंगे। अक्सर संतूर और बाँसुरी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ बाँसुरी एक साधारणतम यंत्र है, जिसे दिमाग जल्दी समझ पाता है; संतूर एक शत तंत्री (सौ तारों वाला) यंत्र है, जो एक साथ दिमाग के सौ बिंदुओं को जागृत कर सकते है।
हम लय भी समझते हैं। कि ताल क्या है, समय किस तरह से बाँधा गया है। किस स्वर को कितना समय दिया गया है। एक मरीज जिसका संतुलन किसी कारण गड़बड़ हो गया है। यानी उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, या आवाज काँप रही है; उसे अगर संगीत के लय सुनाए जाएँ तो उसका शरीर भी एक लय में आ जाएगा। ‘धा धिन धिन धा’ के साथ उसके शरीर के अंग भी बिल्कुल सिन्क्रोनाइज होते चलेंगे। वह ताल के साथ चलेगा और सम आते ही रुकेगा। आप गौर करिए तो हृदय से लेकर हमारी चाल तक, सब ताल-बद्ध है। मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, तो एक ख़ास ताल में बोल रहा हूँ। कहीं तेज, तो कहीं रुक रहा हूँ। आप लिख रहे हैं तो आपकी उँगलियाँ एक ताल में चल रही हैं। यह ‘कोऑर्डिनेशन’ अगर कोई भूल गया हो, जैसे मैंने पारकिन्सन बीमारी की चर्चा की, तो उसे भूले हुए ताल संगीत याद करा सकते हैं।
संगीत से जुड़े लोगों में कई लोग लगभग सौ वर्ष से अधिक भी जीए, जैसे- उस्ताद अलाउद्दीन ख़ान, विलायत हुसैन ख़ान, करमतुल्लाह ख़ान, अहमद जान थिरकवा, ग़ुलाम रसूल ख़ान, कृष्ण राव पंडित, रज़ब अली ख़ान, अब्दुल रशीद ख़ान। और कमाल की बात कि सब खूब खाते-पीते लोग थे, जिनकी जीवन-शैली कोई बहुत स्वास्थ्य-निमित्त नहीं मानी जाएगी। तब तो संगीत था कि उम्र के अंत तक गाते-बजाते रहे। विलायत हुसैन ख़ान की थ्योरी है कि वे लंबी तान लेने के लिए साँस का रियाज करते थे। आम आदमी जितनी देर साँस रोक सकता है, गायक उससे लंबी देर तक साँसों पर नियंत्रण रख सकता है। तो यह एक तरह का प्राणायाम है, जिससे उम्र बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे तैराकी में साँसों का नियंत्रण इसे एक बेहतर साँस और हृदय का व्यायाम बनाता है।
राजन-साजन मिश्र से एक बार पूछा गया, “आप इतना पान खाते हैं। ठंडा पीते हैं। कैसे स्वस्थ रहते हैं?”
उन्होंने हँस कर कहा, “बेग़म अख़्तर तो सिगरेट पीती थीं। खूब ठंडा पीती थीं। संगीत सब पचा लेता है।”
यह बात तो है कि संगीतकारों को शराब और नशे का खूब शौक रहा। लेकिन इसमें कई बरबाद भी हुए और कईयों की असमय मृत्यु भी हुई। बल्कि स्वस्थ संगीतकार वही हुए जो सुबह उठ कर रियाज करते, टहलने-दौड़ने जाते, और फिर आकर रियाज करते। कुछ तो कुश्ती और दंड-बैठक भी करते। लेकिन यहाँ बात करता हूँ ‘म्यूज़िक-थेरापी’ की, जिस पर एलोपैथिक डॉक्टरों को भी विश्वास होने लगा है और अस्पतालों में स्थापित हो रही है। लेकिन इसमें सीमाएँ निर्धारित करनी जरूरी है। इसे जादुई विद्या बनाने से बचना चाहिए। चित्त शांत कर दे, तनाव घटा दे, नींद ला दे, या सोए दिमाग को आंदोलित कर दे, यह मुमकिन है। लेकिन राग सुन कर कैंसर का इलाज हो जाए, यह असंभव है।
हिंदुस्तानी संगीत में ओंकारनाथ ठाकुर के बाद भी इस विषय में प्रयोग होते रहे, लेकिन इनका वैज्ञानिक विश्लेषण या यूँ कहिए कि चिकित्सकीय विश्लेषण कम ही हुआ। पश्चिमी संगीत से ही अधिकतर ‘म्यूज़िक थेरैपी’ सेशन हो रहे हैं। हालांकि मैं हिंदुस्तानी संगीत में उससे बेहतर ही संभावना देख रहा हूँ।
रेडियो सीलॉन के समय देर रात अक्सर राग पीलू पर आधारित गीत आते। बल्कि रात के रागों की संरचना ही कुछ ऐसी है कि चित्त शांत हो जाए और हमें बेहतर नींद आए। इसी को शोधियों ने अब सिद्ध करना भी शुरू किया कि राग पीलू और दरबारी कन्हड़ा से नींद अच्छी आती है। पुणे के एक डाक साहब ने तो अपने मरीजों को जब राग दरबारी सुनाना शुरू किया तो उनकी नींद की गोली आधे डोज़ की कर दी। और वह कहते हैं कि यह कारगर है। मैं भी राग दरबारी सुन कर अक्सर सोता हूँ और पसंदीदा राग है तो नींद अच्छी आती ही है। ख़ास कर विलायत ख़ान साहब का सितार या उस्ताद अमीर ख़ान की बंदिश। एक और राग जो मेरा प्रिय है और इस कड़ी में महत्वपूर्ण, वह है- राग किरवानी। इस पर अलग से शोध का पता नहीं, लेकिन नींद के लिए सुंदर राग है।
तनाव अधिक हो तो यमन कल्याण से शुरु कर बागेश्री या दरबारी से अंत करना कारगर है। यह मेरा मानना है कि तनाव के समय गायन से बेहतर कोई वाद्य-यंत्र है। जैसे सरोद, सितार या सुरबहार। उनका स्केल बहुत अधिक नहीं बदलता। जबकि गायकी में हर गायक का स्केल अलग है और तान के पैटर्न भी भिन्न हैं। तनाव घटने की बजाय बढ़ न जाए, इसलिए इंस्ट्रुमेंटल बेहतर है। तनाव घटाने में एक और राग सुंदर और प्रभावी है- अभोगी कन्हड़ा। एक शोध-पत्र पढ़ रहा था कि अत्यधिक तनाव या अवसाद में राग मधुवंती और राग बिहाग को अवसाद में उपयोगी बताया है। लेकिन ऐसी स्थिति में डाक्टरी सलाह अधिक जरूरी है।
हिन्दोल वीर रस का राग है, जिसे हड्डियों और जोड़ों के रोग में उपयोगी बताया गया है। जयंती कुमारेश और जयदीप घोष ने एक म्यूज़िक थेरैपी पर शृंखला निकाली, उसमें हिंदोल से इस रोग में मदद की बात कही है। संगीत से गठिया ठीक होने पर तो मेरा विश्वास नहीं, लेकिन दर्द घटाने या दर्द की अनुभूति कम होने की बात हो सकती है। यह राग सूर्योदय से पूर्व बिस्तर पर लेटे-लेटे मैं अक्सर सुनता हूँ, और सूर्य की किरणें जब आखिर पड़ती हैं तो ताजगी के साथ उठता हूँ।
बंबई के डॉ. केनी ने संतूर के साथ प्रयोग किए और उनका मानना है कि यह शत-तंत्री यंत्र है, इसलिए यह शरीर पर बहुआयामी प्रभाव डालता है। इसे मानसिक रोगियों में भी अपनाया जा सकता है, ख़ास कर उनमें जिन्हें रोग है नहीं लेकिन मन में बैठा है। साइकोसोमैटिक समस्याओं में एक ‘प्लैसिबो’ की तरह। इसके अतिरिक्त राग यमन, बागेश्री, और तिलक कामोद कुछ अन्य रोगों जैसे माइग्रेन, गठिया और रीढ़ के दर्द में राहत दे रहे हैं। यह सब दर्द को मानसिक रूप से घटाने के तर्क हैं, जो ठीक लगते हैं।
मुझे यह संदर्भ कई जगह मिला कि लिवर की समस्या में राग श्री उपयोगी है। इसके ऋषभ (रे) ध्वनि से लिवर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही कई अन्य सिद्धांत मिले। इनमें एक भी वैज्ञानिक तरीके से एक बड़े सैम्पल साइज़ पर नहीं किया गया। अभी तो आलम यह है कि हिंदुस्तानी संगीत सुनने वाले गिने-चुने हैं। जो नहीं सुनते, उनका तो सुनते ही सर फटने लगता है। जब तक कानों को यह प्रिय न लगेंगे, कोई राग कुछ नहीं कर सकता। और जब प्रिय लगने लगेंगे तो मर्ज का इलाज हो न हो, मर्ज आदमी कुछ देर भूल जरूर जाएगा।
(रमानाथ हेरिटेज सीरीज़ अंतर्गत डॉ. प्रवीण झा का सी.एल. दास मेमोरियल लेक्चर. जुलाई, 2019)