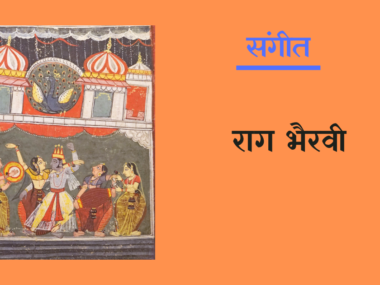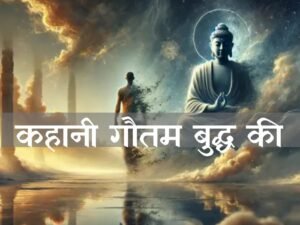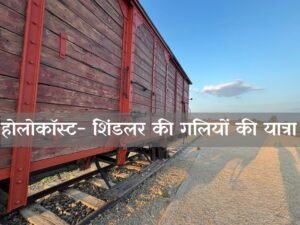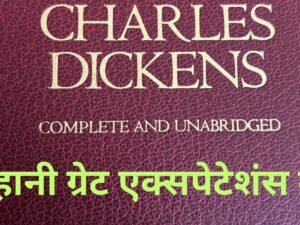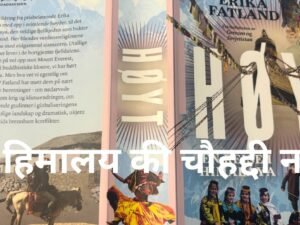चैती का सिग्नेचर है ‘हो रामा’। हालाँकि यह कोई नियम नहीं, लेकिन बहुधा उपयोग में है। इस टेक से आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि चैती गाया जा रहा है। बाकी, नाम से तो स्पष्ट ही है कि चैत में गाया जाएगा। लेकिन, आज एक प्रश्न मुझे मिला कि चैती में विरह का स्वर क्यों?
एक तो लोकगीतों में विरह का स्वर प्रमुख यूँ भी होता है, चाहे बिदेसिया हो, कजरी हो, और बिरहा (मूल रूप) तो खैर बना ही ‘विरह’ से है। लेकिन, चैती में थोड़ी प्रेम भरी मिन्नत है, थोड़ा संकोच है। गाँवों में नवविवाहिता जब ब्याह कर लायी जाती है, तो अपने पति से भी संकोच में रहती है। पति दिन भर खेती-मजदूरी कर लौटा, संयुक्त परिवार है, पत्नी का विरह तो वहीं से शुरू हो जाता है। और वह भी चैत तो होली के बाद रबी फसल (जैसे गेहूँ) का कटाई का समय है। पत्नी अगर खेतों में साथ रही भी, तो दोनों व्यस्त रहेंगे। थक कर मिट्टी में लथपथ सो जाएँगे। लेकिन, उम्मीद रहेगी कि जब फसल बाज़ार जाएगी, तो कमाई होगी। मुझे कुछ सिला देगा, गहना ला देगा। तो थोड़ी शिकायत-मिन्नत भी कर ली जाए।
इसके दूसरे पहलू पर भी ग़ौर किया जाए। ‘हो रामा’ में क्या सूत्र है? यूँ तो यह कई लोकगीतों में प्रयोग में है, लेकिन चैत के समय राम का जन्म हुआ। यह एक बिंदु है। सीता के जीवन में नवविवाहिता समय से ही विरह जुड़ गया। वह साथ भी रहीं, तो राम चलायमान रहे। उसके बाद भी सीता-हरण से विरह उत्पन्न हुआ, और अयोध्या लौट कर पुन: विरह।
एक और बात है कि यह पूरबिया चीज है। पूरब का ग्राम्य-जीवन और संस्कृति मिट्टी से जुड़ा रहा है। दरभंगा महाराज जैसों को छोड़ दें तो वहाँ के कई जमींदारों में भी राजा-नवाबों की शान शायद न मिले। कुछ धोती में खुले देह बैठे मिल जाते, कुछ तो गाय-बथान करते भी। लखनऊ की दरबारी नज़ाकत और शान में जो उपज हुई, उससे भिन्न उपज गया, मिर्जापुर, मिथिला, भोजपुर, मगध में हुई। तभी उसकी बंदिशों में पोखरिया, खोतवा (घोंसला), सेजिया (बिस्तर) जैसे शब्द मिलेंगे। बल्कि, वहाँ के दरबार में जो तवायफ़ थी, वह भी नाचती कम, और खड़े-खड़े मुखमुद्रा बनाते, इस्स करते, कनखी मारते, अधिक गाती। यानी कमर, बाँह, चक्कर लगाने कम या नदारद। तो वहाँ से भी जो चैती जन्मी, उसके भी स्वर बदल गए
‘एहि ठइयाँ मोतिया हेराय गइल हो रामा’ या ‘सेजिया से सइयाँ रूठ गइए’
मिथिला में तो भक्ति-प्रयोग भी हुए और वहाँ भोला बाबा को ले आए- ‘डिम डिम डमरू बजाबय हो रामा’। इसमें पार्वती और शिव को एक्सप्लोर किया गया कि पार्वती अपना विरह-गान गा रही हैं।
कालांतर में पूरब का केंद्र बनारस बनता गया, और वहाँ सभी धाराओं का संगम हो गया।
चैती गायकी में एक ख़ास बात यह भी है कि मीटर बदलने से और पॉज बदलने से उसका मूड बदलता जाता है। एक ही गीत ‘सब बन अमवा बहुरन हो रामा, सइयाँ घर नाही’ को अलग-अलग अंदाज़ में गाकर करुणा भी जन्मती है, संकोच से प्रेम का इज़हार भी, शिकायत भी, मिन्नत भी। चैती सीधे-सीधे हड़बड़ी में गाने की चीज नहीं है, इसको खींच कर, सुस्ता कर गाना होता है। दीपचंडी ताल में। जैसे फ़िल्मी गीत में ‘अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा’। सम्भव है कि चैती में बारह मात्रा तक स….इ…याँsss ही चलेगा। इसमें पुकार भी है, सइयाँ पास नहीं बैठे, उठ कर चले गए या आए ही नहीं। काम करते-करते भी शाम को गाया जा रहा है, लगनी या जाँतसर जैसे, थोड़ी थकान के साथ, लेकिन बुलंद स्वर में।
चैत का जब नव-स्वेद बहता है, तब जाकर साँझ में चैती उपजता है।
देवेंद्र नाथ तिवारी अपने लेख में कुछ और बातें लिखते हैं,
चैता का सम्बन्ध नव वर्ष के उल्लास से है। इसमें सभी नौ रस की प्रधानता है। चैत के उल्लास में विरह या वियोग का उपयोग। इसमें दुराव का स्थान नहीं। इसके तीन रूप हैं – चैता, चैती और घाँटो।
चैता का स्वरूप ‘रूढ़ आरोह’ है, जब महज़ दो-तीन पंक्तियों से शृंगार वर्णन होता है, जैसे
अहि ठइयाँ है रामा अहि ठइयाँ, रामजी के जनमवा भेल अहि ठईयां
दूसरा उदाहरण है
चैत में रामजी जनमले ए रामा, चैत मासे/ घरे घरे बजेल बधैया ए रामा चैत मासे
चैती में इसका साहित्यिक काव्यात्मक भाव प्रधान रूप उभर कर आता है। जैसे-
मारी देली कान्हा जी के मतिया/हो रामा कुबरो सवतिया/काटे धावे चैत के रतिया/हो रामा कुबरो सवतिया
ज़ौहर
चढल चैत चित लगे ना रामा/बाबा के भवनवा/कब होईए पिया से मिलनवा हो रामा/बाबा के भवनवा
घाँटो एक अभिव्यक्ति शैली है जिसमें चैत के सम्बन्ध में वाक्य युद्ध होता है। जैसे-
सुरसती मतवा के करिले सुमिरनवा/हो रामा कंठे सुरवे/कंठे सुरवे होखss ना सहैया/ हो रामा कंठे सुरवे
दादरा और ठुमरी
संगीत में यह ओवरलैप दिखेगा कि कभी चीजें इतनी अदल-बदल कर गायी जाती हैं, कि दोनों का भेद कठिन हो जाता है। कम से कम हम जैसे आम श्रोता के लिए। एक ही गीत को कभी दादरा, कभी ठुमरी कह कर लगभग एक ही अंदाज़ में गाना। मैंने अपनी किताब में कुछ किताबी भेद जरूर लिखे, लेकिन प्रायोगिक रूप में मामला उलझा ही है।
यहाँ कुछ चाल का अंतर है। जैसे पहाड़ी रस्ते और मैदानी रास्ते में हमारी चाल बदल जाती है। ठुमक-ठुमक कर, और घोड़े की तरह दुलक-दुलक कर चलने में अंतर है।
दादरा की कुछ मेढकी या पहाड़ी चाल है, जिसे अजित वडनेरकर जी ने ‘शब्दों का सफर’ में घोड़े की चाल से मिलान किया है, कि दादरा ‘धा धि ना/ धा ती ना (धा धिन ना/ता तिन ना) करती चलती है। यही दादरा ताल भी है। इसकी गति भी कुछ तेज हो सकती है। यह हालांकि कहरवा या रूपक या दीपचंडी ताल में भी मिल जाएगी, इसलिए नियम बनाना कठिन है।
वहीं, ठुमरी अपने विस्तार के साथ आराम से ठुमकती चलती है। एक दादरा को ठुमरी की तरह गाया जा सकता है। एक ठुमरी को दादरा की तरह। यह अब गाने वाले के मूड पर है। लेकिन, इस अंदाज़ से जहाँ ठुमरी अपने में विरह, करुणा, प्रेम, भक्ति सब समेट लेती है; दादरा का क्षेत्र मूलत: शृंगार (एरोटिक) मूड का है। जैसे- ‘न बनावो बतियाँ, हटो काहे को झूठी’। यह भी दिखता है कि पारंपरिक दादरा में ऊर्दू के लफ़्ज़ मिल जाते हैं, ठुमरी में ब्रजभाषा-अवधी ही अधिक प्रयोग में हैं। इसका कारण यह भी है कि ठुमरी पारंपरिक रूप में वैष्णव राधा-कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़ी रही है। इसमें शृंगार-रस का इंजेक्शन या प्रचुरता कोठों पर जाने के बाद आयी।
दादरा तबला (या मन में गिनते हुए) के ताल के साथ-साथ एक अनुशासन से आगे बढ़ती है। ठुमरी में इस संतुलन से अधिक भाव का महत्व नजर आता है, यह रिजिड नहीं।
Buy Author’s book Wah Ustad at this link