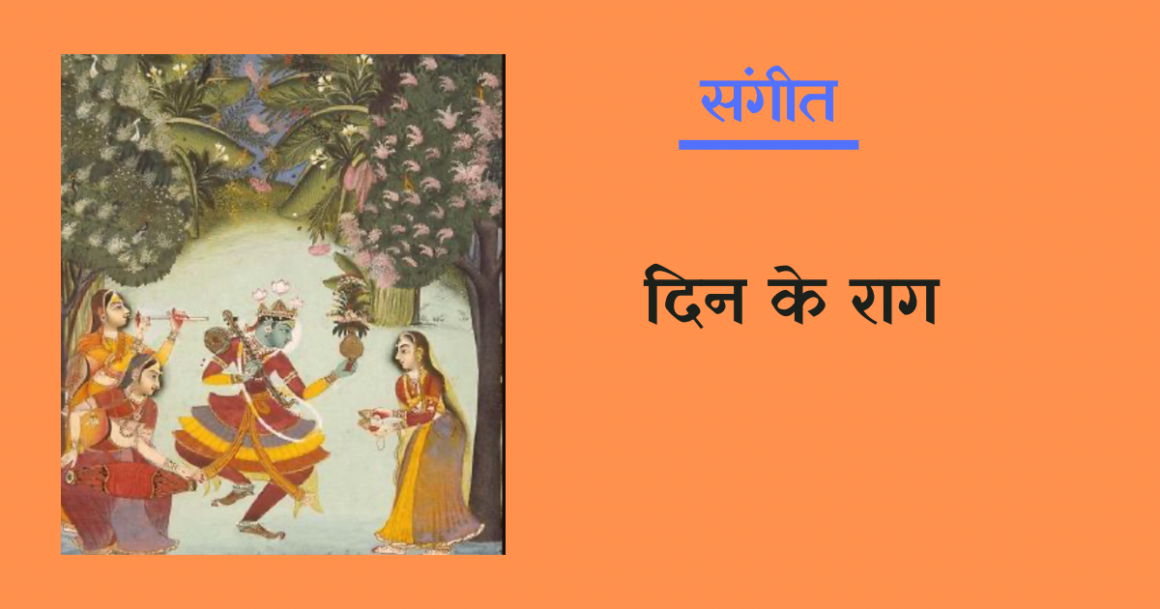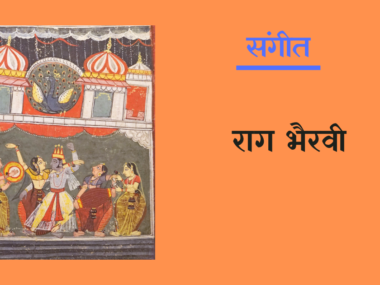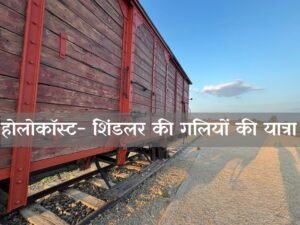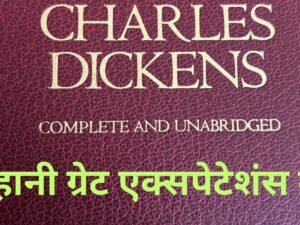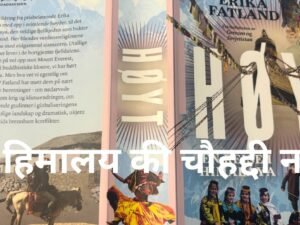9-12 बजे (दिन का दूसरा प्रहर)
‘बैजू बावरा’ फ़िल्म में तानसेन और बैजू बावरा के मध्य वह मशहूर संगीत-द्वंद्व किसे नहीं स्मरण? ‘आज गावत मन मेरो झूम के’ एक अद्भुत् प्रस्तुति है जिसमें उस्ताद अमीर ख़ान और पं. डी. वी. पुलुस्कर की आवाजों में टक्कर होती है। यह पं. भीमसेन जोशी और मन्ना डे के मध्य ‘केतकी गुलाब जूही’ की याद दिलाती है। बैजू बावरा का यह गीत राग देसी में है। फ़िल्म में इसका चित्रण है कि बैजू बावरा के गायन से संगमरमर का पत्थर पिघल कर पानी हो जाता है और तानसेन हार कर भी खुशी से गले मिलते हैं।
विदुषी प्रभा आत्रे जी की राग देसी में बंदिश है- ‘आज मोरी नैया पार उतारो’। इस प्रस्तुति में आलाप भी लंबा है और अंत का तराना इतने सुगम अंदाज में गाया है कि देसी को संपूर्णता में सुनने के लिए यह अच्छा उदाहरण है। इसी प्रहर का एक और राग है- मालगुंजी। उस पर कुछ बेहतरीन फ़िल्मी गीत बने, लेकिन इसका शास्त्रीय अंग मैंने कम सुना है।
एक दफे किसी ने पूछा कि सपेरों का राग कौन सा है? या किस राग से साँपों को वश में कर सकते हैं? अब यूँ तो विज्ञान के हिसाब से साँप सुन नहीं सकता, और वह सपेरे के बीन की हरकतों से आकर्षित होते हैं, ध्वनि से नहीं। किंतु इस प्रश्न का उत्तर अवश्य है। दक्खिन का राग पुन्नारागवली इस कड़ी में सबसे मशहूर राग है, और इस पर आधारित दक्खिन के फ़िल्मों में भी गीत है। हिन्दी फ़िल्मों का लोकप्रिय ट्यून ‘इक परदेशी मेरा दिल ले गया’ हालांकि इस राग पर नहीं। वह संभवत: राग पीलू पर आधारित है। सारंगी पर छजने वाले राग सारंग के भिन्न रूप भी सपेरों से जोड़े गए हैं। मालकौस का तो अर्थ ही सर्प की माला है।
लेकिन इन रागों में कोई साम्य नहीं, और इसलिए ये मेरी जिज्ञासा को शांत न कर सके। फिर मैं आनंद कूमारास्वामी द्वारा संकलित रागमाला पेंटिंगों को पलटने लगा, तो आखिर एक पेंटिंग मिली जिसमें एक स्त्री साँप हाथ में लिए मोरपंखी रंग के कपड़े में बैठी है। यह पेंटिंग राग आसावरी पर आधारित है। इसकी नायिका अपने प्रेमी को ढूँढती मलयगिरी पर्वत की ओर बढ़ रही है। और उस चंदन वन के साँप उसके शरीर से लिपटते जा रहे हैं। आज भी मैसूर के आस-पास के जो चंदन वन या कुख्यात वीरप्पन के इलाके हैं, वह मलयगिरी ही है। ‘मलयगिरी चंदन’ पूजा के लिए सर्वोत्तम माना भी गया है।
अब आसावरी को भी अगर विच्छेद करें तो संभव है कि यह ‘आशी’ और ‘अरि’ से जुड़ कर बना हो, और कालांतर में आसावरी बन गया हो। आशी का अर्थ साँप का विष है, और अरि का अर्थ शत्रु। तो विषधरों को जो वश में करे, वह है राग असावरी। और जब मैं घूम-फिर कर दक्खिन के पुन्नरागवली से साम्य ढूँढता हूँ तो अब कुछ समानता भी नजर आ रही है। इसे अगर कार्नाटिक स्वरमाला में लिखा जाए, तो शायद साम्य बैठ जाए। आसावरी तो कई लोगों ने गाया बजाया लेकिन इमरत ख़ान साहब की सुरबहार में आसावरी जरूर सुननी चाहिए।
12-3 बजे: दुपहरी के राग
वृंदावन में स्वामी हरिदास (तानसेन के गुरू) एक राग रचते हैं, और कृष्ण-राधा को धरती पर ले आते हैं। अगर मल्हार से वर्षा होती है, तो उसी में अलग भावना लाकर वृंदावनी सारंग बनता है और साक्षात् कृष्ण ही आ जाते हैं। स्वर एक से हैं, पर भावना में कृष्ण हैं। सारंग लोक-संस्कृति का राग है, जबकि मल्हार शास्त्रीय ध्रुपद अंग का है। सारंग में राजस्थान की खुशबू है, प्रेम भाव है और राजस्थान की सारंगी भी जुड़ी है। वृंदावनी सारंग ग्रीष्म ऋतु का राग है, और इसमें गांधार (ग) और धैवत (ध) वर्जित है। यह अन्य लोक या उपशास्त्रीय गायकी की तरह काफी थाट पर बना है, लेकिन यह गाया खयाल अंदाज में ही जाता है।
तो स्वामी हरिदास गाते हैं,
“माइ री सहज जोरी प्रगट भइ जु रंग की गौर श्याम घन-दामिनी जइसैं
प्रथम हूँ हुति अब हूँ आगे हूँ रहियै न टरिहैं तइसैं
अंग अंग की उजराइ सुघराइ सुंदरता अइसैं
श्री हरिदास के श्याम कुंजबिहारी सम वयस वइसैं।”
इस पद को हरिदासी प्रेम से सुनते ही राधा और कृष्ण प्रकट होते हैं और एक रूप हो जाते हैं। आज भी मथुरा के बांके-बिहारी मंदिर में वह इसी रूप में पूजित होते हैं। वृंदावनी सारंग हो, धमार हो, बिलासखानी तोडी हो और उनसे भी पूर्व संभवत: नंद कल्यान हो। कहते हैं कि शिशुओं को नंद कल्यान सुनाना चाहिए क्योंकि यह कृष्ण जन्म का राग है।
3-6 बजे (गोधूलि बेला के राग)
राग श्री की पदवी इसलिए भी ऊँची है कि पहले छह रागों में से है, और यह इकलौती राग पार्वती के मुख से निकली। बाद में सिख गुरूओं ने इस राग को केंद्र स्थान दिया और कई सबद इसी राग पर रचे गए। मैं एक नीदरलैंड के सरनामी गायक राज मोहन जी से मिला जो इस राग पर हनुमान चालीसा गा रहे थे। भक्ति में इसके बढ़ते वर्चस्व की वजह से ही यह सुबह गाई जाने लगी, जबकि इसका गायन-काल गोधूलि बेला (सूर्यास्त के समय) है। यह भी कहा जाता है कि राग देस की रचना राग श्री से हुई।
श्री हालांकि भक्ति के अतिरिक्त वीर रस का राग भी है। ओंकारनाथ ठाकुर इसे भयानक रस का राग मानते हैं, और यह गोधूलि बेला में भटकती प्रेतात्माओं को जगा देता है। हालांकि भूतों का राग मैं मालकौस को कहता हूँ, लेकिन लिखित रूप से भयानक राग ‘श्री’ ही है। मैंने इस राग के शायद कई प्रयोग किए, और कुछ अजीब सी सुस्ती जरूर आई पर भयानक कुछ न लगा। यह अवश्य हुआ कि जब यह सुबह सुनता तो ताजगी आती। कई-कई दिनों तक तो मैं अपनी सुबह सिख गुरबानी के साथ ही रखता हूँ। चाय पीते हुए राग श्री सुनते। यह ठीक ही हुआ कि इस राग को सुबह गाया जाने लगा।
ऋतुओं में यह हेमंत ऋतु (अक्तूबर) का राग है। गायकी में इस राग को पकड़ने के लिए आप ध्यान दें कि इस राग में कोमल ऋषभ (रे) बारम्बार आता है। यही वादी स्वर है। और इसमें ‘सा-नी-रे’ और ‘रे-रे-प’ भी कई बार सुनने को मिलते हैं। लेकिन यह राग एक कठिन राग है, जिसे गायक अमूमन महफ़िलों में गाते नहीं। मेरे अनुभव में इसे शाम को सुनने को बाद मन भी कुछ विचलित सा होता है। कुछ-कुछ राग दीपक सा। शायद इसलिए भी लोग कम गाते हों। एक बार अश्विनी भिडे देशपांडे जी को सुन रहा था, एक ऊँची तान पर पत्नी ने संगीत ही बंद कर दिया कि सर दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी मद्धिम कर सुनता रहता हूँ। किसी राग ने अगर तनाव भी ला दिया तो यह सिद्ध करता है कि रागों का शरीर पर प्रभाव है।
इस राग की सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में एक है कुमार गंधर्व की 1975 ई. की रिकॉर्डिंग। वह एक स्वर ‘रे’ पर कम अटके हैं, और राग श्री को रोचक बनाया है। कुमार गंधर्व ऐसे प्रयोग करते रहे कि चलन से हट कर राग को गाया कि वह जनप्रिय लगे और सरदर्द न बने।
इस प्रहर का दिलकश राग है- मारवा।
“मारवा संधि-प्रकाश का राग है
जब दिन जाता हुआ होता है और रात आती हुई होती है
जब दोनों मिलते हैं कुछ देर के लिए
वह अंत और आरम्भ के बीच का धुंधलका है
जन्म और मृत्यु के मिलने की जगह”
– मंगलेश डबराल
राग मारवा और उस्ताद अमीर ख़ान एक दूसरे के पर्याय कहे जा सकते हैं। मुझे इस राग का नाम सुनते ही वही याद आते हैं। कभी यूँ ही अल्हड़पन में इस राग को मैंने कामोत्तेजक राग कह दिया था। दरअसल इस राग की रागमाला पेंटिंग में एक राजा अपनी रानी को शयनकक्ष की ओर ले जा रहे हैं। यही देख यह शुबहा हुआ। सूर्यास्त के आस-पास की बेला में चित्त की स्थिति कुछ विचित्र तो होती ही है। लोग ऑफ़िस से लौट रहे होते हैं, या लौट कर थके-हारे बैठे होते हैं। ऐसे समय में संगीत अगर संतुलित न हो, तो तनाव बढ़ जाए। मारवा उसी वक्त चित्त और मन के बीच एक पुल का काम करता है।
मारवा से मिलते-जुलते मूड में राग सोहनी भी है। सोहनी में कुछ ऊँचे स्वरों पर अधिक जोर है, यानी धैवत (ध), निषाद (नि) पर। और-तो-और यह गाया भी ऊँचा जाता है, अक्सर तार सप्तक में। यह राग इसलिए मुश्किल है ओर कम लोग गाते हैं। एक फैयाज़ ख़ान की बंदिश ‘चलो हटो जाओ जाओ सैंया’ या किशोरी अमोनकर जी की ‘सजन नहीं आए, जोबन बीता जाए’ से यह अंदाजा लग जाएगा कि इसका मूड क्या है? इसमें रूमानी चाहत की इंतहा है।
उस्ताद अमीर ख़ान की गायी बंदिश ‘गुरु बिन ज्ञान न पावे’ राग मारवा की एक कालजयी प्रस्तुति है ही और इसमें अमीर ख़ान की ‘मेरुखण्ड’ से तान बनाने की शैली गौर करने लायक है। कहते हैं कि उस्ताद जब मारवा गाते तो पूरा दर्शक-मंडल सन्न रह जाता। मुझे नहीं लगता कि मारवा को अमीर ख़ान और बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने जितनी ऊँचाई दी, उतना पहले या बाद में कोई दे सका।
कुशल दास ने सुरबहार पर मारवा बजाया है जिसे सुन कर यह कल्पना की जा सकती है कि अन्नपूर्णा देवी कैसा बजाती होगी। शाम को यूँ ही क्षितिज पर सूर्य को अस्त होते देखना और सुरबहार की झण्कार सुनना यूँ लगता है कि गायों का झुंड खेतों से एक धुन में वापस लौट रहा है। मैहर से दूसरी लंबी प्रस्तुति निखिल बनर्जी की भी उपलब्ध है। निखिल बनर्जी की आलाप में बढ़त जहाँ कुछ धीमी और हर स्वर को बारीकी से छूते, एक-एक पुष्प चुनते नजर आती है; कुशल दास का आलाप कुछ यूँ है कि स्वरों की माला गूँथी जा रही हो।
लेकिन मारवा से पहले भीमपलासी सुनी जानी चाहिए। भीमपलासी दोपहर-शाम कभी भी सुनी जा सकती है। मन्ना डे को यह राग पसंद था, और एक खास उल्लेख आता है जब उनसे कविता कृष्णमूर्ति जी गायन सीखतीं थी। घंटों उनके बैंगलूर निवास पर कविता जी बैठ कर रियाज करतीं। कविता जी सीख कर जब बंबई गयीं और लौटीं तो मन्ना डे को खुशखबरी सुनाई कि उनके सिखाए राग पर जो गीत बना वो सुपरहिट हो गया। मन्ना डे ने जब गीत सुना तो भड़क गए, कि यह क्या राग का फलूदा बना दिया? और एक स्त्री होकर यह कैसा नारियों के अपमान में गीत रचा? कविता जी को इतना डांटा कि वे रो पड़ीं।
गीत था- ‘तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त… नी सा ग म प नी सा’
अब यही राग लता जी ने हर स्वर को आंदोलित कर गाया- ‘नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमकी हाए’
एक पॉप बन गया, रवीना टंडन नाचने लगी। और दूसरा क्लासिकल साधना पर फिल्माया गया। इस राग की सबसे मशहूर बंदिश है जिसे पं. जसराज और संजीव अभ्यंकर की आवाज में सुना जा सकता है,
“जा जा रे अपने मंदिरवा/सुन पावेगी सास ननदियाँ
सुन हूँ सदारंग तुमको चाहत है/क्या तुम हमको छलन किया।”
भीमपलासी, मधुवन्ती, पटदीप और मुल्तानी एक से राग हैं। मुल्तानी भी दोपहर से गोधूलि बेला तक ही गाया जाता है। मुल्तानी राग अमीर खुसरो के एक गुरु सूफी संत बहाउद्दीन ज़कारिया मुल्तानी का बनाया राग है। सूफियाना आवाजें ऊँची होती है, और यही वजह है कि मुल्तानी भी तार सप्तक (ऊँचे सप्तक) में गाया जाता है। अगर मुल्तानी मंद्र या मध्य सप्तक में गाया जाए तो यह मुल्तानी कहाँ रहेगा? तोड़ी बन जाएगा। यह राग पंजाब वाले खूब निभाते हैं। जैसे शाम चौरसिया घराने के सलामत-नजाकत अली ख़ान की जोड़ी। उस्ताद अमीर ख़ान ने ‘शबाब’ फ़िल्म में मुल्तानी में शीर्षक गीत गाया है- ‘दया कर हे गिरिधर गोपाल’। मुल्तानी में हम लीन हो जाते हैं, और इसे मैं अक्सर कुछ पढ़ते वक्त फ़ोकस करने के लिए प्रयोग करता हूँ।
फ़ोकस की तो क्या बात, कई लोगों को हिंदुस्तानी संगीत सुनते ही बोरियत या नींद आती है। अगर आपको सचमुच नींद लानी हो तो राग पीलू सुनिए। यह है गोधूलि बेला का राग, लेकिन बच्चों को लोरी सुनाने में कारगर है। जो लोग ‘रेडियो सिलोन’ बचपन में सुनते होंगें, उन्हें याद होगा ठीक 11 बजे प्रोग्राम खत्म होते ही लता मंगेशकर फिल्म ‘अलबेला’ से गीत गाती- ‘धीरे से आ जा अँखियन में’। यह गीत माँएँ बच्चों को सुलाने में काम लाती। कहने की जरूरत नहीं सी. रामचंद्रा की ये कम्पोजिशन राग पीलू पर है। सलिल चौधरी का ‘आ जा री आ, निंदिया आ जा तू…’ भी इसी राग में है।
दरअसल पीलू में चार कोमल यानी हल्के स्वर हैं, जो आपके मन को हल्का कर देते हैं। लेकिन कोमल स्वरों में गाना-बजाना कठिन हो जाता है। फ़िल्मी गीतों की बात कही तो, ‘काली घटा छाए, मोरा जिया घबराए..’। यह गाना बस लता गा सकती थी पर एस.डी. बर्मन की कुछ अन-बन थी, आशा जी से गवा लिया। अब लग रहा है वो आशा जी के लिए ही बना था। और आशाजी ने तो पीलू में पॉप भी गाया। जब ओ. पी. नय्यर ने उनसे गवाया- ‘जाइए आप कहाँ जाएँगें’ तो उस्ताद अमीर खान ने फोन किया, “भाई! क्या जुल्म कर रहे हो?”
नौशाद साहब भी पीलू के दीवाने थे। मुगल-ए-आजम का ‘मोहे पनघट पे, नंदलाल’ पीलू में ही है। वह मशहूर युगल गीत ‘जाने क्या तूने कही’ में भी पीलू का प्रभाव है। जैसे राग पहाड़ी कोमल स्वरों की वजह से सुगम फ़िल्मी संगीत में खूब प्रयोग होता है, वैसे ही पीलू भी।
एक व्यस्त मुहल्ले में शाम हो रही है। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं। महिलाएँ छत पर बैठी हैं, गप्पें मार रही है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यह पच्छिम के ‘ब्लूज़’ संगीत वाला माहौल है जहाँ कुछ शोर भी है, और सन्नाटा भी। ऐसे माहौल में नेपथ्य में पुरिया धनश्री बजता रहे तो सोने पर सुहागा। पुरिया धनश्री सुनने में (और रस में भी) मारवा और सोहनी रागों के करीब है। यह भी गोधूलि बेला का ही राग है। इस राग में एक लोकप्रिय ट्रेडमार्क बंदिश है,
“पायलिया झण्कार मोरी; झनन झनन बाजे झण्कार;
पिया समझाउ समझत नाही; सास ननद मोरी देगी गारी।”
इस बंदिश में एक उत्तर-दक्खिन की जुगलबंदी है- किशोरी अमोनकर जी और बालामुरली कृष्णा के बीच। यहाँ किशोरी जी हिंदी में और उसी बंदिश को तमिल में बालामुरली कृष्णा गाते हैं। इसे सुनते वक्त पुरिया का हर रंग निखर उठता है। इस बंदिश से मिलता-जुलता ही फ़िल्म रंगीला का गीत है- ‘हाय रामा ये क्या हुआ..’। उस गीत में जो माहौल बना है और सिनेमैटोग्राफ़ी है, वह पुरिया और मारवा के मूड से मिलती है। बस मिलती ही नहीं. बल्कि इस गीत की शुरुआत ही नेपथ्य में गायी जा रही इस बंदिश से होती है। जब प्रेम में लंबे विरह के बाद युगल अचानक मिल गए हों, यानी करुणा (दर्द) भी है और शृंगार भी। इसलिए यह भारी-भरकम राग है, सहज नहीं। इस रस को लाना कितना कठिन है कि दर्द भी हो और खुशी भी। पुरिया में यह भावना ‘पंचम’ (प) की वजह से आती है, जहाँ गायक अक्सर जोर देते हैं, विराम लेते हैं। यही इसका वादी स्वर भी है। अक्सर यह राग ऐसे उठायी जाती है- नि रे ग म प प…. इसमें कुछ सूफ़ियाना रस भी है, और इसलिए यह निजामुद्दीन औलिया के प्रिय राग में से था।
पुरिया के साथ मेवाती घराना और पं. जसराज का साथ ख़ास जुड़ाव है। गायकी में उनके घराने से बेहतर पुरिया कम लोगों ने गाया। उनकी गायी बंदिश ‘फूलन के हरवा’ यू-ट्यूब से सुनी जा सकती है। वादन में उस्ताद विलायत ख़ान का बजाया पुरिया अद्वितीय है। उसमें जो झाला है और तबले की तीनताल मात्राओं के साथ गति की कलाबाजी है, वह सुनने लायक है। उनके दादा इमदाद ख़ान तो बस दो ही राग बजाते थे- पुरिया और यमन कल्यान।
एक बार किसी ने पूछ लिया, “ख़ान साहब! आप कुछ और क्यों नहीं बजाते?”
उन्होंने हँस कर कहा, “इन रागों के लिए तो एक जन्म कम है। गर इन्हें इस जन्म में साध लिया, तो अगले जन्म में जरूर कुछ और बजाउँगा।”