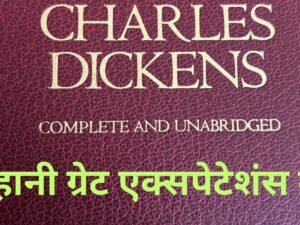Translation of Nobel speech by Vidiadhar Surajprasad Naipaul
दो दुनिया
1
यह मेरे लिए असामान्य है। मैंने पाठ अवश्य किए हैं, लेकिन कभी भाषण नहीं दिया। मुझे जो भाषण देने कहते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ – मेरे पास भाषण देने के लिए कुछ नहीं है। यह सच है।
यह बात अजीब लग सकती है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के पचास वर्ष मात्र शब्द, भावों और विचारों में बिताए; उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे संबंध में जो कुछ भी मूल्यवान है, वह मेरी पुस्तकों में ही है। इसके अतिरिक्त जो भी है, वह अपरिपक्व है। मुझे इसका बोध नहीं। संभवत: मेरी अगली पुस्तक की प्रतीक्षा में है। यह कभी अचानक मेरे मन में आएगा, जब मैं लिखने बैठूँगा। यह आश्चर्य का तत्त्व (एलिमेंट ऑफ़ सरप्राइज) ही मैं अपनी लेखनी में ढूँढता हूँ। आत्म-आकलन का तरीका इतना आसान तो नहीं ही है।
प्रूस्त ने बहुत बारीकी से एक लेखक के रूप में लेखक, और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में लेखक, के अंतर बताए हैं। यह उनके निबंध संग्रह ‘अगेन्स्ट सेंते ब्यूवे’ में मिलेगा।
उन्नीसवीं सदी के फ़्रेंच आलोचक सेंते ब्यूवे की अवमानना थी –
लेखक को समझने के लिए उसके बाह्य-स्वरूप और उसके जीवन को समझना आवश्यक है।
यह एक आकर्षक अवधारणा नजर आती है कि एक व्यक्ति के माध्यम से उसकी कृति पर दृष्टि डाली जाए। यह अवधारणा अकाट्य नजर आती है। प्रूस्त ने इस अवधारणा की तर्कपूर्वक धज्जियाँ उड़ाई।
प्रूस्त ने लिखा, “सेंते ब्यूवे का तरीका हमारी अंतरात्मा की मामूली समझ पर भी ध्यान नहीं देता। पुस्तक हमारे दूसरे पक्ष की कृति है, जो हमारे मुखर सामाजिक पक्ष से भिन्न है। अगर हम उस दूसरे पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, उस आधार पर अपनी धारणा बनाएँगे, तब हमें शायद सही निष्कर्ष मिले।”
प्रूस्त के यह शब्द आपके साथ होने चाहिए जब आप किसी लेखक या किसी भी व्यक्ति की जीवनी पढ़ रहे हों, जिनसे आप प्रेरणा लेना चाहते हों। जीवनी में जीवन के हर रहस्य और संबंध आपके समक्ष होंगे, लेकिन उनकी लेखनी का रहस्य न होगा। किसी भी तरह का दस्तावेजीकरण हमें वहाँ नहीं पहुँचा सकता।
लेखक की जीवनी तो क्या, आत्मकथा भी अपूर्ण होती है।
प्रूस्त तो इस विस्तारण के उस्ताद हैं, लेकिन मैं कुछ देर के लिए ‘अगेंस्ट सेंते ब्यूवे’ पर लौटना चाहूँगा।
प्रूस्त लिखते हैं, “दरअसल लेखक अपने अंतरात्मा की उक्ति, जो एकांत में लिखी गयी, वही हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। सामाजिक जीवन में तो हमारा सतही रूप ही सबके समक्ष होता है, अंतरात्मा की उक्ति नहीं। जब हम अपने उस रूप को, जो समाज के मध्य है, किनारे कर देंगे, तभी हमारी अंतरात्मा की ध्वनि सुनाई देगी।”
जब प्रूस्त यह लिख रहे थे, उस वक्त उन्हें वह विषय नहीं मिला था। वह विषय जो उनके महान् साहित्यिक परिश्रम का सुंदर प्रतिफल होने वाला था। आप मेरे दिए संदर्भ से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपने आत्म-बोध पर विश्वास करते थे कि उनका भाग्य ही एक दिन उन्हें विषय देगा। मैंने यह संदर्भ कई स्थानों पर दिए हैं। इसका कारण है कि मैं अपना कार्य इन्हीं सिद्धांतों पर करता हूँ। मैंने अपने आत्म-बोध पर भरोसा किया है। शुरुआत में भी किया था, अब भी करता हूँ। मुझे इल्म नहीं कि आगे क्या होगा और क्या लिख बैठूँगा। मैंने लेखन का विषय अपने आत्म-बोध पर छोड़ रखा है। मेरे पास एक सोच और एक रूपरेखा जरूर होती है, जब मैं लिखना शुरू करता हूँ; लेकिन यह समझने में मुझे भी बरसों लग जाते हैं कि आखिर मैंने लिखा क्या?
मैंने पहले कहा है कि मेरे विषय में जो भी मूल्यवान है, वह मेरी किताबों में है। अब मैं इस पर आगे की बात कहता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि मैं अपनी पुस्तकों का योग-फल हूँ। हर पुस्तक जो मेरे आत्म-बोध से जन्मी, वह मेरे अनुभव का ही विस्तार है। मेरे जीवन के किसी साहित्यिक बिंदु पर जो आखिरी पुस्तक होगी, उसमें उससे पहले लिखी किताबें समाहित होगी। इसका कारण मेरी पृष्ठभूमि है।
2
मेरी पृष्ठभूमि जितनी सुलभ है, उतनी ही भ्रांतिपूर्ण। मैं ट्रिनिडाड में जन्मा। वेनेजुएला के ओर्निको नदी के मुहाने पर छोटा सा द्वीप। ट्रिनिडाड न पूरी तरह दक्षिण अमरीका का हिस्सा है, न कैरीबियन का। यह नई दुनिया के एक बागान (प्लांटेशन) उपनिवेश की तरह विकसित किया गया। 1932 ई. में मेरे जन्म के समय यहाँ की जनसंख्या चार लाख थी। उनमें डेढ़ लाख भारतीय थे। लगभग सभी गंगा के मैदानी इलाकों से आए हिन्दू और मुसलमान।
यह मेरा छोटा सा समुदाय था। इस भारतीय आप्रवास का बड़ा हिस्सा 1880 ई. के बाद का था। मसौदा कुछ इस तरह था। मजदूरों का बागान से पाँच साल का बंधन था। यह अवधि खत्म होने पर उन्हें भारत वापसी का टिकट मिलता अथवा पाँच एकड़ जमीन। 1917 ई. में गांधी और अन्य लोगों के विरोध से यह प्रथा खत्म कर दी गयी। इस विरोध के कारण अंतिम किश्त में आए लोगों को न टिकट मिली, न जमीन। ऐसे लोग तो कहीं के न रहे। ये लोग पोर्ट-ऑफ-स्पेन की सड़कों पर सोते। मैंने बचपन में उन्हें सड़कों पर पड़े देखा है। मुझे उस वक्त उनकी परिस्थिति का बोध नहीं था। यह बात मेरे ध्यान में बाद में आयी। उस वक्त उनकी परिस्थिति का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह उस उपनिवेश में हो रही निर्दयता का मात्र एक उदाहरण है।
मेरा जन्म एक छोटे शहर शहुआनास (Chaguanas) में हुआ। यह परीआ की खाड़ी से दो-तीन मील की दूरी पर था। शहुआनास भारतीयों के लिए उच्चारण और हिज्जे के हिसाब से विचित्र नाम था तो वह इसे भारतीय जाति-नाम ‘चौहान’ (Chauhan) कहते थे।
मैं चौंतीस साल का था जब मुझे अपने जन्म-स्थान के विषय में पता लगा। मैं सोलह वर्ष से लंदन में रह रहा था। उस वक्त मैं अपनी नौवीं किताब लिख रहा था। यह ट्रिनिडाड के मानव-इतिहास पर आधारित था जिसमें मैं वहाँ की कथाएँ पुनर्जीवित कर रहा था। मैं ब्रिटिश संग्रहालय जाकर स्पैनिश काग़जात पलटता रहता। ये काग़जात 1890 ई. के वेनेजुएला विवाद के संदर्भ में स्पैनिश आर्काईवों से ब्रिटिश सरकार के लिए नकल (कॉपी) किए गए थे। यह विवाद 1530 ई. में शुरू हुआ और स्पैनिश सत्ता के अंत तक चलता रहा।
मैं एल डोरैडो के बेवकूफाना खोज और अंग्रेज नायक वाल्टर रेली के संबंध में पढ़ रहा था। 1595 ई. में उसने ट्रिनिडाड पर आक्रमण कर सभी स्पैनिश लोगों को मार कर, ओर्निको तक ‘एल डोरैडो’ खोजते हुए यात्रा की। उसे कुछ नहीं मिला पर इंग्लैंड जाकर कहा कि ‘एल डोरैडो’ मिल गया। उसके पास दिखाने के लिए मात्र कुछ रेत और कुछ सोना था। उसने दावा किया कि ओर्निको की रेत से यह सोना निकला। जिस जौहरी ने उसे जाँचा, उसने कहा कि रेत में कुछ भी नहीं और सोना उत्तरी अफ्रीका का है।
उसने अपनी बात को साबित करने के लिए एक किताब लिखी और चार सदी तक लोग मानते रहे कि उसे कुछ मिला था। उस पुस्तक का लंबा शीर्षक ही भ्रामक है- “एक विशाल, समृद्ध और सुंदर गुयाना साम्राज्य की खोज, जो महान् स्वर्णिम मानोआ (एल डोरैडो) के पास है, और एमेरिया, आरोमिया, अमापिया तथा अन्य रियासतों के करीब”
इसमें कितना सच नजर आता है? वह शायद ही कभी ओर्निको पहुँच पाया।
जैसा अति-आत्मविश्वासी लोगों के साथ होता है, रेली अपनी ही कल्पनाओं का शिकार होता है। बीस साल बाद, वृद्ध और बीमार रेली को लंदन कारागार से रिहा किया गया और गुयाना जाकर सोने की खान खोजने कहा गया। इस छलपूर्ण यात्रा में उन्होंने अपना बेटा खो दिया। एक पिता ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा के फेर में अपना बेटा गँवा दिया। हताशा और ग्लानि से भरे रेली के पास जीने का कोई मूल्य नहीं बचा था और वह सूली पर चढ़ने लंदन लौट गया।
कहानी यहाँ खत्म हो जानी थी। लेकिन स्पैनिश स्मृतियाँ लंबी होती है। शायद इसलिए उनकी राजकीय चिट्ठियाँ भी देर से पहुँचती थी। ट्रिनिडाड की चिट्ठियों को स्पेन पहुँचने में दो साल भी लग जाते थे। आठ साल के बाद भी ट्रिनिडाड और गुयाना के स्पैनिश खाड़ी के ‘इंडियन्स’ (मूल निवासी) से हिसाब बराबर कर रहे थे। एक दिन ब्रिटिश संग्रहालय में मैंने स्पेन के राजा की ट्रिनिडाड के गवर्नर को लिखी चिट्ठी पढ़ी। उसमें तारीख लिखी थी- 12 अक्तूबर 1625!
राजा ने लिखा था, “मुझे आप से इंडियन्स की धरती शहुआनास की जानकारी चाहिए। आपके अनुसार उनकी संख्या हज़ार से अधिक है। वे इतने गिरे हुए लोग हैं कि जब शहर लूटा जा रहा था, वे ब्रिटिशों की अगुवाई कर रहे थे। उनके इस अपराध की सजा नहीं मिल पायी थी क्योंकि हमारी सेना पर्याप्त नहीं थी; और चूँकि इंडियन्स हमें मालिक नहीं मानते तो हमने दंड देने का फैसला लिया है। मेरी आज्ञा का पालन करें और मुझे ख़बर करते रहें कि आप क्या कर रहे हैं।”
गवर्नर ने क्या किया, यह मुझे नहीं पता। मुझे संग्रहालय में शहुआनास को कोई और संदर्भ नहीं मिला। शायद सेवील के स्पैनिश आर्काइव के काग़जों के अम्बार में शहुआनास के अन्य संदर्भ रहे हों, जिसकी नकल बनाना ब्रिटिश भूल गए। सत्य यह है कि कुछ हज़ार इंडियन्स आदिवासी जो पारिया की खाड़ी के दोनो तरफ बसे थे, वे ऐसे विलुप्त हुए कि अब शहुआनास या चौहान में उन्हें कोई नहीं जानता। मुझे यूँ लगा कि उस ब्रिटिश संग्रहालय में 1625 ई. के बाद उस स्पेन के राजा की चिट्ठी का अर्थ ढूँढने वाला मैं पहली व्यक्ति था। वह काग़ज मुझसे पहले मात्र 1896-97 ई. में पढ़ा गया था, और फिर दशकों तक नहीं पढ़ा गया।
हम शहुआनास में रहते थे। जब मैंने अपने विद्यालय जाना प्रारंभ किया, प्रतिदिन मैं अपनी दादी के घर के सामने से गुजरता; दो-तीन दुकान पार करते ही चाइनीज़ पार्लर, जुबली थिएटर। वह दुर्गंध करती सस्ते साबुन की पुर्तगाली फैक्ट्री, जहाँ साबुन की टिक्कियाँ सुखाई जाती। मैं आखिर शहुआनास राजकीय विद्यालय पहुँचता। विद्यालय के आगे गन्ने के बागान थे, जो पारिया की खाड़ी तक फैले थे। जो लोग बाग़ान से बेदखल हो गए थे, उनके अपने खेत, अपनी दिनचर्या, अपने नियम और अपने धर्मस्थल थे। उन्हें इल्म था कि ओरिनोको नदी कितनी तीव्र गति से पारिया की खाड़ी में गिरती है। अब उनके सभी कौशल और उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
3
दुनिया हर समय चलायमान रहती है। लोग हर जगह बेदखल होते रहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब 1967 ई. में पहली बार मुझे अपने जन्म-स्थान के संबंध में ऐसी बातें मालूम हुई जो मुझे पता ही न थी। दरअसल हम इन कृषि-प्रधान उपनिवेशों में अंधों की तरह रहते थे। यह वहाँ के अधिकारियों की हमें अंधेरे में रखने की चाल नहीं थी। हमें बस इसका ज्ञान नहीं था। शहुआनास के विषय में जानना न ही महत्वपूर्ण था, न सुलभ। वहाँ कुछ आदिवासी जरूर थे। ब्रिटिश गयाना में ये लोग हास्य के पात्र थे। जंगली और हो-हल्ला करने वाले- वाराहूण!
मुझे लगता था कि यह शब्द यूँ ही बना दिया गया। लेकिन वेनेजुएला यात्रा के दौरान मुझे मालूम हुआ कि यह वाकई एक आदिवासी जाति है।
बचपन की एक धुँधली सी कहानी थी. जो अब मेरे लिए एक विदारक कथा है। ये आदिवासी मुख्यभूमि से नाव पर आते थे, जंगलों से गुजरते द्वीप के दक्षिणी छोर तक जाते थे। कुछ फल उठा कर चढ़ावा चढ़ाते थे। उसके पश्चात पारिया की खाड़ी से गुजरते हुए ओरिनोको के मुहाने तक चले जाते थे। यह प्रक्रिया जरूर महत्वपूर्ण होगी जो चार सौ वर्षों के उनके विलुप्तप्राय इतिहास में बच कर रह गयी होगी।
शायद वे वेनेजुएला और ट्रिनिडाड की समान वनस्पति होने के बावजूद एक ख़ास फल ढूँढने आते थे। मुझे नहीं मालूम। मुझे याद भी नहीं कि किसी ने यह सवाल पूछा हो। अब स्मृतियाँ भी खो गयी। वह पवित्र जमीन अगर वाकई थी, तो वह अब सपाट हो चुकी है।
जो बीत गयी, वह बात गयी। मुझे लगता है कि यही सामान्य नजरिया है। हम भारतीय, जो भारत से प्रवासित हुए, वे इसी नजरिए के साथ द्वीप पर रहे। हम रीति-रिवाजों से जीवन जीते रहे। कभी अपना आकलन नहीं किया, जहाँ से ज्ञान का उद्गम होता।
हम में से आधे लोग ढोंग करते रहे या संभवत: मात्र अनुभव जमा करते रहे; लेकिन कभी ऐसी सोच नहीं बनायी कि हम अपने साथ एक ऐसा भारत लेकर आए हैं जिसे कालीन की तरह इस सपाट धरती पर बिछा सकते हैं।
शहुआनास में मेरी दादी का घर दो हिस्सों में बँटा था। सामने का हिस्सा ईंट और पलस्तर से बना था, जिसमें सफ़ेद रंग चढ़ा था। यह किसी आम भारतीय घर की तरह था, जिसमें ऊपरी तल पर एक बड़ी रेलिंग लगी छत होती। उसके ऊपर के तल पर पूजा-घर होता। यह शिल्प-कला के हिसाब से काफी समृद्ध था। खंभों पर कमल और हिंदू देवी-देवता उकेरे थे। सब भारत से लायी स्मृतियों से बनाए गए। ट्रिनिडाड के हिसाब से यह विचित्र वास्तु-कला थी। इस घर के पीछे फ्रेंच कैरीबियन शैली की इमारत एक पुल से जुड़ी थी। प्रवेश-द्वार घर के दोनों हिस्सों के मध्य किनारों से होकर था। लकड़ी के फ़्रेम से बना लोहे का विशाल द्वार था। यह द्वार उस घर को घोर निजता देती थी।
बचपन में मुझे दो दुनिया का बोध हुआ। एक जो उस ऊँचे द्वार के बाहर शुरु होता, और एक घर के अंदर। यूँ कहिए कि अपनी दादी की दुनिया। यह हमारे जाति-बोध के कुछ अवशेष थे, जिसे आखिर खत्म कर दिया गया। ट्रिनिडाड के आप्रवासियों के लिए जातिवाद का अंत एक तरह की सुरक्षा थी, क्योंकि यह उपेक्षित समुदाय था। कुछ समय के लिए, और मात्र कुछ समय के लिए, अपने तरीके से जीना, अपने शर्तों पर जीना, हमारे मिटते हुए भारत में जीना। यह अजीब सी आत्म-केंद्रित धारणा थी। हमने अपने अंदर झाँका, अपने दिन जीए। बाहर की अंधकारमय दुनिया से हमने कोई सवाल नहीं किए।
हमारे पड़ोस में एक मुसलमान की दुकान थी। मेरी दादी की दुकान का एक कोना उसके दुकान की दीवाल से लगा था। उसका नाम था- मियाँ। हमें उसे और उसके परिवार के संबंध में बस इतना ही मालूम था। हमने शायद उसे देखा भी हो, लेकिन मेरे मन में कोई छवि अब नहीं उभरती। हमें मुसलमानों का कुछ पता नहीं होता था। यह परायापन और अपनी निजता से बाहर रखना दूसरे हिंदुओं के लिए भी था।
जैसे, हम दिन में भात और रात को रोटी खाते। कुछ लोग इस प्राकृतिक नियम का पालन न कर रात में भात खाते। मुझे ये लोग अजनबी नजर आते। आप यह कल्पना करिए कि मैं उस वक्त सात वर्ष से कम उम्र का था, क्योंकि सात वर्ष के उम्र में ही शहुआनास में दादी की यह दुनिया मेरे लिए खत्म हो गयी। हम (ट्रिनिडाड की) राजधानी चले आए। बाद में उत्तर-पश्चिम की पहाड़ों पर।
लेकिन मन की यह प्रवृत्ति कि कुछ दरवाजे खोलने हैं, कुछ बंद करने हैं, यह कुछ समय चलता रहा। अगर मेरे पिता ने लघु-कथाएँ नहीं लिखी होती तो मुझे भारतीय समुदाय के जीवन का कोई ज्ञान न होता। उन कथाओं ने मुझे ज्ञान के अतिरिक्त भी बहुत कुछ दिया। मुझे एक तरह से ठोस बनाया। दुनिया में खड़े होने की एक जगह दी। इन कथाओं के बिना न जाने मेरा मष्तिष्क कैसा होता?
बाहर की दुनिया अंधकारमय थी, जिसकी हमारे मन में कोई जिज्ञासा न थी। मेरी उम्र मात्र इतनी थी कि भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण की कुछ समझ बन पायी। जो हमारे परिवार में पाँच वर्ष या उसके बाद आए, उनके भाग्य में यह भी नहीं था। हमें किसी ने हिन्दी नहीं सिखायी। कभी कोई कुछ अक्षर लिख गया, बस उतना ही; बाकी हमें खुद ही सीखना था।
जैसे-जैसे अंग्रेज़ी ने हमारे घर में प्रवेश किया, हमने अपनी भाषा खोनी शुरू की।
मेरी दादी के घर में धर्म ही धर्म था, खूब पाठ-पूजा होती, कुछ तो कई दिनों तक चलते। लेकिन हमें भाषा समझ नहीं आती। किसी ने कभी हमें अनुवाद कर समझाया नहीं।
इसलिए हमारे पूर्वजों का धर्म हमारे दैनिक जीवन से खत्म होता गया, और एक रहस्य बनता गया।
Author Praveen Jha translates a part of Nobel Prize speech of V S Naipaul.
Read original complete lecture here
गिरमिटियों का इतिहास इस पुस्तक में पढ़ें Click here for book Coolie Lines based on Girmitiya history
मेसोअमरीकी इंडियन्स का इतिहास इस पुस्तक में